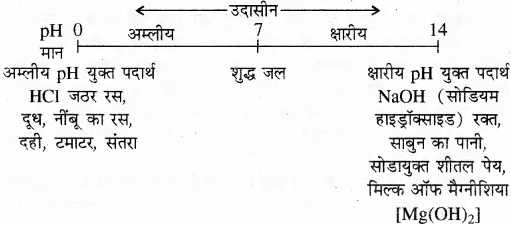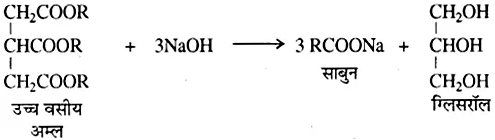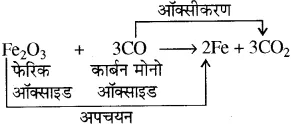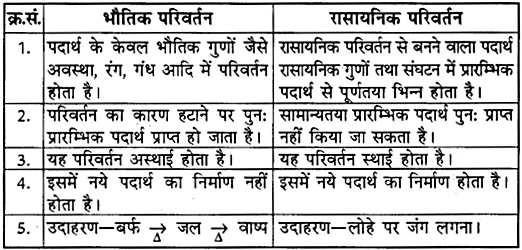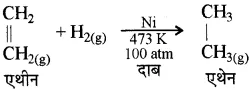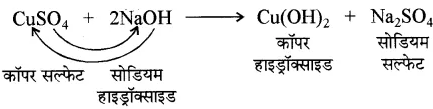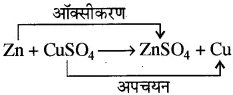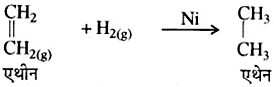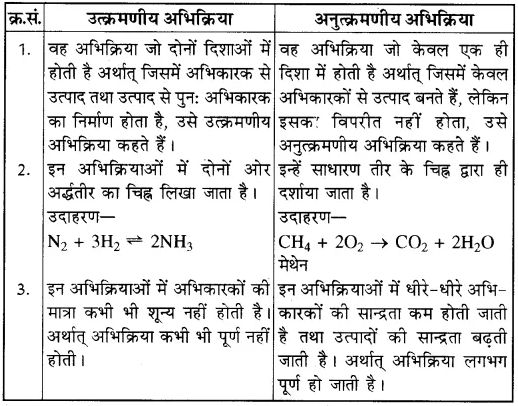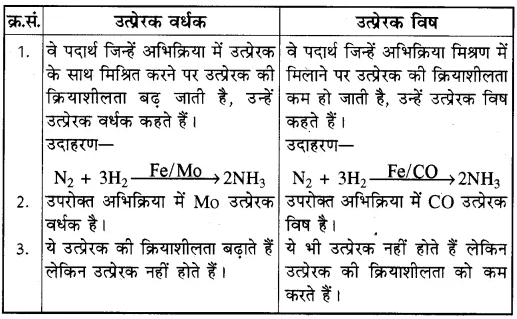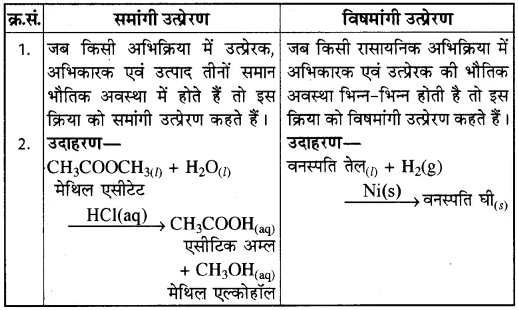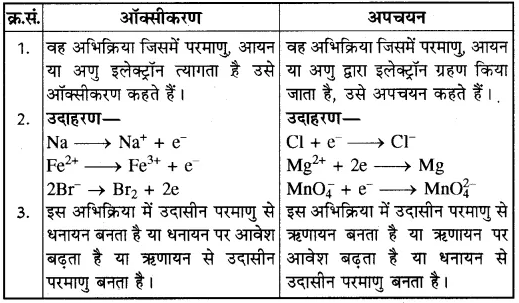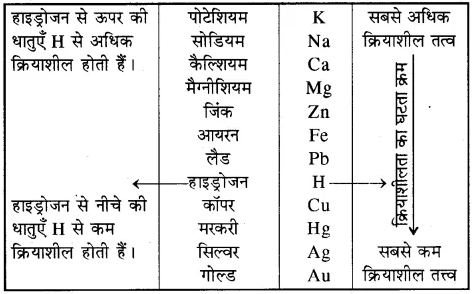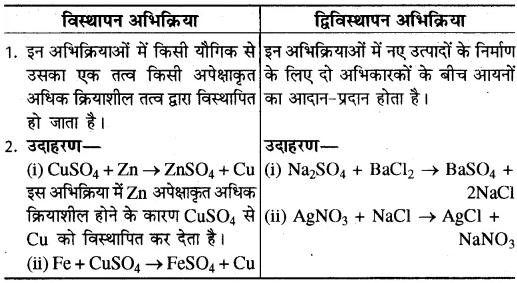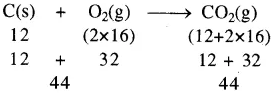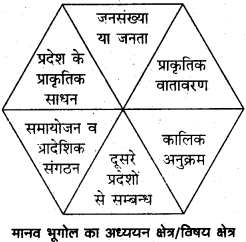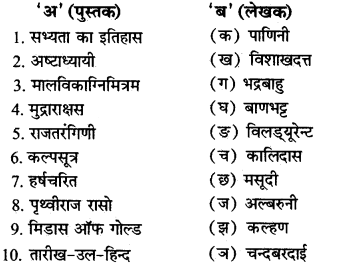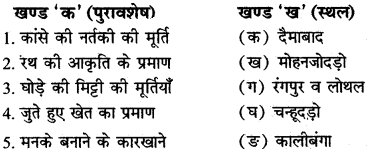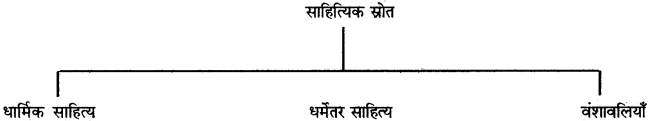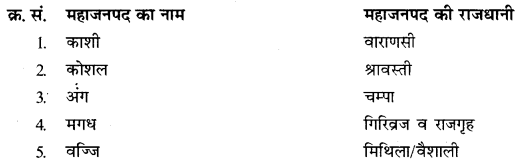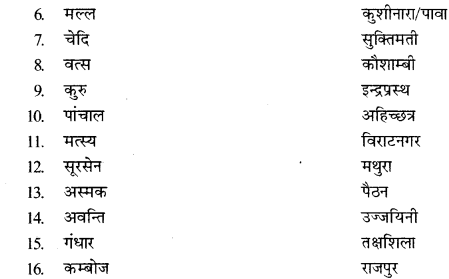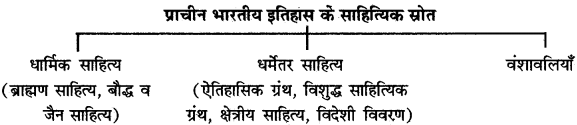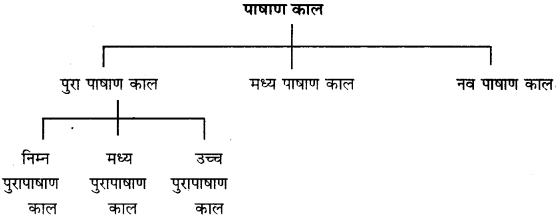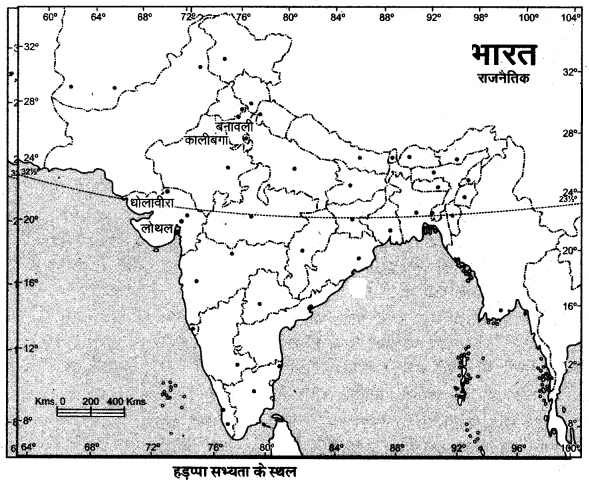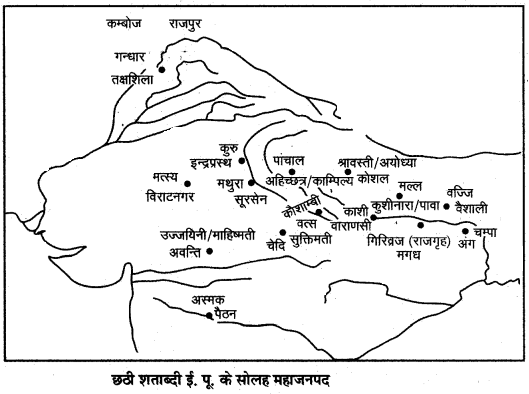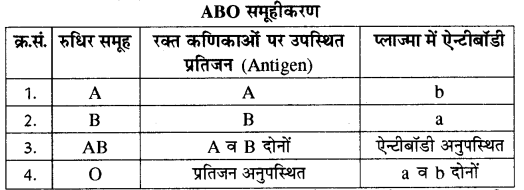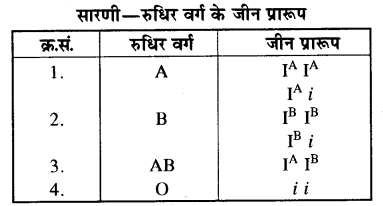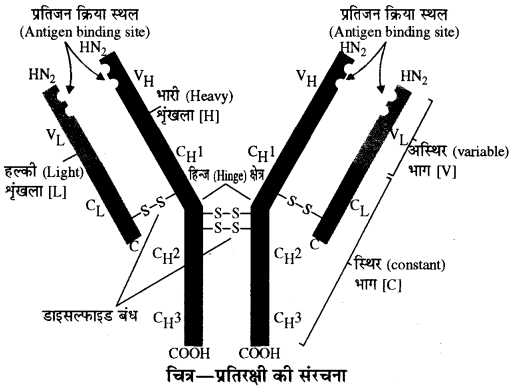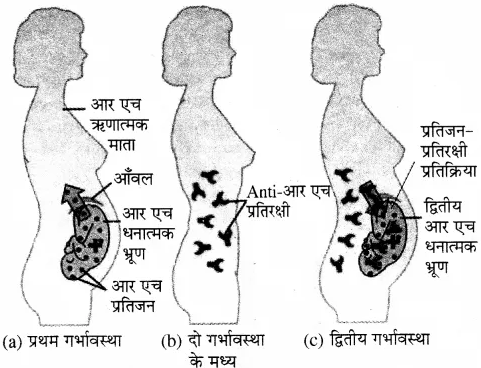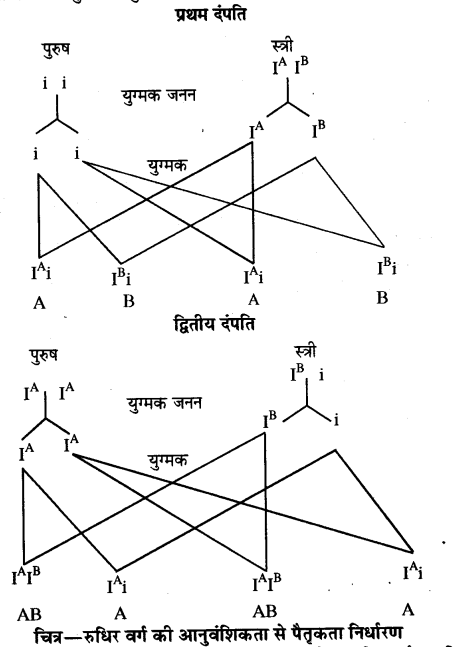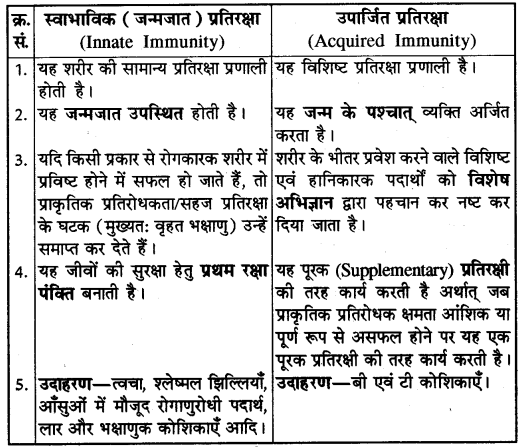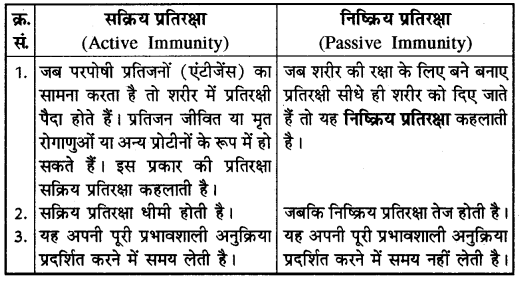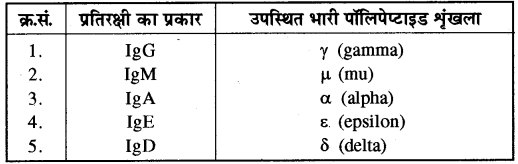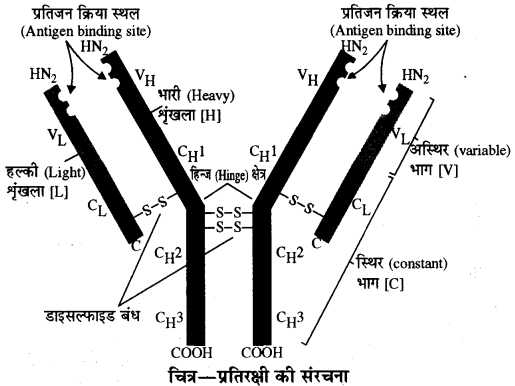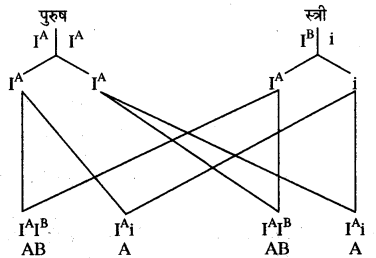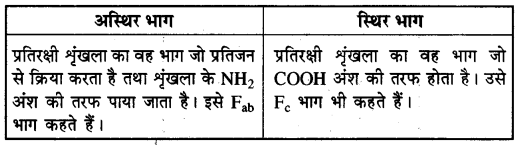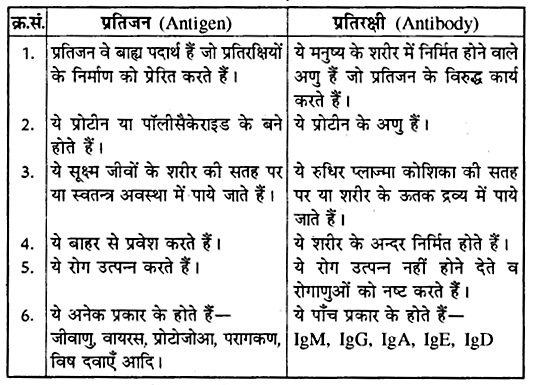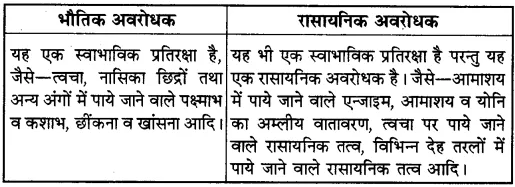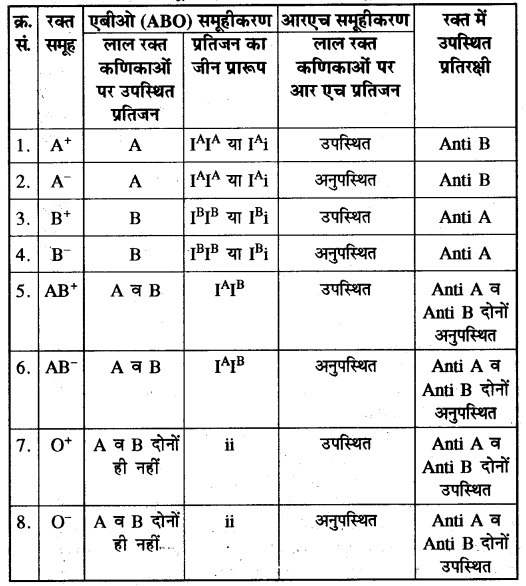![SMILE 3 CLASS 8]()
by Sheetal Panwar | Apr 19, 2021 | CLASS 10, E CONTENT, REET, STUDENT CORNER |
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST
रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक
K. L. SEN MERTA (M.Sc. M.A. B.Ed.)
SCIENCE EDUCATOR,
These Solutions for Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक are part of Solutions for Class 10 Science. Here we have given Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक
| Board |
RBSE |
| Textbook |
SCERT, Rajasthan |
| Class |
Class 10 |
| Subject |
Science |
| Chapter |
Chapter 6 |
| Chapter Name |
रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक |
| Number of Questions Solved |
144 |
| Category |
RBSE CLASS X |
आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST
1. FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है
(क) ऑक्सीकरण
(ख) अपचयन
(ग) अपघटन।
(घ) संयुग्मन
2. एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी|
(क) अपघटनीय
(ख) विस्थापन
(ग) ऑक्सीकरण
(घ) संयुग्मन
3. इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं
(क) ऑक्सीकारक
(ख) उत्प्रेरक
(ग) अपचायक
(घ) कोई नहीं
4. दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएँ हैं|
(क) ऑक्सीकरण
(ख) अपचयन
(ग) अनुक्रमणीय
(घ) उत्क्रमणीय
5. अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं
(क) उत्प्रेरक
(ख) ऑक्सीकारक
(ग) अपचायक
(घ) कोई नहीं
6. एन्जाइम होते हैं
(क) ऋणात्मक उत्प्रेरक
(ख) धनात्मक उत्प्रेरक
(ग) स्वतः उत्प्रेरक
(घ) जैव उत्प्रेरक
7. 2Mg + O2 → 2 MgO
इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है
(क) ऑक्सीकृत।
(ख) अपचयित
(ग) अपघटित
(घ) विस्थापित
8. उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है
(क) →
(ख) ↑
(ग) ↓
(घ) ⇔
9. वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है, कहलाती
(क) जैव रासायनिक
(ख) उत्क्रमणीय
(ग) स्वतः उत्प्रेरित
(घ) अनुत्क्रमणीय
10. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा
(क) निकलती है।
(ख) अवशोषित होती है।
(ग) विलेय होती है।
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तरमाला- 1. (ख) 2. (क) 3. (ग) 4. (घ) 5. (क) 6. (घ) 7. (क) 8. (घ) 9. (ग) 10. (क)
प्रश्न 11. रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर- वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संघटन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
उदाहरण- कोयले को जलाने पर CO2 गैस का बनना।
C(s) + O2(g) → CO2(g)
प्रश्न 12. वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइये।।
उत्तर- वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए निकेल (Ni) उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न 13. उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? नाम लिखें।
उत्तर- उत्प्रेरण मुख्यतः चार प्रकार का होता है-
- धनात्मक उत्प्रेरण
- ऋणात्मक उत्प्रेरण
- स्वतः उत्प्रेरण
- जैव उत्प्रेरण।
प्रश्न 14. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है?
उत्तर- यह एक विस्थापन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया है।
प्रश्न 15. रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दें।
उत्तर-
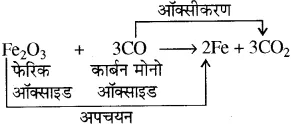
प्रश्न 16. उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं ?
उत्तर- वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है अर्थात् जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण
Na2(g) + 3H2(g) ⇔ 2NH3(g)
प्रश्न 17. उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष का क्या कार्य है?
उत्तर- उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं जबकि उत्प्रेरक विष से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है।
प्रश्न 18. अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौनसी अभिक्रिया कहलाती है?
उत्तर-
अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
प्रश्न 19. वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है?
उत्तर-
वेग के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है-
- तीव्र अभिक्रियाएँ
- मंद अभिक्रियाएँ।
प्रश्न 20. ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दें।
उत्तर-
कैल्सियम कार्बोनेट का विघटन एक ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है।
CaCO3 कैल्सियम कार्बोनेट →Δ→ CaO + CO2↑ कैल्सियम ऑक्साइड
प्रश्न 21. किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है?
उत्तर-
उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि या कमी कर देते हैं। लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं।
प्रश्न 22. रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है?
उत्तर-
रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही नष्ट। अतः सम्पूर्ण अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है।
23. रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ?
उत्तर-
वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है अर्थात् ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं, उसे रेडॉक्स या उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं।
प्रश्न 24. कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है?
उत्तर-
कोयले का दहन एक संयुग्मन अभिक्रिया है, किन्तु इस अभिक्रिया में कोयले का ऑक्सीकरण भी हो रहा है। अतः यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है।
प्रश्न 25. प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की pH कितनी होगी?
उत्तर-
समान सान्द्रता के प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की pH 7 होगी क्योंकि विलयन उदासीन हो जाएगा।
प्रश्न 26. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें।
उत्तर-
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित अन्तर हैं
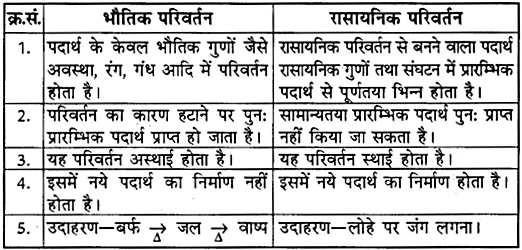
प्रश्न 27. संयुग्मन व अपघटनीय अभिक्रियाओं को एक-एक उदाहरण के साथ लिखें।
उत्तर-
(i) संयुग्मन अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयुग्मन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नये बंधों का निर्माण होता है।
इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का साधारण योग होता है अतः इन्हें योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है।
उदाहरण- कैल्सियम ऑक्साइड (बिना बुझा चूना) का जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड (बुझा हुआ चूना) बनाना।।
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq)
(ii) अपघटनीय अभिक्रियाएँ-वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर (टूट कर) दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उन्हें अपघटनीय अभिक्रियाएँ कहते हैं। इनमें अभिकारकों के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं। जिससे छोटे अणुओं का निर्माण होता है।
उदाहरण- CaCO3 (कैल्सियम कार्बोनेट) को गर्म करने पर CaO तथा CO2 गैस बनती है।
CaCO3(s)(चूना पत्थर) → CaO(s) + CO2(g)(कैल्सियम ऑक्साइड)
प्रश्न 28. AgNO3 + KCl → AgCI + KNO3
उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? नाम लिखें तथा समझाएँ।
उत्तर-
यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में विस्थापित होते हैं तथा नये यौगिक बनते हैं। अभिक्रिया–
AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3
में AgNO3, के NO3– आयन KCl के Cl– आयनों को विस्थापित कर रहे हैं जिससे सिल्वर क्लोराइड (AgCl) तथा पोटेशियम नाइट्रेट (KNO3) बन रहे हैं।
प्रश्न 29. ऑक्सीकरण व अपचयन को इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के आधार पर समझाइए।
उत्तर-
ऑक्सीकरण-ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। उदाहरण
K → K+ + e–
Fe2+ → Fe3+ + e–
2Cl– → Cl2 + 2e–
यहाँ पोटेशियम परमाणु एक e– त्याग कर K+ धनायन में, फेरस (Fe2+)
आयन एक और e– त्याग कर (Fe3+) फेरिक आयन में तथा क्लोराइड (Cl–) आयन e– त्याग कर उदासीन क्लोरीन परमाणु में ऑक्सीकृत होता है। इन अभिक्रियाओं से ज्ञात होता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है या धनायन पर आवेश बढ़ता है या ऋणायन से उदासीन परमाणु बनता है।
अपचयन-वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु, आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उसे अपचयन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण
Br + e– → Br–
MnO4– + e– → MnO4-2
Mg+2 + 2e– → Mg
यहाँ ब्रोमीन परमाणु एक e– ग्रहण कर ब्रोमाइड आयन (Br–), मैग्नेट आयन (MnO4–), एक e ग्रहण कर परमैंग्नेट आयन (MnO4-2) तथा मैग्नीशियम आयन (Mg+2) दो e– ग्रहण कर उदासीन Mg परमाणु में अपचयित हो रहे हैं। अतः अपचयन अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या धनायन से उदासीन परमाणु बनता है।
प्रश्न 30. उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? लिखें।
उत्तर-
(a) क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं
- धनात्मक उत्प्रेरक-उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।
2SO2 + O2 →NO→ 2SO3
- ऋणात्मक उत्प्रेरक-उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।
2H2O2 →ग्लिसरॉल→ 2H2O + O2
- स्वतः उत्प्रेरक-जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है अर्थात् अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उस उत्पाद को स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं।
उदाहरण
CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट + H2O ⇔ CH3COOH एसीटिक अम्ल + C2H5OH एथेनॉल
इस अभिक्रिया में CH3COOH स्वतः उत्प्रेरक है।
- जैव उत्प्रेरक-वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें एन्जाइम भी कहते हैं।
उदाहरण
NH2CONH2 यूरिया + H2O → यूरिएज → 2NH3 + CO2
(b) भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं
- समांगी उत्प्रेरक-जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है।
उदाहरण-
CH3C00CH3(l) मेथिल एसीटेट + H2O(l) →HCl(aq)→ CH3COOH(aq) एसीटिक अम्ल + CH3OH(aq) मेथिल एल्कोहॉल
2SO2(g) + O2(g) सल्फर डाईऑक्साइड → NO(g)→ 2SO3(g) सल्फर ट्राईऑक्साइड
- विषमांगी उत्प्रेरक-जब किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न-भिन्न होती है तो इस अवस्था में उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं।
उदाहरण-
N2(g) + 3H2(g) →Fe(s) →2NH3(g)
वनस्पति तेल(l) + H2(g) →Ni(s)→ वनस्पति घी(s)
सूक्ष्म विभाजित निकल धातु (Ni) की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में तेल द्रव अवस्था में, H2 गैसीय अवस्था में, Ni तथा घी ठोस अवस्था में है।
प्रश्न 31. अपघटनीय अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं? वर्णन करें।
उत्तर-
अपघटनीय अभिक्रियाओं में एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अपघटनीय अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती
(i) विद्युत अपघटन
(ii) ऊष्मीय अपघटन
(iii) प्रकाशीय अपघटन
(i) विद्युत अपघटन- जब किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित होकर कैथोड तथा एनोड पर भिन्नभिन्न उत्पाद बनाता है, तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरणजल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनती है।
2H2O(l) →विद्युत धारा→ 2H2(g) + O2(g)
2NaCl(aq) →विद्युत धारा→ 2Na(aq) + Cl2(ag)↑
(ii) ऊष्मीय अपघटन- इस अभिक्रिया में यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है। उदाहरण-कैल्शियम कार्बोनेट को 473K ताप तक गर्म करने पर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 बनाता है।
CaCO3 →Δ→ CaO + CO2 ↑
(iii) प्रकाशीय अपघटन- प्रकाशीय अपघटन में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे-छोटे अणुओं में टूट जाता है।
उदाहरण-
2HBr → H2↑ + Br2
प्रश्न 32. क्लोरोफार्म में कुछ मात्रा में एथिल एल्कोहॉल मिलाकर क्यों रखा जाता है?
उत्तर-
क्लोरोफार्म वायु की ऑक्सीजन से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। इस अभिक्रिया के वेग को कम करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में एथेनॉल (C2H5OH) मिला दिया जाता है।
2CHCl3 क्लोरोफॉर्म + O2 →C2H5OH→ 2COCl2 फॉस्जीन + 2HCl
यहाँ एथेनॉल अल्प मात्रा में बनी फॉस्जीन (COCl2) से क्रिया करके डाइएथिल कार्बोनेट तथा HCl बनाता है, जिससे अभिक्रिया धीमी हो जाती है।
2C2H5OH + COCl2 → (C2H5)2CO3 अविषाक्त + 2HCl.
प्रश्न 33. दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों?
उत्तर-
दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण के जलीय विलयन में उपस्थित दुर्बल अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होता अर्थात् कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में भी रहता है। अतः विलयन में अम्ल व क्षार के समान मोल होने पर भी प्रबल क्षार से प्राप्त OH- अधिक मात्रा में रहते हैं। अतः विलयन क्षारीय होता है। जिसकी pH 7 से अधिक होती है। उदाहरण
CH3COONa सोडियम एसीटेट + H2O → CH3COOH दुर्बल अम्ले (अल्प आयनित) + NaOH प्रबल क्षार (पूर्ण आयनित)
प्रश्न 34. क्या ये अभिक्रियाएँ संभव हैं? उत्तर कारण सहित लिखें।
(i) Cu + ZnSO4 → CuSO4 + Zn
(ii) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
उत्तर-
ये दोनों ही विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करते हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं होता।
(i) यह अभिक्रिया सम्भव नहीं है क्योंकि Cu, Zn से कम क्रियाशील धातु है अतः यह Zn को विस्थापित नहीं कर सकता।
Cu + ZnSO4 → CuSO4 + Zn
(ii) यह अभिक्रिया सम्भव है क्योंकि Fe, Cu से अधिक क्रियाशील है। अतः यह Cu को विस्थापित करके FeSO4 तथा Cu बनाता है।
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
प्रश्न 35. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण-अपचयन को पहचाहिए
- C + O2 → CO2
- Mg + Cl2 → MgCl2
- ZnO + C → Zn + CO
- Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
उत्तर-
- C + O2 → CO2– इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन O2 का अपचयन हो रहा है।
- Mg + Cl2 → MgCl2 -इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम (Mg) का अधिक विद्युतऋणी तत्व क्लोरीन (Cl2) के साथ संयोग हो रहा है अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन (Cl2) का अपचयन हो रहा है।
- ZnO + C → Zn + CO-इस अभिक्रिया में ZnO में से ऑक्सीजन निकल रही है अतः इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है।
- Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2-इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड (Fe2O3) का आयरन में अपचयन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है।
उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है अतः इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं।
प्रश्न 36. रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं? वर्णन करें।
उत्तर-
रासायनिक अभिक्रिया-वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का रासायनिक गुण तथा संघटने मूल पदार्थ से भिन्न होता है अर्थात् किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है परन्तु पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है।
उदाहरण- मैग्नीशियम के फीते का दहन
2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s) मैग्नीशियम ऑक्साइड (श्वेत चूर्ण)
रासायनिक अभिक्रियाएँ मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं
(i) संयुग्मन अभिक्रियाएँ
(ii) विस्थापन अभिक्रियाएँ।
(iii) द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ
(iv) अपघटनीय अभिक्रियाएँ
(i) संयुग्मन अभिक्रियाएँ या योगात्मक अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयुग्मन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य नये बंधों का निर्माण होता है।
उदाहरण- एथीन का हाइड्रोजनीकरण
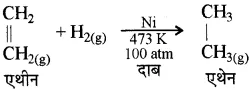
(ii) विस्थापन अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित होता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बंध टूटते हैं तथा नये बंधों का निर्माण होता है।
उदाहरण- CuSO4 नीला (कॉपर सल्फेट) + Zn जिंक → ZnSO4 रंगहीन (जिंक सल्फेट) + Cu
(iii) द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में विस्थापित होकर नये यौगिकों का निर्माण होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। इनमें दोनों अभिकारकों के कुछ भाग आपस में विस्थापित होकर नए उत्पाद बनाते हैं।
उदाहरण-
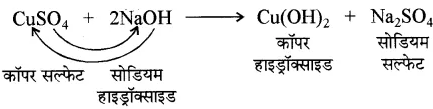
(iv) अपघटनीय अभिक्रियाएँ- वे अभिक्रियाएँ जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें अपघटनीय अभिक्रियाएँ कहते हैं। अपघटनीय अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती हैं
(a) विद्युत अपघटन
(b) ऊष्मीय अपघटन
(c) प्रकाशीय अपघटन
उदाहरण- 2NaCl(ag) →विद्युत अपघटन→ 2NaOH(aq) + Cl2(g)↑
प्रश्न 37. ऑक्सीकरण-अपचयन से क्या समझते हैं? उदाहरणों के साथ व्याख्या करें।
उत्तर-
ऑक्सीकरण तथा अपचयन को विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया जाता है
- ऑक्सीजन के संयोग एवं विलोपन (वियोजन ) के आधार पर-किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है।
उदाहरण- ऑक्सीकरण
2Mg + O2 → 2MgO
S + O2 → SO2 सल्फर डाईऑक्साइड
अपचयन-
2KClO3 → 2KCl + 3O2
- हाइड्रोजन के संयोग तथा विलोपन के आधार पर-किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है।
उदाहरण- ऑक्सीकरण
2H2S + O2 → 2H2O + 2S
इस अभिक्रिया में H2S (हाइड्रोजन सल्फाइड) गैस सल्फर (S) में ऑक्सीकृत हो रही है।
CH3CH2OH एथेनैल →[O]→ CH3CHO + H2 एथेनॉल
अपचयन-
H2 + Cl2 → 2HCl
यहाँ क्लोरीन का HCl में अपचयन हो रहा है।
- विद्युत धनी तत्त्वों के संयोग तथा विलोपन के आधार पर-वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धनी तत्व (धन विद्युती तत्व) का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण तथा विद्युत धनी तत्व का योग होता है, उसे अपचयन कहते हैं।
उदाहरण- ऑक्सीकरण
2KI + Cl2 → 2KCl + I2
H2S + Cl2 → 2HCl + S
इन अभिक्रियाओं में पोटेशियम आयोडाइड (KI) का आयोडीन (I2) में तथा H2S का सल्फर (S) में ऑक्सीकरण हो रहा है।
अपचयन-
Cl2 + Mg → MgCl2
यहाँ क्लोरीन (Cl2) का मैग्नीशियम क्लोराइड (MgCl2) में अपचयन हो रहा है।
- विद्युतऋणी तत्वों के संयोग तथा विलोपन के आधार पर-वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी पदार्थ का विद्युतऋणी.तत्व के साथ संयोग होता है, उन्हें ऑक्सीकरण तथा जब किसी पदार्थ में से विद्युतऋणी तत्व निकलता है तो उन्हें अपचयन अभिक्रियाएँ कहते हैं ।
उदाहरण- ऑक्सीकरण
Ca + Cl2 → CaCl2
यहाँ कैल्सियम (Ca) का अधिक विद्युतऋणी तत्व क्लोरीन (Cl2) के साथ संयोग हो रहा है अतः यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
अपचयन-
2FeCl3 + H2 → 2FeCl2 + 2HCl
इस अभिक्रिया में FeCl3 में से ऋण विद्युत तत्व Cl के निकलने के कारण इसका अपचयन हो रहा है।
सारांश के रूप में ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋणविद्युती तत्व का योग होता है। अथवा हाइड्रोजन या किसी अन्य धनविद्युती तत्व का निष्कासन होता है।
इसी प्रकार अपचयन वे अभिक्रियाएँ हैं जिनमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या किसी अन्य धनविद्युती तत्व का योग होता है अथवा ऑक्सीजन या किसी अन्य ऋणविद्युती तत्व का निष्कासन होता है।
आजकल ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा इलेक्ट्रॉन के आदान-प्रदान के आधार पर दी गई है।
- इलेक्ट्रॉन के आदान-प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण-वे अभिक्रियाएँ जिनमें परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उन्हें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ कहते हैं।
Na → Na+ + e–
Fe2+ → Fe3+ + e–
2Cl– → Cl2 + 2e
अतः ऑक्सीकरण की क्रिया में उदासीन परमाणु धनायन बनाता है या धनायन पर आवेश बढ़ता है या ऋणायन पर आवेश में कमी होती है।
अपचयन-वे अभिक्रियाएँ जिनमें परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन (e–) ग्रहण करता है, अपचयन कहलाती है।
Cl+e– → Cl–
MnO4-1 + e– परमैंग्नेट आयन → MnO4-2 मैंग्नेट आयन
Mg+2+2e– → Mg
अतः अपचयन अभिक्रयाओं में उदासीन परमाणु से ऋणायन बनता है या ऋणायन पर आवेश बढ़ता है या धनायन पर आवेश में कमी होती है।
उपापचयी अभिक्रिया-
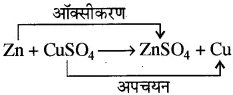
उपरोक्त अभिक्रिया में Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण (Zn → Zn+2 + 2e–) तथा कॉपर सल्फेट का Cu में अपचयन (Cu+2 + 2e– → Cu) हो रहा है।
प्रश्न 38. उत्प्रेरक की विशेषताएँ तथा उत्प्रेरक के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर-
उत्प्रेरक-वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं किन्तु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं।
उत्प्रेरक की विशेषताएँ अथवा गुण निम्न प्रकार हैं
- उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं लेकिन उनके स्वयं के रासायनिक संघटन तथा मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही आवश्यक होती है।
- प्रत्येक अभिक्रिया के लिये एक विशिष्ट उत्प्रेरक आवश्यक होता है अतः एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता।
- उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारम्भ नहीं करता है केवल उसके वेग को बढ़ाता है।
- उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र तथा प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है।
- उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा ताप में परिवर्तन से इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है।
उत्प्रेरकों के प्रकार-उत्प्रेरकों को भौतिक अवस्था तथा क्रिया के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है।
- भौतिक अवस्था के आधार पर
(a) समांगी उत्प्रेरक- जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो इस स्थिति में उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक तथा इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण
2SO2(g) + O2(g) सल्फर डाईऑक्साइड →NO(g)→ 2SO3(g) सल्फरट्राईऑक्साइड
(b) विषमांगी उत्प्रेरक- जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न-भिन्न होती है तो इस स्थिति में उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक तथा इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण
N2(g) + 3H2(g) →Fe(S)→ 2NH3(g)
- क्रिया के आधार पर
(a) धनात्मक उत्प्रेरक- वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण
2KClO3 →MnO2→ 2KCl + 3O2
(b) ऋणात्मक उत्प्रेरक- वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं।
उदाहरण-ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है। अतः हाइड्रोजन परॉक्साइड को संग्रहित करने के लिए इसमें सूक्ष्म मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाते हैं।
2H2O2 →ग्लिसरॉल → 2H2O + O2
(c) स्वतः उत्प्रेरक- जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण
CH3COOC2H5 + H2O ⇔ CH3COOH + C2H5OH
यहाँ प्रारम्भ में अभिक्रिया का वेग कम होता है परन्तु एसीटिक अम्ल (CH3COOH) के कुछ मात्रा में बनने के पश्चात् अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अतः इस अभिक्रिया में एसीटिक अम्ल स्वतः उत्प्रेरक है।
(d) जैव उत्प्रेरक- वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक (एन्जाइम) कहते हैं।
उदाहरण- माल्टोज →माल्टेज→ ग्लूकोज
प्रश्न 39. रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण व इसकी विशेषताएँ लिखें।
उत्तर-
रासायनिक समीकरण-जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाईऑक्साइड गैस बनती है।
C + O2 → CO2
रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण
- रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सर्वप्रथम क्रियाकारकों को बायीं ओर लिखकर तीर का निशान (→) लगाया जाता है, तत्पश्चात् दायीं ओर उत्पादों को लिखा जाता है।
- क्रियाकारकों और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच धन का चिन्ह (+) लगाया जाता है। जैसे
C + O2 → CO2
- अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उनके साथ कोष्ठक में ठोस के लिए (s), द्रव के लिए (l) तथा गैस के लिए (g) लिख देते हैं।
C(s) + O2(g) → CO2(g)
- अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उसके लिए (aq) लिखते हैं।
CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(aq).
- अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात् दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान ⇔ इस प्रकार लगाया जाता है।
- अभिक्रिया सम्पन्न होने के लिये आवश्यक ताप तथा दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं।
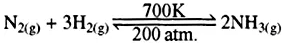
- ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ क्रमशः धनचिन्ह (+) तथा ऋण चिन्ह (-) लगाकर ऊष्मा की मात्रा को भी लिखा जाता है। ऊष्मा को चिन्ह Δ से भी लिखा जाता है।
N2 + 3H2 → 2NH3 + 10.5 kcal/mole
N2 + 2O2 → 2NO2 – 21.6 kcal/mole
- अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है।
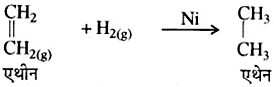
रासायनिक समीकरण की विशेषताएँ-रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं
- क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि की सम्पूर्ण जानकारी मिलती है।
- पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
- रासायनिक अभिक्रिया के लिये आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि के बारे में ज्ञात हो जाता है।
- अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी यह भी स्पष्ट हो जाता है।
- रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी भी हो जाती है।
प्रश्न 40. निम्नलिखित में अंतर बताइए
(a) उत्क्रमणीय-अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया
(b) उत्प्रेरक वर्धक-उत्प्रेरक विष
(c) समांगी-विषमांगी उत्प्रेरण
(d) ऑक्सीकरण-अपचयन।
उत्तर-
(a) उत्क्रमणीय-अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया
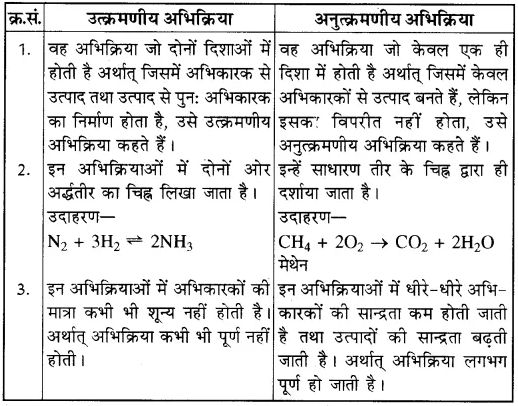
(b) उत्प्रेरक वर्धक-उत्प्रेरक विषउत्प्रेरक वर्धक ।
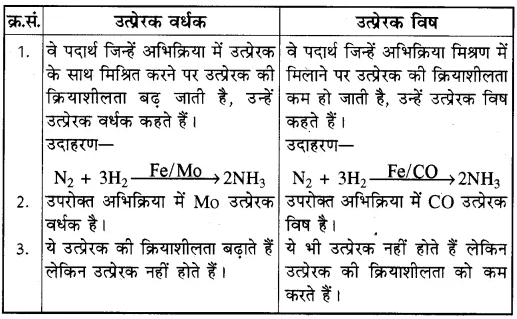
(c) समांगी-विषमांगी उत्प्रेरण
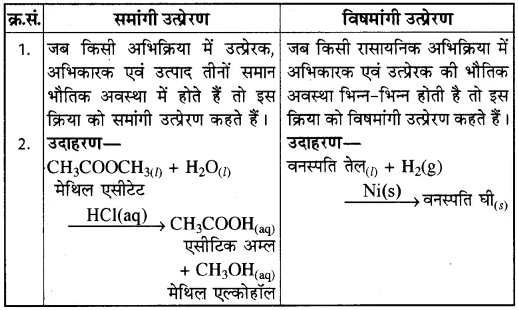
(d) ऑक्सीकरण-अपचयनक्र.सं. ऑक्सीकरण
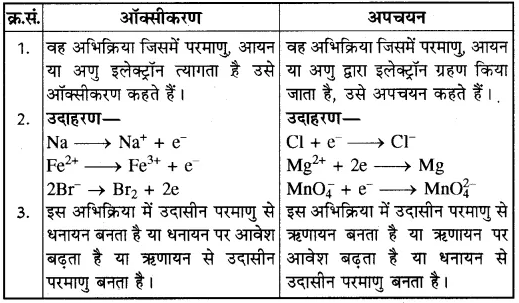
(अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर)
1. जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका
(अ) ऑक्सीकरण होता है
(ब) अपचयन होता है।
(स) अप्रभावित रहता है।
(द) जल अपघटन होता है।
2. ऊष्माशोषी अभिक्रिया है
(अ) CaO का जल में घुलना
(ब) NH4Cl का जलीय विलयन बनाना
(स) NaOH का जलीय विलयन बनाना
(द) उपरोक्त सभी
3. H2 +Cl2 → 2HCl में
(अ) H2 का अपचयन हो रहा है
(ब) H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है।
(स) Cl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है।
(द) उपरोक्त सभी
4. नीचे दी गयी अभिक्रिया के संबंध में कौनसा कथन असत्य है?
2PbO(s) + C(s) → 2Pb(s) + CO2(g)
(i) सीसा अपचयित हो रहा है।
(ii) कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत हो रही है।
(iii) कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है।
(iv) लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है।
(अ) (i) एवं (ii)
(ब) (i) एवं (iii)
(स) (i), (ii) एवं (iii)
(द) उपरोक्त सभी
5. अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की है?
(अ) संयोजन अभिक्रिया
(ब) द्विविस्थापन अभिक्रिया
(स) वियोजन अभिक्रिया
(द) विस्थापन अभिक्रिया
6. लौह-चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?
(अ) हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है।
(ब) क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रॉक्साइड बनता है।
(स) कोई अभिक्रिया नहीं होती है।
(द) आयरन लवण एवं जल बनता है।
7. अभिक्रिया-वनस्पति तेल + H2 →Ni→ वनस्पति घी, में उत्प्रेरक वर्धक है
(अ) Fe
(ब) Mo
(स) Cu
(द) Co
8. अभिक्रिया Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है?
(अ) CuSO4
(ब) Zn
(स) ZnSO4
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
9. NH4Cl के विलयन की pH होगी
(अ) 7
(ब) 7 से कम
(स) 7 से अधिक
(द) कुछ नहीं कहा जा सकता।
10. निम्न में से कौनसा भौतिक परिवर्तन नहीं है?
(अ) लोहे का चुम्बक बनना
(ब) कार्बन के जलने पर CO2 का बनना
(स) नौसादर (NH4Cl) का उर्ध्वपातन
(द) शक्कर का जल में विलेय होना ।
उत्तरमाला- 1. (अ) 2. (ब) 3. (ब) 4. (अ) 5. (द) 6. (अ) 7. (स) 8. (ब) 9. (ब) 10. (ब)
प्रश्न 1. निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए
Pb(NO3)2(s) →ऊष्मा→ PbO(s) + NO2(g) + O2(g)
उत्तर-
Pb(NO3)2(S) →ऊष्मा→ PbO(s) + 2NO2(g) + O2(g)
प्रश्न 2. चिप्स की थैली में कौनसी गैस भरी जाती है ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो सके?
उत्तर-
नाइट्रोजन गैस
प्रश्न 3. अपघटनीय अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी कारक बताइए।
उत्तर-
ताप, विद्युत तथा प्रकाश।
प्रश्न 4. पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौनसी गैस निकलती है?
उत्तर-
पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है।
2KClO3 (s) →गर्भ→2KCl(s) + 3O2(g)↑
प्रश्न 5. Pb(s) + CuCl2(aq) → PbCl2(aq) + Cu(s) किस प्रकार की अभिक्रिया है?
उत्तर-
विस्थापन एवं रेडॉक्स (उपापचयी) अभिक्रिया।
प्रश्न 6. मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है?
उत्तर-
श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड।
प्रश्न 7. मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है या अपचयित? (2Mg + O2 →2 MgO)
उत्तर-
मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है।
प्रश्न 8. CH4(g) + O2 → CO2(g) + H2O का संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा?
उत्तर-
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O (l)
प्रश्न 9. N2 तथा H2 की अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
उत्तर-
N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
प्रश्न 10. कैल्सियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है?
उत्तर-
कैल्सियम ऑक्साइड (CaO) को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है।
प्रश्न 11. कॉपर से अधिक सक्रिय तीन धातुओं के नाम लिखिए।
उत्तर-
आयरन (Fe), जिंक (Zn) तथा मैग्नीशियम (Mg)
प्रश्न 12. अभिक्रिया H2S + Br2 → 2HBr + S में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है?
उत्तर-
Br2 (ब्रोमीन) का।
प्रश्न 13. संगमरमर (Marble) का रासायनिक सूत्र क्या है?
उत्तर-
CaCO3 (कैल्सियम कार्बोनेट)।
प्रश्न 14. Zn, Pb तथा Cu की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए।
उत्तर-
Zn > Pb > Cu
प्रश्न 15. एन्जाइमों का संघटन तथा विशेषता बताइए।
उत्तर-
एन्जाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि भिन्न-भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं।
प्रश्न 16. उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कौनसी दो अभिक्रियाएँ साथ-साथ चलती हैं ?
उत्तर-
उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र अभिक्रिया तथा प्रतीप अभिक्रिया साथ-साथ चलती हैं।
प्रश्न 17. एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण बताइए।
उत्तर-
रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का वहन एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है।
प्रश्न 18. उत्प्रेरक वर्धक का एक उदाहरण दीजिए।
उत्तर-
अभिक्रिया-वनस्पति तेल + H2 →Ni/Cu→ वनस्पति घी, में Ni उत्प्रेरक तथा Cu उत्प्रेरक वर्धक है।
प्रश्न 19. सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं ?
उत्तर-
तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं।
प्रश्न 20. भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं ?
उत्तर-
वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
प्रश्न 21. दूध से दही बनना तथा तैयार सब्जी का कुछ घण्टों बाद खराब होना किस प्रकार के परिवर्तन हैं ?
उत्तर-
रासायनिक परिवर्तन।
प्रश्न 22. कॉपर सल्फेट नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर नीला रंग विलुप्त हो जाता है, क्यों ?
उत्तर-
ZnSO4 तथा Cu बनने के कारण।
प्रश्न 23. ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा लिखिए।
उत्तर-
वह अभिक्रिया जिसमें कोई स्पीशीज (तत्व, परमाणु, आयन या अणु) इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे ऑक्सीकरण तथा इन स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसे अपचयन कहते हैं।
प्रश्न 24. अपचायक किसे कहते हैं ?
उत्तर-
वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं।
प्रश्न 25. ऑक्सीकारक किसे कहते हैं ?
उत्तर-
वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं।
प्रश्न 1. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए
(i) बर्फ का पिघलना (A) एन्जाइम
(ii) उपापचयी (रेडॉक्स) अभिक्रिया (B) भौतिक परिवर्तन
(iii) जैव उत्प्रेरक (C) CuO(s) + H2(g) → Cu(s) + H2O(l)
उत्तर-
(i) (B)
(ii) (C)
(iii) (A)
प्रश्न 2. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए
(i) संयुग्मन अभिक्रिया (A) इलेक्ट्रॉन दाता पदार्थ N;
(ii) अपचायक (B) वनस्पति तेल(l) + H2(g) →Ni(s)→ वनस्पति घी(s)
(iii) विषमांगी उत्प्रेरण (C) 2Mg(s) + O2(g) → 2MgO(s)
उत्तर-
(i) (C)
(ii) (A)
(iii) (B)
प्रश्न 1. निम्नलिखित में कोई एक अन्तर लिखिए
(अ) धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक
(ब) ऊष्मीय-अपघटन एवं विद्युत-अपघटन
(स) संकलन एवं विस्थापन अभिक्रिया (माध्य. शिक्षा बोर्ड, 2018)
उत्तर-
(अ) वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं।
धनात्मक उत्प्रेरक- 2SO2 + O2 →NO→ 2SO3
ऋणात्मक उत्प्रेरक- 2H2O2 →ग्लिसरील→ 2H2O + O2
(ब) ऊष्मीय अपघटन में यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है जबकि विद्युत अपघटन में किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित होकर कैथोड तथा एनोड पर भिन्न-भिन्न उत्पाद बनाता है।
(स) संकलन (योगात्मक या संयुग्मन) अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं जबकि विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होता है।
प्रश्न 2. संयुग्मन, विस्थापन एवं अपघटनीय अभिक्रियाओं को दर्शाने वाली एक-एक रासायनिक समीकरण लिखिए। (माध्य. शिक्षा बोर्ड, मॉडल पेपर, 2017-18 )
उत्तर-
- संयुग्मन अभिक्रिया
C(s) + O2(g)→CO2(g)
- विस्थापन अभिक्रिया
CuSO4(aq) + Zn(s) → ZnSO4(aq) + Cu(s)
- अपघटनीय अभिक्रिया
2H2O(l) →विद्युत धारा→ 2H2(g) + O2(g)
प्रश्न 3. रेडॉक्स अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं? अभिक्रिया ZnO + C → Zn + CO में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन हो रहा है?
उत्तर-
रेडॉक्स अभिक्रिया-ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है अर्थात् जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएँ एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
उपरोक्त अभिक्रिया में ZnO का अपचयन तथा C का ऑक्सीकरण हो रहा है।
प्रश्न 4. अभिक्रिया CuO + H2 → Cu + H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए।
उत्तर-
अभिक्रिया CuO + H2 → Cu + H2O में H2 का ऑक्सीकरण तथा CuO का अपचयन हो रहा है।”
अन्य उदाहरण- 4Na + O2 → 2 Na2O
प्रश्न 5. (अ) रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए।
(ब) निम्न अभिक्रियाओं में A को पहचानिए
(i) Zn + CuSO4 → A + Cu
(ii) Na2SO4 + BaCl2 → A + 2NaCl
उत्तर-
(अ) CuO + H2 →Δ→ Cu+ H2O
(ब) (i) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu (जिंक सल्फेट)
(ii) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl (बेरियम सल्फेट)
अतः अभिक्रिया (i) में (A) ZnSO4 है तथा (ii) में (A) BaSO4 है।
प्रश्न 6. निम्न समीकरणों में X, Y व Z को पहचानिए
(i) Cu + CO2 →नमी→ हरा पदार्थ (X)
(ii) Ag + Y →हेवा→ काला पदार्थ (Ag2S)
(iii) FeSO4 →ऊष्मा→ Fe2O3 + SO3 + Z
उत्तर-
X = CuCO3, Y = H2S, Z = SO2
प्रश्न 7. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए
(i) CuSO4 (aq) + Fe (S) →
(ii) Zn (s) + H2SO4 (l) →
(iii) 4Na (s) + O2 (g) →
उत्तर-
(i) CuSO4 (aq) + Fe (s) → FeSO4 (aq) + Cu (s)
(ii) Zn (s) + H2SO4 (l) → ZnSO4 (aq) + H2 (g)
(iii) 4Na (s) + O2 (g) → 2Na2O (s)
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST
प्रश्न 8. निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए
(अ) कैल्सियम हाइड्रोक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड → कैल्सियम कार्बोनेट + जल
(ब) जिंक + सिल्वर नाइट्रेट → जिंक नाइट्रेट + सिल्वर
(स) ऐलुमिनियम + कॉपर क्लोराइड → ऐलुमिनियम क्लोराइड + कॉपर
(द) बेरियम क्लोराइड + पोटैशियम सल्फेट → बेरियम सल्फेट + पोटैशियम क्लोराइड
उत्तर-
संतुलित रासायनिक समीकरण
(अ) Ca(OH)2(aq) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l)
(ब) Zn(s) + 2AgNO3 (aq) → Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s)
(स) 2Al(s) + 3CuCl2(aq) → 2AlCl3(aq) + 3Cu(S)
(द) BaCl2(aq) + K2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2KCl(aq)
प्रश्न 9. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए
(i) जेल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं।
(ii) सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन (जल में ) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन (जल में) से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं।
उत्तर-
(i) BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) → 2NaCl(aq) + BaSO4(s)
(ii) NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l)
प्रश्न 10. किसी पदार्थ ‘x’ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है।
(i) पदार्थ ‘X’ का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए।
(ii) पदार्थ ‘X’ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए।
उत्तर-
(i) पदार्थ ‘X’ कैल्सियम ऑक्साइड है। जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसे चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO है।
(ii) CaO(s) + H2O(l)(बिना बुझा हुआ चूना) → Ca(OH)2(aq) (बुझा हुआ चूना) (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड)
प्रश्न 11. जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है?
उत्तर-
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इसमें लोहा (आयरन), कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है।
Fe(s) (आयरन) + CuSO4 (aq) (कॉपर सल्फेट) → FeSO4 (aq) (आयरन सल्फेट) + Cu(s) (कॉपर)
इस अभिक्रिया में लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धीरे-धीरे गायब होने लगता है।
प्रश्न 12. (a) किसी रासायनिक समीकरण की सीमाएँ बताइए।
(b) उत्प्रेरण किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए।
उत्तर-
(a) बहुत सी विशेषताओं के बाद भी रासायनिक समीकरण की निम्न सीमाएँ हैं
- यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता है।
- इससे क्रियाकारक तथा उत्पाद की सान्द्रता के बारे में स्पष्ट नहीं होता है।
(b) उत्प्रेरण-वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, परन्तु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं।
उदाहरण-
2KClO3 →MnO2→ 2KCl + 3O2
प्रश्न 13. प्रमुख तत्त्वों की सक्रियता श्रेणी लिखिए।
उत्तर-
प्रमुख तत्त्वों की सक्रियता श्रेणी
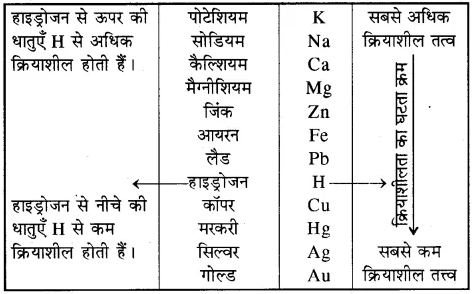
प्रश्न 14. रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? समझाइए।
उत्तर-
किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों एवं उत्पादों को तथा प्रतीकों के रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं।
वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लम्बा हो जाता है अतः इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसकी सबसे सरल विधि शब्द समीकरण होती है। जैसे-मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अतः इसका शब्द समीकरण इस प्रकार होगा
मैग्नीशियम (अभिकारक) + ऑक्सीजन → मैग्नीशियम ऑक्साइड (उत्पाद)
इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं तथा एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसे उत्पाद कहते हैं।
प्रश्न 15. संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?
उत्तर-
संतुलित रासायनिक समीकरण-संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है, जिसके दोनों पक्षों (अभिकारक एवं उत्पाद) में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्त्व-द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का न तो निर्माण होता है न ही विनाश अर्थात् किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।
जैसे- Fe + H2O → Fe3O4 + 4H2 (कंकाली समीकरण)
3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (संतुलित समीकरण)
प्रश्न 16. अपचायक तथा ऑक्सीकारक क्या होते हैं? समझाइए।
उत्तर-
वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है तथा ये इलेक्ट्रॉन त्यागकर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। अतः अपचायक इलेक्ट्रॉनदाता तथा ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉनग्राही होता है।
प्रश्न 17. क्या होता है जब? ( केवल रासायनिक समीकरण दीजिए)
(i) चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है।
(ii) जिंक धातु की सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया की जाती है।
(iii) बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है।
उत्तर-
(i) Ca(OH)2(aq) चूने का पानी। (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) + CO2(g) → CaCO3(s) (कैल्सियम कार्बोनेट) + H2O(l)
(ii) Zn (जिंक) + 2NaOH (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) → Na2ZnO2(सोडियम जिंकेट) + H2
(iii) Ca(OH)2 (बुझा हुआ चूना) कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड + Cl2 → CaOCl2 (ब्लीचिंग पाउडर) + H2O
प्रश्न 18. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर-
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया- वह अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के साथसाथ ऊर्जा/ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
उदाहरण-
(i) प्राकृतिक गैस का दहन
CH4 (g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) + ऊर्जा
(ii) श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया- वह अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा को अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
उदाहरण-
(i) N2(g) + O2(g) → 2NO(g)
(ii) शर्करा का जल में विलयन बनाना।
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST
प्रश्न 19. वियोजन (अपघटनीय) अभिक्रिया को संयोजन (संयुग्मन) अभिक्रिया के विपरीत माना जाता है, क्यों? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर-
वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे-छोटे एक से अधिक उत्पाद बनाता है जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ (तत्व या यौगिक) मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं।
संयोजन अभिक्रिया-
उदाहरण-
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
वियोजन अभिक्रिया-
2FeSO4(s) फेरस सल्फेट (हरा रंग) → Fe2O3(s) फेरिक ऑक्साइड + SO2(g) + SO3(g)
प्रश्न 20. ऑक्सीजन के संयोग तथा विलोपन के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण भी दीजिए
(a) ऑक्सीकरण
(b) अपचयन।
उत्तर-
(a) ऑक्सीकरण-
वह अभिक्रिया, जिसमें किसी पदार्थ के साथ
ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात् ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं।
ऑक्सीकरण के उदाहरण
- 2Cu(s) + O2(g) → 2CuO(s) कॉपर ऑक्साइड (काला रंग)
- C(s) + O2(g) → CO2(g)
(b) अपचयन-
वह अभिक्रिया, जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकलती है अर्थात् ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है।
अपचयन के उदाहरण
- CuO(s) + H2(g) →ताप→ Cu(s) भूरा रंग + H2O(l)
- ZnO(s) + C(s) → Zn (S) + CO (g)
प्रश्न 21. विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के उदाहरण भी दीजिए।
उत्तर-
विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अन्तर—
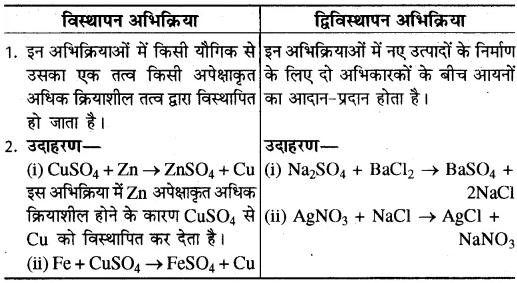
प्रश्न 22. उत्क्रमणीय अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
अभिक्रिया–A + B ⇔ C + D (उत्क्रमणीय)
उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक साथ दोनों दिशाओं (अग्र व प्रतीप) में होती है। सर्वप्रथम अभिकारकों (A+ B) से उत्पादों (C+ D) का निर्माण होता है। उपयुक्त मात्रा में उत्पाद बनते ही प्रतीप अभिक्रिया प्रारम्भ होकर पुनः अभिकारकों का निर्माण होने लगता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है तथा हर समय अभिक्रिया मिश्रण में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं । सामान्यतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया बन्द पात्र में होती है।
उदाहरण
(i) N2 + 3H2 ⇔ 2NH3
(ii) H2O + H2CO3 ⇔ H3O+ + HCO–3
प्रश्न 23. भौतिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएँ अथवा गुण बताइए।
उत्तर-
भौतिक परिवर्तन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं
- भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है।
- इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारम्भिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है।
- यह परिवर्तन अस्थायी होता है।
- इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है।
प्रश्न 24. रासायनिक अभिक्रिया से क्या आशय है? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर-
रासायनिक अभिक्रिया-वह अभिक्रिया जिसमें प्राप्त उत्पाद मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों एवं संघटन में भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है परन्तु पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण
2 Mg(s) + O2 → 2MgO(s)
मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है।
अन्य उदाहरण-
C(s) + O2(g) → CO2(g)
इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिकों के परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध टूटते हैं तथा नये बंधों का निर्माण होता है।
प्रश्न 25. रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, समझाइए।
उत्तर-
रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। जिसमें अभिक्रिया को दोनों ओर, अणुओं की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाता है।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। जैसे
C3H8 प्रोपेन + O2 → CO2 + H2O
C3H8 + O2 → 3CO2 + H2O
यहाँ C को संतुलित किया गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं तथा अन्त में ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता है।
C3H8 + O2 → 3CO2 + 4H2O
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
प्रश्न 1. अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण को समझाइए।
उत्तर-
वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं
(a) तीव्र अभिक्रिया
(b) मंद अभिक्रिया
(a) तीव्र अभिक्रिया- ये अभिक्रियाएँ अत्यन्त तेजी से सम्पन्न होती हैं। सामान्यतया ऐसी अभिक्रियाएँ आयनिक होती हैं जैसे-प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया 10-10 सेकण्ड में ही सम्पन्न हो जाती है।
NaOH प्रबल क्षार + HCl प्रबल अम्ल → NaCl + H2O (10-10sec)
AgNO3 + HCl → AgCl श्वेत अवक्षेप + HNO3
सिल्वर नाइट्रेट विलयन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन को मिलाते ही सिल्वर क्लोराइड (AgCl) का श्वेत अवक्षेप बन जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बहुत तेज होती है तथा इस अभिक्रिया का अर्द्धआयु काले (tip) 10-12 सेकण्ड होता है।
(b) मंद अभिक्रिया- वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनको पूर्ण होने में कई घंटे, दिन या वर्ष तक लग जाते हैं, उन्हें मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएँ बहुत धीमी गति से होती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया वर्षों तक चलती रहती है।
4Fe + 3O2 + 6H2O → 2Fe2O3.3H2O
अन्य उदाहरण-
2KClO3 →Δ→ 2KCl + O2
CH3COOH एसीटिक अम्ल + C2H5OH एथेनॉल → CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट + H2O
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 6 CHEMICAL REACTION & CATALYST
प्रश्न 2. सिद्ध कीजिए कि किसी अभिक्रिया में उत्पादों तथा अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है।
उत्तर-
अभिक्रिया-2Mg(s) + O2(g) →Δ→2MgO(s) में मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों में मैग्नीशियम (Mg) के परमाणुओं की संख्या 2 है तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 है और उत्पाद बनने के पश्चात् भी इनकी संख्या उतनी ही रहती है। अतः अभिक्रिया से पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात् Mg तथा 0, का द्रव्यमान समान रहता है।
अन्य उदाहरण-
अभिक्रिया-
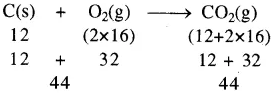
में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले का दहन हो रहा है। यहाँ कोयला (C) तथा ऑक्सीजन (O2) अभिकारक हैं । इस अभिक्रिया में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। इससे सिद्ध होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान रहता है।
प्रश्न 3. अम्ल तथा क्षार के मध्य अभिक्रिया को क्या कहते हैं ? विभिन्न प्रकार के अम्लों एवं क्षारों के मध्य अभिक्रिया का वर्णन करते हुए विलयन की pH बताइए।
अथवा
उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए।
उत्तर-
जब अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल बनता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल के हाइड्रोजन आयन (H+) क्षार के हाइड्रॉक्सिल आयन (OH-) से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं।
अम्ल + क्षार → लवण + जल
(a) प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया- जब समान सान्द्रता के प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो प्राप्त विलयन की pH 7 होती है। क्योंकि अम्ल एवं क्षार मिलाने पर विलयन उदासीन होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल से प्राप्त एक मोल H+ आयन क्षार के एक मोल OH- आयनों से क्रिया कर जल बनाते हैं अतः विलयन उदासीन हो जाता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार पूर्णतः आयनित होते हैं।
उदाहरण-
HCl + NaOH → NaCl + H2O
H+ + Cl– + Na+ + OH– → Na+ + Cl– + H2O
कुल अभिक्रिया इस प्रकार होती है
H+ + OH– → H2O
(b) दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया- दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के मध्य होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया में दुर्बल अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होता है अतः अम्ल एवं क्षार के समान मोल लेने पर भी OH- आयनों की मात्रा H+ आयनों से अधिक होती है अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात् भी विलयन में OH- आयन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं अतः विलयन की pH 7 से अधिक होती है।
उदाहरण-
CH3COOH दुर्बल अम्ल + NaOH प्रबल क्षार ⇔ CH3COONa + H2O
CH3COOH + Na+ OH– ⇔ CH3COO–Na+ + H2O
CH3COOH + OH– ⇔ CH3COO– + H2O
(c) प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के मध्य अभिक्रिया- प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया में दुर्बल क्षार पूर्णतः आयनित नहीं होता है। अतः विलयन में अम्ल तथा क्षार के समान मोल लेने पर भी H+ आयनों की मात्रा OH- आयनों की मात्रा से अधिक होती है अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात् भी विलयन में H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं इसलिए विलयन की pH 7 से कम होती है।
HCl प्रबल अम्ल + NH4OH दुर्बल क्षार → NH4Cl + H2O
H+Cl– + NH4OH + NH4+Cl– + H2O
H+ + NH4OH + NH4+ + H2O
We hope the given Solutions for Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक will help you. If you have any query regarding Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 6 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उत्प्रेरक, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
कक्षा 10 का दोहरान करने के लिए नीचे विज्ञान पर क्लिक करें
विज्ञान SCIENCE REVISION
CLCIK HERE FOR FREE MOCK TEST
CLICK HERE FOR ALL CLASS STUDY MATERIAL 2021
JOIN TELEGRAM
SUBSCRIBE US SHALA SUGAM
SUBSCRIBE US SHIKSHA SUGAM
SOME USEFUL POST FOR YOU
⇓ ⇓ ⇓
![SMILE 3 CLASS 8]()
by Sheetal Panwar | Apr 18, 2021 | CLASS 12, E CONTENT, MOCK TEST, REET, STUDENT CORNER |
RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र Human Geography Nature and Special Area

Rajasthan Board RBSE CLASS 12 HISTIRY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र
RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र Human Geography Nature and Special Area
पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर
बहुचयनात्मक प्रश्न
प्रश्न 1. आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे?
(अ) हम्बोल्ट
(ब) रिटर
(स) रेटजेल
(द) हंटिंगटन
प्रश्न 2. “मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।” परिभाषा किसने दी?
(अ) रेटजेल
(ब) एलन सैम्पल
(स) ब्लॉश
(द) कार्ल सावर
प्रश्न 3. नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं?
(अ) ग्रिफिथ टेलर
(ब) ब्लॉश
(स) मैकिण्डर
(द) हरबर्टसन
प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन फ्रांसिसी भूगोलवेत्ता नहीं है?
(अ) ब्लॉश
(ब) ब्रुश
(स) डिमांजियाँ
(द) रिटर उत्तरमाला
उत्तरमाला:
1. (स), 2. (ब), 3. (अ), 4. (द).
प्रश्न 5. मानव भूगोल के त्रि-संतुलन के घटकों के नाम बताइए।
उत्तर: जैविक, अजैविक व सांस्कृतिक घटक।
प्रश्न 6. रेटजेल की पुस्तक का नाम बताइए।
उत्तर: रेटजेल की पुस्तक का नाम एन्थ्रोपोज्योग्राफी है।
प्रश्न 7. संभववाद विचारधारा किसने दी?
उत्तर: संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी विद्वान पॉल-विडाल-डी-ला-ब्लॉश ने दी।
प्रश्न 8. प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केन्द्रों के नाम बताइए।
उत्तर: प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केन्द्रों में सिन्धु घाटी सभ्यता, मोहन जोदड़ो की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि शामिल हैं।
प्रश्न 9. मानव भूगोल के पाँच उपक्षेत्रों के नाम बताइए।
उत्तर: मानव भूगोल के पाँच उपक्षेत्रों में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, निर्वाचन (राजनीतिक) भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल एवं ऐतिहासिक भूगोल शामिल हैं।
प्रश्न 10. मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए।
उत्तर: मानव भूगोलं की प्रकृति अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत है। जीन ब्रुश के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध कीमतों से,
भू-गर्भशास्त्र का सम्बन्ध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का सम्बन्ध पौधों से है उसी प्रकार भूगोल का केन्द्र बिन्दु स्थान से है जिसमें कहाँ व क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल मानव को केन्द्रीय भूमिका का अध्ययन करता है। फ्रेडरिक रेटजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है।
उन्होंने मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के सम्बन्धों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अन्तर्गत आता है। इसी कारण मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केन्द्रीय बिन्दु के रूप में रहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के विकास (कब, क्यों, कैसे) को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है।
मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन व क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर केन्द्रित रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव के जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण के उपयोग का अध्ययन व वातावरण में किए गए बदलाबों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। सारांशत: यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल मानव व वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन मानव को केन्द्रीय भूमिका के रूप में रखकर अध्ययन कस्ता है।
प्रश्न 11. मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए।
उत्तर: इस काल में नौसंचालन सम्बन्धी कुशलताओं व खोजों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नये क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को बढ़ावा दिया जिससे विश्व के संदर्भ में विशाल ज्ञान का प्रसार हुआ। इस काल में अन्वेषण, विवरण वे प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। इस काल में मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। प्रदेशों की यह समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी इसी आधार पर भौगोलिक अध्ययन किये गए।
प्रश्न 12. मानव भूगोल के विषय-क्षेत्र का वर्णन कीजिये।
उत्तर: मानव भूगोल मानव व उससे सम्बन्धित क्रियाओं का अध्ययन जनसंख्या करने वाला विषय है। इसका विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं अन्तर्सम्बन्धित या जनता स्वरूप को दर्शाता है। मानव भूगोल सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों (राज्य, राष्ट्र, प्रदेश) में निवास करने वाली जनसंख्या व उससे सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय व ऐतिहासिक तथ्यों का समावेशित अध्ययन करती है।
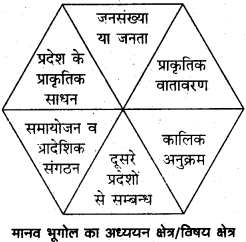
मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्यतः जनसंख्या संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक वातावरण, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण तथा कालिक विश्लेषण को शामिल किया जाता है। मानव भूगोल के इस विषय ४त्र को दिये गए चित्र से समझा जा सकता है। मानव भूगोल के इस विषय क्षेत्र को उपर्युक्त पहलुओं के आधार पर वर्णित। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र/विषय क्षेत्र किया गया है –
- जनसंख्या संसाधन/जनता व उसकी क्षमता: मानव भूगोल में जनसंख्या से सम्बन्धित दशाओं-जनसंख्या वितरण, घनत्व, जनसमूहों, जनसंख्या के प्रवास, अधिवास व उसकी प्रजातियों तथा सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता संगठन है।
- प्राकृतिक संसाधन/प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन: मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन व मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, मत्स्य रूपी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन शामिल है।
प्रश्न 13. आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइये।
उत्तर: इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पैशेल, रिचथोफेन व रेटजेल ने की। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। रेक्सल, विडाल-डी-ला-ब्लॉश, ब्रेश, दी मातन, डिमांजियाँ व फ्रेब्रे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर एवं ब्रिटेन में हरबर्टसन, मैकिण्डर, रॉक्सबी तथा फ्लुअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया।
20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। फ्रेडरिक रेटजेल जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ने मानव समांजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक सम्बन्धों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। इस काल के प्रारम्भिक दौर में मानव वातावरण सम्बन्धों का नियतिवादी, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया गया। नियतिवाद में प्रकृति के संभववाद में मानव को अधिक प्रभावी माना। 21वीं सदी के आरम्भ में नव नियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों में सामंजस्य पर जोर दिया गया।
यह विचारधारा ‘रुको व जाओ’ के नाम से भी जानी जाती है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन ‘सांस्कृतिक भूगोल’ एवं आर्थिक भूगोल’ के रूप में हुआ। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उप-शाखाओं; जैसे-राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल का उद्भव हुआ।
अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोतर
RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र Human Geography Nature and Special Area
प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है?
(अ) संसाधन भूगोल
(ब) मृदा विज्ञान
(स) मानव भूगोल
(द) नगरीय भूगोल
प्रश्न 2. मानव भूगोल का प्रादुर्भाव ब विकास किस शताब्दी से सम्बन्धित है?
(अ) 12वीं
(ब) 14वीं
(स) 16वीं
(द) 18वीं
प्रश्न 3. “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है” यह कथन किसका है?
(अ) फ्रेडरिक रेटजेल
(ब) एलन सैम्पल
(स) ब्लॉश
(द) रिटर
प्रश्न 4. संभववाद की नींव किसने रखी थी?
(अ) डी ला ब्लॉश
(ब) हंटिंगटन
(स) रेटजेल
(द) ब्रुश
प्रश्न 5. भूगोल का जनक किसे कहा जाता है?
(अ) हिकेटियम
(ब) एनेक्सीमेंडर
(स) हैरोडोट्स
(द) रेटजेल
प्रश्न 6. आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ के भूगोलवेत्ताओं ने की थी?
(अ) अमेरिकन
(व) फ्रांसीसी
(स) जर्मन
(द) यूनानी
प्रश्न 7. किस विचारधारा में प्रकृति को प्रधानता दी गई है?
(अ) निश्चयवाद
(ब) संभववाद
(स) नवनियतिवाद
(द) प्रसम्भाव्यवाद
प्रश्न 8. ‘रुको और जाओ’ की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था?
(अ) रेटजेल ने
(ब) ब्लॉश ने
(स) ग्रिफिथ टेलर ने
(द) हैरोडोट्स ने
प्रश्न 9. मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ?
(अ) 1910 के दशक में
(ब) 1930 के दशक में
(स) 1950 के दशक में
(द) 1970 के दशक में
प्रश्न 10. निम्नलिखित में जो मानव भूगोल का अंग नहीं है, वह है –
(अ) जनसंख्या भूगोल
(ब) कृषि भूगोल
(स) जलवायु विज्ञान
(द) नगरीय भूगोल
उत्तरमाला:
1. (स), 2. (द), 3. (अ), 4. (अ), 5. (अ), 6. (स), 7. (अ), 8. (स), 3. (ब), 10. (स)
निम्नलिखित में स्तम्भ अ को स्तम्भ ब मे मुमेलित कीजिए –
स्तम्भ (अ)
(भूगोलवेत्ता) |
स्तम्भ (ब)
(सम्बन्धित राष्ट्र) |
| (i) हम्बोल्ट |
(अ) ब्रिटेन |
| (ii) डिमांजियाँ |
(ब) अमेरिका |
| (iii) कार्ल सॉवर |
(स) फ्रांस |
| (iv) मैकिण्डर |
(द) जर्मन |
उत्तर: (i) द, (ii) स, (iii) ब, (iv) अ
प्रश्न 1. भूगोल किस तरह का विज्ञान है?
उत्तर: भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न 2. एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की विशेषता बताइए।
उत्तर: भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यावहारिक विषय है।
प्रश्न 3. भूगोल किसको अध्ययन करता है?
उत्तर: भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाती है।
प्रश्न 4. भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर: भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ-भौतिक भूगोल व मानव भूगोल हैं।
प्रश्न 5. भौतिक भूगोल क्या है?
उत्तर: भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें भोतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न 6. मानव भूगोल क्या है?
उत्तर: मानव भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण व संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है।
प्रश्न 7. एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: एलन सैम्पल के अनुसार, “मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।”
प्रश्न 8. डिकेन व पिट्स ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है?
उत्तर: डिकेन व पिट्स के अनुसार, “मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट अध्ययन किया जाता है।”
प्रश्न 9. मानव भूगोल की प्रकृति को कौन प्रकट करता है?
उत्तर: मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है।
प्रश्न 10. मानव भूगोल किस पर केन्द्रित रहता है?
उत्तर: मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकसमायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केन्द्रित रहता है। इसमें मानव को केन्द्र बिन्दु माना जाता है।
प्रश्न 11. हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है?
उत्तर: हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों-भौतिक दशाएँ व मानवीय अनुक्रिया के रूप में बांटा है।
प्रश्न 12.मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल तथ्यों के नाम लिखिए।
उत्तर: मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल तथ्यों में मुख्यतः जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक – संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन तथा दूसरे प्रदेशों से संबन्धों को शामिल किया गया है।
प्रश्न 13. जनसंख्या व उसकी क्षमता से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: जनसंख्या व उसकी क्षमता से तात्पर्य जनसंख्या के वितरण प्रारूप, घनत्व, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास तथा जनसंख्या की प्रजातिगत एवं सामाजिक संरचना व जनसंख्या संघटन से होता है।
प्रश्न 14.प्राकृतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: वे सभी जैविक या अजैविक घटक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं तथा जिनका मानवीय आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु प्रयोग होता है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है।
प्रश्न 15. प्राकृतिक संसाधन कौन-कौन से हैं?
उत्तर: भूमि, जल, वन व खनिज मुख्यत: प्राकृतिक संसाधन में शामिल किये जाते हैं।
प्रश्न 16. सांस्कृतिक तत्व कौन-कौन से हैं?
अथवा
सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए।
उत्तर: सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों में जीव-जन्तुओं एवं मानवे का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविको के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास, सड़कें, उद्योग व मानव की क्रियाओं से निर्मित स्वरूपों को शामिल किया जाता है।
प्रश्न 17.कालिक अनुक्रम क्या है?
अथवा
कालिक विश्लेषण से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: मानव समाज और उसके भौगोलिक सम्बन्ध स्थिर नहीं होते हैं अपितु सभी सम्बन्ध क्रियात्मक होते हैं। इन सभी सम्बन्धों का समयानुसार अध्ययन ही कालिक अनुक्रम या कालिक विश्लेषण कहलाता है।
प्रश्न 18. वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अभिन्न अंग कैसे बन गया है?
उत्तर: वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ते वातावरण अवनयने व प्रदूषण की समस्याओं के बढ़ने से वातावरण नियोजन मानव भूगोल का अभिन्न अंग बन गया है।
प्रश्न 19. मानव के अभ्युदय के साथ कौन-सी प्रक्रियाएँ प्रारम्भ हो गई थीं?
उत्तर: पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपान्तरण मानव के अभ्युदय के साथ ही आरम्भ हो गया था।
प्रश्न 20.मानव भूगोल के विषयों में दीर्घकालिक सातत्य क्यों पाया जाता है?
उत्तर: मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारम्भ की कल्पना करने पर इसकी जड़े इतिहास में अत्यंत गहरे स्वरूप को दर्शाती हैं जिसके कारण मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य/नैरंतर्य पाया जाता है।
प्रश्न 21. अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को किन-किन युगों में बांटा गया है?
उत्तर: अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को तीन युगों-प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल में बांटा गया है।
प्रश्न 22.मानव भूगोल के संदर्भ में प्राचीन काल की दशाओं को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
प्राचीन काल में मानव भूगोल का कैसा स्वरूप दृष्टिगत होता था?
उत्तर: प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच आपसी अन्त: क्रियाएं न्यून थीं। एक-दूसरे के बारे में ज्ञान कम था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप मिलती थी।
प्रश्न 23. प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव किन सभ्यताओं में देखने को मिलता है?
उत्तर: भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं में प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है।
प्रश्न 24.अरस्तू ने वातावरण के प्रभाव को किस – प्रकार स्पष्ट किया था?
उत्तर: अरस्तु के अनुसार वातावरण मानवीय चिंतन वे स्वभाव को नियंत्रित करता है। उन्होंने ठण्डे प्रदेशों के मानव को बहादुर परन्तु चिन्तन में कमजोर बताया था जबकि एशिया के लोगों को सुस्त किन्तु चिंतनशील बताया था।
प्रश्न 25.हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है?
उत्तर: हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखा था इसी कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है।
प्रश्न 26.मध्य काल में मिथक व रहस्य क्यों खुलने लगे?
अथवा
मानव भूगोल का मध्यकाल किस प्रकार एक नया काल सिद्ध हुआ?
उत्तर: मध्यकाल में नौसंचालन सम्बन्धी कुशलताओं, अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त हुईं जिससे मिथक व रहस्य खुलने लगे। इसी कारण यह काल एक नया काल सिद्ध हुआ।
प्रश्न 27.नव नियतिवाद की विचारधारा क्या है ?
उत्तर: मानव व प्रकृति दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों में सामंजस्य पर जोर देने से सम्बन्धित अवधारणा नवनियतिवाद है। इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसे ‘रुको व जाओ’ के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न 28. मानव भूगोल में कौन-कौनसी दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ?
उत्तर:मानव भूगोल में कल्याणपरक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा एवं आचरणात्मक विचारधारा का उदय हुआ था।
प्रश्न 29. आचरणपरक विचारधारा क्या है?
उत्तर: आचरणपरक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएँ करते समय हमेशा भार्थिव लाभ पर ही विचार नहीं करता बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र आवरण पर्यावरण) पर आधारित होते हैं। यही आचरणपरक विचारधारा है।
प्रश्न 1. भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ हैं। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, वन, खनिज, जल, उच्चावचों (पर्वत, पठार, मैदान) आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।
प्रश्न 2. रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है।’ रेटजेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एन्थ्रोपोज्योग्राफी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया।
प्रश्न 3. पाल विडाल-डी-ला-ब्लॉश ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है?
अथवा
ब्लॉश के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए।
उत्तर: विडाल-डी-ला-ब्लॉश, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे। जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। उनके अनुसार, “मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक सम्बन्धों को एक नया विचार देता है। जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक सम्बन्धों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है।”
प्रश्न 4. मानव भूगोल की प्रकृति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अन्तर्सम्बन्धों पर निर्भर है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहद् स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। गृह, गाँव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन (बन्दरगाह), दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएँ भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्त्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। वस्तुतः मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ-साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं।
प्रश्न 5. जीन ब्रून्श ने मानव भूगोल की प्रकृति को किस प्रकार स्पष्ट किया है?
उत्तर: प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्श के अनुसार, “जिस प्रकार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध कीमतों से, भू-गर्भशास्त्र का सम्बन्ध चट्टानों से, वनस्पतिशास्त्र का सम्बन्ध पौधों से, मानवाचार-विज्ञान का सम्बन्ध जातियों से तथा इतिहास को सम्बन्ध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केन्द्र बिन्दु स्थान है। जिसमें कहाँ’ व ‘क्यों’ जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है।”
प्रश्न 6. सांस्कृतिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? इसके तत्वों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: सांस्कृतिक वातावरण का अर्थ-पृथ्वी तल पर मानव के द्वारा प्रकृति प्रदत्त दशाओं में परिवर्तन करने से जो स्वरूप दृष्टिगत होते हैं उन्हें सांस्कृतिक वातावरण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण के तत्व-वे सब तत्व जो मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं, सांस्कृतिक वातावरण के अंग हैं। सांस्कृतिक तत्व मानव वे पर्यावरण के अन्तर्सम्बन्ध को प्रकट करते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अन्तर्गत जीव-जन्तुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि सम्मिलित हैं।
प्रश्न 7. मानव भूगोल में उपशाखाओं का उदय कैसे हुआ?
उत्तर: मानव भूगोल, भूगोल की एक मुख्य शाखा है। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। इस विभाजन का मुख्य कारण मानव भूगोल का अध्ययन अधिक सूक्ष्म रूप से करना था। मानव की क्रियाओं में विशेषीकरण की यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती रही जिसके कारण मानव भूगोल में उपशाखाओं का विकास जारी रहा। राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, संसाधन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल इसी प्रक्रिया के परिणाम हैं।
RBSE CLASS 12 GEOGRAPHY LESSON 1 मानव भूगोल: प्रकृति व विषय क्षेत्र (MANAV BHUGOL : PRAKRITI VA VISHAY KSHETR)
प्रश्न 1. मानव भूगोल का भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में उदय कैसे हुआ? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, इसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल एक समाकलनात्मक, आनुभविक व व्यावहारिक विषय है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसमें प्रकृति के साथ मानवीय अध्ययन पर जोर दिया जाता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण व संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है।
इन सभी दशाओं से मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान बन जाता है जिसमें मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक सम्बन्धों का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। इन सभी देशाओं से यह एक पूर्ण विषय को रूप धारण कर लेता है। मानव की महत्ता व सभी कार्यों में संलग्नता के कारण अंतत: मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास 18वीं शताब्दी में हो गया था। यहीं से मानव भूगोल का एक शाखा के रूप में उदय हुआ।
प्रश्न 2. मानव भूगोल मानव केन्द्रित विषय (विज्ञान) क्यों है?
उत्तर: मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक-समायोजन व क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर मुख्य रूप से केन्द्रित रहता है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या-क्या बदलाव लाता है ? इन तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। मानव के कारण ही जनसंख्या, जनसंख्या प्रदेशों व संसाधनों की रचना हुई है।
मानव ने अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन-सहन को परिवर्तित किया है साथ ही रूपान्तरण व समायोजन भी किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जो कुछ भी शामिल है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध मानव से ही है। क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों को पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन मानव को आधार मानकर किया जाता है। इन सब दशाओं के कारण ही मानव भूगोल में मानव की केन्द्रीय भूमिका मानी गई है।
प्रश्न 3. मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख पक्ष कौन-कौन से हैं?
अथवा
मानव भूगोल का विषय क्षेत्र किन बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है?
उत्तर:
मानव भूगोल के अन्तर्गत प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समुदायों के आपसी कार्यात्मक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। इसके अन्तर्गत मानव जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक उद्देश्यों, मान्यताओं तथा रीति-रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रमुख पक्षों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है –
- मानव संसाधन।
- प्रदेश में मौजूद विभिन्न प्राकृतिक संसाधन।
- मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य।
- मानव और वातावरण के मध्य आपसी समायोजन।
- विभिन्न प्रदेशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध।
- कालिक विश्लेषण।
प्रश्न 4. प्रादेशिक समायोजन को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
प्रादेशिक संगठन की प्रक्रिया क्या है? वर्णन कीजिए।
उत्तर:
पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएँ किस प्रकार वितरित हैं ? यह जानना ही आवश्यक नहीं है अपितु यह भी जानना, आवश्यक है कि उनका वितरण इस प्रकार से क्यों है? इनके बिना भूगोल का अध्ययन सार्थकता को प्राप्त नुहीं कर सकता है। ये सभी भिन्नताएँ या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती हैं या मानवीय क्रियाओं के कारण। मानव ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं से कैसे लगायी है, का अध्ययन करना भी मानव भूगोल का क्षेत्र है।
संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनके उपयोगं व संरक्षण का अध्ययन मानव भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन प्रदेश के संदर्भ में ही हो सकता है। आज वातावरण अवनयन व प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। अत: वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल का मुख्य अंग बन गया है। ये सभी दशाएं प्रादेशिक समायोजन के मिश्रित स्वरूप का ही परिणाम हैं।
प्रश्न 5. फ्रेडरिक रेटजेल के मानव भूगोल में योगदान को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
फ्रेडरिक रेटजेल आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं। इन्होंने मानव भूगोल को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने ‘एन्थ्रोपोज्योग्राफी’ नामक ग्रंथ की रचना की थी जो मानव भूगोल को इनकी विशेष देन है। इन्होंने इसे ग्रंथ में प्रादेशिक वर्णन के स्थान पर मानव भूगोल एवं भौतिक परिवेश सम्बन्धित व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किए थे। इन्होंने मानव को विकास की अन्तिम कड़ी माना था।
अपने ग्रंथ में इन्होंने मानव वितरण के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक परिवेश के कारक व तत्त्वों की सरल वे स्पष्ट व्याख्या की थी। इन्होंने निश्चयवाद का प्रबल समर्थन किया था। ये मानव की शारीरिक, मानसिक, वितरण व गतिशीलता हेतु पर्यावरणीय दशाओं को महत्त्वपूर्ण मानते थे। इन्होंने मानव के विश्व वितरण स्वरूप का वर्णन किया था। इन्होंने जलवायु के प्रभाव को मुख्य मानते हुए प्राचीन सभ्यता केन्द्रों के उद्भव एवं विकास का कारण भी इसे ही माना था।
प्रश्न 6. मानव भूगोल में 1970 के दशक के पश्चात विकसित विचारधाराओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
अथवा
मात्रात्मक क्रांति के पश्चात भूगोल में कौन-सी विचारधाराओं का विकास हुआ था? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि एवं अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते 1970 के दशक में भूगोल में निम्नलिखित तीन नई विचारधाराओं का उदय हुआ –
- कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा: मानव भूगोल की इस विचारधारा का सम्बन्ध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे।
- आमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा: मानव भूगोल की इस विचारधारा में निर्धनता के कारण, बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का सम्बन्ध पूँजीवाद के विकास से था।
- व्यवहारवादी विचारधारा: मानव भूगोल की इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर अधिक जोर दिया।
प्रश्न 1. मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति व विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
उत्तर:
मानव भूगोल की परिभाषाएँ-मानव भूगोल को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वान एवं उनके : द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं –
- रेटजेल के अनुसार, “मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच सम्बन्धों का संश्लेषित अध्ययन है।” रेटजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में भौतिक तथा मानवीय तत्त्वों के संश्लेषण पर अधिक बल दिया गया है।
- एलन सी. सैम्पल के अनुसार, “मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील सम्बन्धों का अध्ययन है।” सैम्पल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में कार्यरत मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील सम्बन्धों की व्याख्या की गयी है। सैम्पल की इस परिभाषा में सम्बन्धों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है।
- पाल विडाल-डी-लॉ-ब्लॉश के अनुसार, “मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य सम्बन्धों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को प्रस्तुत करता है।” ब्लॉश द्वारा दी गई मानव भूगोल की यह परिभाषा पृथ्वी एवं मनुष्य के अन्त:सम्बन्धों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करती है।
- अल्बर्ट डिमांजियाँ के अनुसार-“मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के सम्बन्धों का अध्ययन है।”
- लिविंग स्टोन एवं रोजर्स के अनुसार, “मानव भूगोल भौतिक/प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच सम्बन्धों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारणों एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।”
मानव भूगोल की प्रकृति:
मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अन्तर्सम्बन्धों पर टिका है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहत् स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। गृह, गाँव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्त्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। वस्तुतः मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ-साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है।
मानव भूगोल का विषय क्षेत्र:
मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीविकोपार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये गए सभी प्रयासों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आता है। अत: पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित हैं, वे सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। पृथ्वी तल पर मिलने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उसकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल के सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों का अध्ययन भी करना पड़ता है।
प्रश्न 2. प्राचीन काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइये।
उत्तर: प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच आपस में अन्योन्य क्रिया न्यून थी। एक-दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था तथा चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्त्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनैक्सीमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया।
अरस्तू ने वातावरण के प्रभाव की वजह से ठण्डे प्रदेशों के मानव को बहादुर परन्तु चिंतन में कमजोर बताया जबकि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया। इतिहासकार हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। स्ट्रेबो व उसके समकलीन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भू-पारिस्थितिकीय स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया।
CLASS 12 HISTIRY LESSON 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत (BHARAT KA VAIBHAVPURN ATIT )
(Jan Aadhaar) राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण 2021 HOW TO APPLY FOR JAN AADHAAR AT HOME ऑनलाइन आवेदन दस्तावेज
चिरंजीवी योजना / MukhyaMantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana Rajasthan | Raj Universal Health Scheme Apply Online Registration Form 2021
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 5 CHEMEISRY IN EVERYDAY LIFE
RAJASTHAN SINGLE DAUGHTER DAUBLE DAUGHTER SCHEME
CLCIK HERE FOR FREE MOCK TEST
CLICK HERE FOR ALL CLASS STUDY MATERIAL 2021
JOIN TELEGRAM
SUBSCRIBE US SHALA SUGAM
SUBSCRIBE US SHIKSHA SUGAM
(Jan Aadhaar) राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण 2021 HOW TO APPLY FOR JAN AADHAAR AT HOME ऑनलाइन आवेदन दस्तावेज
RAJASTHAN SINGLE DAUGHTER DAUBLE DAUGHTER SCHEME
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना )
SOME USEFUL POST FOR YOU
⇓ ⇓ ⇓
![SMILE 3 CLASS 8]()
by Sheetal Panwar | Apr 18, 2021 | CLASS 12, E CONTENT, MOCK TEST, REET, STUDENT CORNER |

CLASS 12 HISTIRY LESSON 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत (BHARAT KA VAIBHAVPURN ATIT )
पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर
बहुचयनात्मक प्रश्न
भारत का वैभवपूर्ण अतीत प्रश्न 1.
किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है?
(अ) अथर्ववेद
(ब) सामवेद
(स) यजुर्वेद
(द) ऋग्वेद।
उत्तर: (अ) अथर्ववेद
प्रश्न 2. ‘मिडास ऑफ गोल्ड’ पुस्तक के लेखक कौन थे?
(अ) मैक्समूलर
(ब)डी. डी. कौशाम्बी
(स) अल मसूदी
(द) अल्बेरुनी।
उत्तर: (स) अल मसूदी
12 प्रश्न 3. विक्रम सम्वत् की शुरूआत कब हुई?
(अ) 78 ई. पूर्व.
(ब) 57 ई. पूर्व.
(स) 78 ई.
(द) 130 ई.।
उत्तर: (ब) 57 ई. पूर्व.
प्रश्न 4. निम्नांकित में से कौन – सा वेदांग नहीं है?
(अ) शिक्षा
(ब) व्याकरण
(स) ज्योतिष
(द) सूत्र।
उत्तर: (द) सूत्र।
प्रश्न 5. प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रन्थ ‘युक्तिकल्पतरु’ के लेखक का नाम था?
(अ) राजा भोज
(ब) गौतमी पुत्र सातकर्णी
(स) भास्कराचार्य
(द) बाणभट्टं।
उत्तर: (अ) राजा भोज
प्रश्न 6. ऋग्वेदिक आर्यों को भौगोलिक क्षेत्र था?
(अ) ईरान
(ब) अफगानिस्तान
(स) दो आब प्रदेश
(द) सप्तसैन्धव।
उत्तर: (द) सप्तसैन्धव
प्रश्न 7.सिन्धु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं?
(अ) लोथल
(ब) राखीगढ़ी
(स) धौलावीरा
(द) मोहनजोदड़ो।
उत्तर: (स) धौलावीरा
प्रश्न 8. महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे?
(अ) समिति
(ब) सभा
(स) आसन्न प्रज्ञापक
(द) संस्थागार।
उत्तर: (द) संस्थागार।
अति लघूत्तरात्मक प्रश्नउत्तर
प्रश्न 1. लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान किन पुरातत्ववेत्ता ने प्रारम्भ किया था?
उत्तर: लुप्त सरस्वती नदी शोध अभियान प्रसिद्ध पुरातत्वविद् डॉ. वी. एस. वाकणकर ने प्रारम्भ किया था।
प्रश्न 2. दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किन – किन देशों में हुआ?
उत्तर: दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, श्याम, चम्पा, बर्मा, लंका आदि देशों में हुआ।
प्रश्न 3.अंगकोरवाट के स्मारक किस देश में स्थित हैं?
उत्तर: अंगकोरवाट के स्मारक कम्बोडिया में स्थित हैं।
प्रश्न 4. नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।
उत्तर: नवपाषाण युग में मानव पत्थर के उपकरणों की सहायता से कृषि व पशुपालन कार्य करने लगा था।
प्रश्न 5. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोग ताँबे की धातु से परिचित थे।
प्रश्न 6. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के अधिकांश लेख किस पर मिलते हैं?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता के अधिकांश लेख मुहरों पर मिलते हैं।
प्रश्न 7. आरण्यक ग्रंथों में किस विषय को प्रतिपादित किया गया है?
उत्तर: आरण्यक ग्रंथों में प्रत्येक वेद की संहिता को प्रतिपादित किया है।
प्रश्न 8. त्रिपिटक क्या हैं?
उत्तर: त्रिपिटक बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं, ये तीन हैं-सुत्तपिटक, विनयपिटक, अभिधम्मपिटक।
प्रश्न 9. दस राज्ञ युद्ध किन-किन के मध्य लड़ा गया?
उत्तर: दस राज्ञ युद्ध भरत जन के राजा सुदास तथा दस जनों के राजाओं के मध्य लड़ा गया जिसमें सुदास की विजय हुई थी।
प्रश्न 10. पंच जन में कौन-कौन से जन सम्मिलित थे?
उत्तर: पंच जन में-अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं दुह्य सम्मिलित थे।
प्रश्न 11. तीन ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए।
उत्तर: तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं-ऐतरेय, कौषितकी, शतपथ।
प्रश्न 12. प्राचीन भारत में गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले दो विद्वानों के नाम बताइये।
उत्तर: प्राचीन भारत में गणित के क्षेत्र में योगदान करने वाले दो विद्वान-
- भास्कराचार्य एवं
- बोधायन थे।
प्रश्न 13. भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणाद ने किस पद्धति का आविष्कार किया?
उत्तर: भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कणाद ने पदार्थ व उसके संघटक तत्व व गुण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।
प्रश्न 14. 16 संस्कारों के नाम बताइए।
उत्तर: 16 संस्कारों के नाम इस प्रकार हैं।
1. गर्भाधान, 2. पुंसवन, 3. सीमन्नतोनयन, 4. जातकर्म, 5. नामकरण, 6. निष्क्रमण, 7. अन्नप्राशन, 8. चूड़ाकर्म, 9. कर्णवेध, 10. विद्यारम्भ, 11. उपनयन, 12. वेदारम्भ, 13. केशान्त, 14. समावर्तन, 15. विवाह, 16. अन्त्येष्टि।
प्रश्न 15. चार पुरुषार्थ क्या है?
उत्तर: जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। वे पुरुषार्थ हैं, ये चार हैं-
- धर्म
- अर्थ
- काम व
- मोक्ष।
प्रश्न 16. आश्रम व्यवस्था क्या है?
उत्तर: व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसके जीवन की गति को चार आश्रमों में विभाजित किया गया। आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति जीवन के इन चार सोपानों-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम को पार करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है।
प्रश्न 17. दिल्ली में लौह स्तम्भ कहाँ स्थित है?
उत्तर: दिल्ली में लौह स्तम्भ मेहरौली में स्थित है।
प्रश्न 1. शैलचित्र कला के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर: आदि मानव गुफाओं, चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों जिन्हें शैलाश्रय कहा जाता है, में निवास करता था। शैलाश्रय की छतों, दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित चित्रांकन किया गया है जिन्हें शैलचित्र कहते हैं। मानव ने जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की है। इनसे प्रारम्भिक मानव के सांस्कृतिक सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों; जैसे- भीमबेटका, पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, राजस्थान में चम्बल नदी घाटी क्षेत्र, बाराँ, आलनियाँ, विलासगढ़, दर्रा, रावतभाटा, कपिल धारा, बूंदी व विराट नगर (जयपुर), हरसौरा (अलवर) व समधा आदि स्थानों पर शैलाश्रयों में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन मानवजीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करते हैं तथा हमें उस समय की संस्कृति का बोध कराते हैं।
प्रश्न 2. प्राचीन समाज व धर्म में त्रिऋण वे यज्ञ व्यवस्था को समझाइए।
उत्तर: प्राचीन भारतीय समाज में ऋण तथा यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों। संदर्भो में मनुष्य के ऋणों की चर्चा की गई है। इन ऋणों से मुक्त होने पर ही मुक्ति सम्भव है ये प्रमुख ऋण हैं
- पितृ ऋण – सन्तानोत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरन्तरता बनाकर हम पितृ ऋण की पूर्ति कर सकते हैं।
- ऋषि ऋण – ऋषियों से प्राप्त ज्ञान और परम्परा का संवर्द्धन करके हम ऋषि ऋण की पूर्ति कर सकते हैं।
- देव ऋण – देवताओं के प्रति हमारा दायित्व जिसे यज्ञादि से पूर्ण किया जाता है।
यज्ञ व्यवस्था: भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ के लिए पाँच महायज्ञों का भी प्रावधान किया गया है
(क) ब्रह्म या ऋषि यज्ञ – ऋषियों के विचारों का अनुशीलन करना।
(ख) देव यज्ञ – देवताओं की यज्ञ द्वारा स्तुति, पूजा करना, प्रार्थना करना, वन्दना करना।
(ग) पितृ यज्ञ – माता-पिता की सेवा करना तथा गुरु, आचार्य एवं वृद्धजनों का सम्मान वे सेवा करना।
(घ) भूत यज्ञ – विभिन्न प्राणियों को भोजन कराकर संतुष्ट करना व अतिथियों की सेवा करना।
(ङ) नृप यज्ञ – सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।
प्रश्न 3. महाजनपद से क्या तात्पर्य है? 16 महाजनपदों के नाम लिखिए।
उत्तर: ऋग्वैदिक काल में जन (कबीला) का स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था परन्तु उत्तर वैदिक काल तक आते-आते कृषि क्रान्ति के परिणामस्वरूप स्थायी जीवन को बढ़ावा मिला तथा जन बसना शुरू हो गये, जिन्हें जनपद कहा गया। बुद्ध के काल तक जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था तथा भू-विस्तार के लिए आपसी संघर्ष होने लगा। निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गये और जनपदों ने महाजनपदों का रूप ले लिया।
ये 16 महाजनपद थे:
अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जि संघ, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवन्ति, गान्धार तथा कम्बोज।
प्रश्न 4. सभा व समिति क्या थी ?
उत्तर: वैदिक युग में राजतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित थी। राजा राज्य की सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा को शासन कार्य में सहायता देने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित ‘सभा’ और ‘समिति’ नामक दो परिषदें होती थीं। ये परिषदें राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएँ थीं। समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा होती थी जिसमें महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति की बैठकों में राजा भी भाग लेता था। समिति की तुलना में सभी छोटी संस्था थी जिसमें ज्येष्ठ एवं विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। सभा अनुभवी वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी जो राजा को परामर्श एवं न्याय कार्य में सहयोग करती थी।
प्रश्न 5. उपनिषदों में किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है?
उत्तर: उपनिषद् भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन के मूलाधार हैं। उपनिषद् समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं चाहे वह वेदान्त हो या सांख्य या जैन धर्म या बौद्ध धर्म उपनिषदों को भारतीय सभ्यता का अमूल्य धरोहर माना जाता है। उपनिषदों में ऋषियों द्वारा खोजे गये उत्तर हैं जिनमें निराकार, निर्विकार असीम अपार को अंतदृष्टि से समझने और परिभाषित करने की अदम्य आकांक्षा के लेखबद्ध विवरण मिलते हैं। उपनिषद् चिन्तनशील एवं कल्पनाशील मनीषियों की दार्शनिक रचनाएँ हैं। उपनिषदों में वास्तविक वैदिक दर्शन का सार है। उपनिषद् में आत्म और अनात्म तत्वों का निरूपण किया गया है जो वेद के मौलिक रहस्यों का प्रतिपादन करता है।
प्रश्न 6. भारतीय इतिहास की जानकारी में विदेशी साहित्य का योगदान बताइए।
उत्तर: प्राचीनकाल से ही भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक विरासत ने विश्व के देशों को आकर्षित किया है। भारत की राजनीति, धर्म व दर्शन के अध्ययन हेतु भी कई विदेशी यात्री भारत आये और उन्होंने भारत के सम्बन्ध में पर्याप्त विवरण दिया इनमें प्रमुख थे
- यूनानी राजदूत मेगस्थनीज जो चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसने अपनी पुस्तक ‘इंडिका’ में मौर्य प्रशासन, समाज व आर्थिक स्थिति के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य यूनानी लेखकों टेसियंस, हेरोडोटस, निर्याकस, ऐरिस्टोब्युलस, आनेक्रिटस, स्ट्रेबो, ऐरियन आदि लेखक भी प्रमुख हैं।
- चीनी यात्रियों में फाह्यान, सुंगयन, ह्वेनसांग एवं इत्सिग का वृत्तान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये चीनी यात्री जिस शासक के शासनकाल में भारत आये उनके ग्रंथ तत्कालीन शासन व्यवस्था को उजागर करते हैं।
- तिब्बती वृत्तान्तों में तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथ, मसूदी का मिडास ऑफ गोल्ड’ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।
- अरबी लेखकों में मसूदी ने अपनी पुस्तक ‘मिडास ऑफ गोल्ड’ में भारत का विवरण दिया है। सुलेमान नवी की पुस्तक ‘सिलसिलात उल तवारीख’ में पाल प्रतिहार शासकों का विवरण मिलता है।
- अल्बेरुनी की सबसे महत्वपूर्ण कृति ‘तारीख उल हिन्द’ में भारतीय समाज व संस्कृति की विस्तृत जानकारी मिलती है।
प्रश्न 7. भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए सिक्कों का महत्व बताइए।
उत्तर: प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के ताँबे तथा चाँदी के हैं। इन पर केवल चित्र है, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती थी। मौर्यकालीन, कुषाणकालीन तथा गुप्तकालीन सिक्के तत्कालिक शासन व्यवस्था की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सिक्कों से हमें निम्नलिखित वस्तु स्थितियों के सम्बन्ध में जानकारियाँ मिलती हैं-
- शासकों के नाम
- तिथिक्रम निर्धारण
- शासकों के चित्र
- वंश परम्परा
- शासकों के गौरवपूर्ण कार्य
- धार्मिक विश्वास की जानकारी
- कला की जानकारी
- शासकों की रुचियों का ज्ञान
- व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी
- साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान
- नवीन तथ्यों का उद्घाटन।
प्रश्न 8. वेदांग साहित्य क्या है? स्पष्ट करिए।
उत्तर:
वैदिक साहित्य को भली-भाँति समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदांग हिन्दू धर्म ग्रंथ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द और निरुक्त-ये छः वेदांग हैं।
- शिक्षा – इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि है।
- कल्प – वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसके बारे में कल्प में बताया गया है। इसकी तीन शाखायें हैं-स्रोतसूत्र, ग्रहसूत्र और धर्मसूत्रं हैं।
- व्याकरण – इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त-अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है।
- निरुक्त – वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक उल्लेख निरुक्त में किया गया है।
- ज्योतिष – इससे वैदिक यज्ञों एवं अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से अर्थ वेदांग ज्योतिष से है।
- छन्द – वेदों में प्रयुक्त गायत्री उष्णिक आदि छन्दों की रचना का ज्ञान छन्दशास्त्र से होता है।
छन्द को वेदों का पाद, कल्पे को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुख कहा गया है।
प्रश्न 9. सिन्धु स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ बताइये।
उत्तर:
सिन्धु सभ्यता एवं संस्कृति विशुद्ध भारतीय है। इस सभ्यता का उद्देश्य रूप और प्रयोजन मौलिक एवं स्वदेशी है। उत्खनन द्वारा जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर सिन्धु सभ्यता की जो विशेषताएँ उभरकर आयीं वे निम्नलिखित हैं
- व्यवस्थित नगर नियोजन सिन्धु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो व अन्य प्रमुख पुरास्थलों से प्राप्त अवशेषों को देखने से स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के निर्माता नगर निर्माण की कला से परिचित थे।
- मकानों आदि से गन्दा जल निकालने की यहाँ उत्तम व्यवस्था थी। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की ढुकी. हुई नालियाँ बनी हुई मिली हैं। प्रत्येक छोटी नाली बड़ी नाली में और बड़ी नालियाँ नाले में जाकर मिलती थी। इस प्रकार नगर का सारा गन्दा जल नगर से बाहर जाता था।
- मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है जिसका आकार 39 × 23 × 8 फीट है।
- हड़प्पा व मोहनजोदडों से विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं जिनका आकार क्रमशः 55 × 43 मीटर तथा 45.71 x 15.23 मीटर है।
- धौलावीरा से 16 छोटे – बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं जिनसे जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी मिलती है।
- लोथल से पक्की ईंटों का डॉक यार्ड मिला है जिसका आकार 214 x 36 मीटर है तथा गहराई 3.3 मी. है। इसके उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते थे।
प्रश्न 10. आरण्यक साहित्य क्या है?
उत्तर:
संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा हमें सम्पूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या चार है-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वे अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के चार भाग-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् हैं। आरण्यक ग्रंथों की रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गयी है। इन ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। इनमें मुख्य रूप से आत्मविद्या और रहस्यात्मक विषयों के विवरण हैं। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। ये वेद मंत्र तथा ब्राह्मण का सम्मिलित अभिधान है।
प्रश्न 11. सिन्धु सरस्वती कालीन प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए।
उत्तर:सिन्धु निवासी विभिन्न शिल्प कलाओं एवं उद्योगों से परिचित थे। इनका औद्योगिक जीवन उन्नत था। सिन्धु सभ्यता में सूत कातना, सूती वस्त्रों की बुनाई, आभूषण निर्माण, बढ़ईगिरी, लुहार का कार्य, कुम्भकार का कार्य आदि व्यवसाय विकसित थे। यहाँ से उत्खनन में मछली पकड़ने के काँटे, आरियाँ, तलवारें, चाकू, भाले, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि यहाँ धातु उद्योग विकसित था। सिन्धु सभ्यता के लोग बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे। मनका निर्माण उद्योग भी विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। ये मनके सोने-चाँदी, ताँबे, पीली मिट्टी, शैलखड़ी, पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाये जाते थे। इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें मिली हैं जो अधिकांशतः सेलखड़ी से बनी हैं।
प्रश्न 12.सिन्धु सरस्वती सभ्यता की मुहर निर्माण कला की विशेषताएँ बताइये।
उत्तर:सिन्धु सरस्वती सभ्यता में उत्खनन से लगभग 2500 मुहरें प्राप्त हुई हैं। ये लाख, पत्थर तथा चमड़े आदि की बनी हुई हैं। यहाँ से प्राप्त मुहरें मुद्रा निर्माण कला के समुन्नत होने का संकेत देती हैं। इन मुहरों पर पशुओं (एक सींग का पशु, बाघ, हाथी, साँड, गैंडा), पेड़-पौधे, मानव आकृतियाँ आदि के चित्र हैं जो हमें उस समय की मानव गतिविधियों और धर्म का संकेत देते हैं। इन मुहरों के अग्रभाग पर पशु का अंकन एवं संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है तथा पीछे एक घुण्डी बनी हुई है जो सम्भवतया टाँगने के काम आती थी।
प्रश्न 13. कौटिल्य ने किन विषयों को इतिह्मस में सम्मिलित किया है?
उत्तर: कौटिल्य ने इतिहास में पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया है। उनकी प्रसिद्ध कृति ‘अर्थशास्त्र’ में तत्कालीन राजप्रबन्ध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है।
प्रश्न 14. मृदपात्र संस्कृतियों के नाम बताइये।
उत्तर: पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। प्राप्त औजारों एवं मृदभाण्डों से हम भारत में मानव विकास की यात्रा को समझ सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन में चार मृद्भाण्ड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं
- गेरुए रंग युक्त मृद्भाण्ड संस्कृति
- काली व लाल मृद्भाण्ड परम्परा
- चित्रित स्लेटी रंग की मृद्भाण्ड संस्कृति
- उत्तरी काली चमकीली परम्परा।
प्रश्न 15. प्राचीन भारत में समुद्री यात्राएँ व नौका शास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं?
उत्तर:
भारत में प्राचीन काल से ही समुद्री मार्गों, बन्दरगाहों, जलयानों आदि का व्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व रहा है। पाँच-छः हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बन्दरगाह थे; जैसे- लोथल (गुजरात), पेरीप्लस में चोल दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोटायम्, कोणार्क, मच्छलीपट्टनम् एवं कावेरीपट्टनम आदि। इन बन्दरगाहों से भारत का व्यापार मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों के साथ होता था। सिन्धु सभ्यता की अनेक मुहरों व पात्रों पर जलपोतों के प्राप्त चित्र भी प्राचीन भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का प्रमाण हैं।
अनेक विदेशी यात्री; जैसे- वास्कोडिगामा, फाह्यान, ह्वेनसांग आदि ने आवागमन में भारतीय जलमार्ग का प्रयोग किया। नौका शास्त्र-राजा भोज द्वारा रचित पुस्तक युक्तिकल्पतरु में नौका निर्माण एवं नौकाओं के प्रकार का विस्तृत उल्लेख हैं। दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग किया गया। मेगस्थनीज ने भी नौ दलों के नौका संगठन का उल्लेख किया है। नौकाओं का समूह जब सागर में चलता था तो नौकाध्यक्ष उस समूह का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार तथा पतवार सँभालने वाले को नियामक कहा जाता था।
प्रश्न 16. वंशावली क्या है?
उत्तर: घंशावली व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह व्यक्ति के पूर्वजों के सम्बन्ध में जानकारी देती है। वंशावली लेखक हर जाति, वर्ग के घर – घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है।
प्रश्न 1. प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातत्व का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रिया-कलापों का अध्ययन करना है। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है
1. उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष:
पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही मुख्य स्रोत हैं। प्राप्त औजारों एवं मृदभाण्डों से हम भारत में मानव विकास की यात्रा को समझ सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में चार मृदभाण्ड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं।
- गेरुए रंग युक्त मृदभाण्ड संस्कृति
- काली व लाल मृदभाण्ड परम्परा
- चित्रित स्लेटी रंग की मृद्भाण्ड संस्कृति
- उत्तरी काली चमकीली परम्परा।
उत्खनन से सड़कें, नालियाँ, भवन, ताँबे व कांस्य के बने औजार, बर्तन व आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं जिससे तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है।
2. अभिलेख:
तिथियुक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेखों का विशेष महत्व है। इनमें सम्बन्धित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है। अभिलेखों में सबसे प्रमुख अशोक द्वारा लिखवाये गये लेख हैं जो शिलालेखों, स्तम्भ लेखों तथा गुहालेखों तीन रूपों में मिलते हैं।
अन्य प्रमुख अभिलेख खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख, चन्द्रगुप्त का महरौली स्तम्भ लेख, स्कन्दगुप्त का भितरी स्तम्भ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ लेख, प्रभावती गुप्त को ताम्र लेख आदि हैं।
3. सिक्के व मुद्राएँ:
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रह्म है। इनसे शासकों के नाम, तिथियाँ, चित्र, वंश परम्परा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी मिलती है। सिक्कों के साथ ही मुहरें भी प्रचलित थीं। इन पर राजा, सामन्त, पदाधिकारीगण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर तथा नाम होते थे।
4. स्मारक व भवन:
पुरातात्विक स्रोतों के अन्तर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मन्दिर, राजप्रासाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं। इससे उस समय की कला, संस्कृति व राजनैतिक जीवन की जानकारी मिलती है।
5. मूर्तियाँ, शैलचित्र कला व अन्य कलाकृतियाँ:
उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो उस समय के धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती हैं। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैलचित्र प्राप्त हुए हैं जिनसे प्रारम्भिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है।
प्रश्न 2. प्राचीन भारतीय वैभव की जानकारी में वैदिक साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर: विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद हैं। वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है और यही वेद वैदिक सभ्यता के आधार स्तम्भ हैं। वेदों के द्वारा हमें सम्पूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है-श्रेष्ठ या उत्तम। वेदों से हमें इन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति भारत में हुई तथा वे भारत से ईरान और यूरोप की ओर गए।
वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई जो भारतीय संस्कृति का वैभव है। प्राचीन काल में जितना साहित्य संस्कृत में लिखा गया उतना अन्य भाषा में नहीं मिलता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में न किया गया हो। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। हमारे ऋषियों ने लम्बे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया है। इसलिए वेदों को संहिता कहा गया है। वेदों की संख्या चार हैं-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद है। इसमें 10 अध्याय और 1028 सूक्त हैं।
इसमें छन्दों में रचित देवताओं की स्तुतियाँ हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता व ऋषि का उल्लेख है। सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। इसके 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नये हैं शेष ऋग्वेद के हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाये जाते हैं। यज्ञों, कर्मकाण्डों व अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह यजुर्वेद में है। इसमें 40 अध्याय हैं एवं शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद दो भाग हैं। अन्तिम वेद अथर्ववेद में 20 मण्डल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गयी। इसका अन्तिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिन्तन हैं।
प्रत्येक वेद के चार भाग हैं-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। यज्ञ और कर्मकाण्डों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वे ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाते हैं। आरण्यक ग्रंथों की रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई। इनमें दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है।
वैदिक साहित्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई जिसके छः भाग हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द एवं ज्योतिष। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद व शिल्पवेद चार उपवेद भी हैं जिनसे चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वेद ज्ञान के समृद्ध भण्डार हैं तथा प्राचीन भारतीय समाज के स्वरूप को परिलक्षित करते हैं।
प्रश्न 3. प्राचीन भारत में विज्ञान व कला के क्षेत्र में समृद्धता पर निबन्ध लिखिए।
उत्तर: प्राचीन भारतीय संस्कृति कला व विज्ञान के क्षेत्र में प्रारम्भ से उत्कृष्ट रही है। कला व विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों ने भारत ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व को लाभान्वित किया है। कला व विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों का अध्ययन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं।
1. कला के क्षेत्र में समृद्धता:
भारतीय कलाकारों की अपने विचारों और भावनाओं की सुन्दर एवं कलात्मक अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति-परम्परा की बेजोड़ कड़ी है। कला के उत्कृष्ट प्रमाण सिन्धु सरस्वती सभ्यता में भी मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त मुहरों एवं बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी देखने को मिलती है। मिट्टी से बने मृभाण्ड, मृणमूर्तियाँ, मुहर निर्माण, आभूषण निर्माण आदि इस सभ्यता के उत्कृष्ट कला प्रेम के उदाहरण हैं।
वैदिक काल में अयस् धातु को आग में पिघलाकर उसे पीट कर विभिन्न आकार देने में यहाँ के लोग सक्षम थे। ऋग्वेद में हिरण्य (सोना) से विभिन्न आभूषण बनाये जाने का उल्लेख है। आभूषणों में कर्णशोभन व निस्क (स्वर्णमुद्रा या मूल्य की इकाई का आभूषण) बनाये जाते थे। वैदिक आर्य कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे। इस काल में काष्ठ कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी कला के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। इन धर्मों के अनुयायियों द्वारा भारत के विभिन्न भागों में निर्मित मन्दिर, मठ, चैत्य, विहार, स्तूप, मूर्तियाँ गुफाएँ भारतीय कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। कौलवी की बौद्ध गुफाएँ, साँची, भरहुत एवं अमरावती के स्तूप, कन्हेरी (मुम्बई), कालें भाजा (मुम्बई-पुणे के मध्य) के चैत्य विहार बौद्धकला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मूर्तिकला की दृष्टि से गांधार व मथुरा कला विशेष उल्लेखनीय है। सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजन्ता के भित्ति चित्र चित्रकला की दृष्टि से विश्व विख्यात हैं।
2. विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियाँ:
विज्ञान के विभिन्न विषयों; जैसे-चिकित्सा विज्ञान, खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, गणित तथा रसायन विज्ञान आदि पर लिखे गये ग्रंथों से परवर्ती लोगों को अत्यन्त सहायता मिली तथा इन ग्रंथों का अरबी, लैटिन व अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद, जिसे ऋग्वेद का एक उपवेद कहा जाता है की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। आयुर्वेद के त्रिधातु सिद्धान्त, त्रिदोष सिद्धान्त, पंच भौतिक देह व उसका पुरुष प्रकृति सम्बन्ध, सांख्य दर्शन का सप्तधातु सिद्धान्त आज भी उपयोगी है। चरक, सुश्रुत, धनवन्तरि, बाग्भट्ट इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वान थे।
आर्यभट्ट की वर्गमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, पाई का चार दशमलव तक मान, ब्रह्मगुप्त के घात के विस्तार का सूत्र, बोधायन के शुल्वसूत्र में क्षेत्रफल के सूत्र तथा चिति प्रमेय सिद्धान्त, वर्ग सूत्र एवं आपस्तम्ब कात्यायन द्वारा वृत्त के ग्राफ को नापने की विधि आदि गणित के क्षेत्र में भारतीयों की विश्व को अमूल्य देन है।
भारतीय पंचाग प्रणाली, प्राचीन ज्योतिषविदों द्वारा प्रतिपादित चन्द्र द्वारा पृथ्वी को परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर बारह राशियाँ, सत्ताईस नक्षत्र, तीस दिन का चन्द्र मास, बारह मास का वर्ष, चन्द्र व सौरवर्ष में समन्वय हेतु तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के द्वारा समायोजन आदि सिद्धान्त आज भी यथावत् हैं।
भौतिकी क्षेत्र में कणाद ऋषि ने अणु सिद्धान्त, पदार्थ व उसके संघटक तत्व व गुण का सिद्धान्त तथा अणुओं के संयोजन की विशद धारणा प्रस्तुत की। पदार्थ, कार्यशक्ति, गति व वेग आदि विषयक भौतिक सिद्धान्त प्राचीन ऋषियों व विद्वानों ने दिये। प्राचीन काल में भारतीयों को रासायनिक मिश्रण का भी ज्ञान था। इसका उदाहरण मेहरौली का लौह स्तम्भ है जो आज भी उसी अवस्था में हैं।
प्रश्न 4. प्राचीन भारत में राजनैतिक तंत्र व गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए।
उत्तर: प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्येक काल में भिन्न-भिन्न रूपों में देखा गया जो निम्नलिखित हैं
1. सिन्धु सभ्यता का राजनीतिक जीवन:
सिन्धु सभ्यता की लिपि अपठनीय होने के कारण इस काल के राजनीतिक जीवन का निर्धारण करना दुष्कर है। खुदाई में प्राप्त विभिन्न भग्नावशेषों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासियों का जीवन सुखी और शांतिपूर्ण था। नागरिकों को सार्वजनिक रूप से अधिकाधिक सुख सुविधाएँ उपलब्ध थीं।
2. वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था:
वैदिक काल में व्यवस्थित राजनैतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। वैदिक युग में राजतन्त्रीय शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा को शासन कार्य में सहायता देने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित सभा और समिति नामक दो परिषदें होती थीं। वैदिक काल में राष्ट्र-जन-विश-ग्राम-कुल राजनैतिक संगठन का अवरोही क्रम था।
3. महाकाव्य काल:
इस काल में भी राजतन्त्रीय शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजा का पद वंशानुगत था तथा उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद् भी होती थी। इस समय कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है जिसमें-अन्धक, वृष्णि, कुकुर और भोज प्रमुख थे।
4. महाजनपद काल:
इस काल में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ। ऋग्वैदिक काल में जन (कबीले) का स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था। उत्तर वैदिक़ काल में जन बसना शुरू हो गये। अतः ये जनपद कहे जाने लगे। जनपदों में भू-विस्तार के लिए आपसी संघर्ष होने लगा। निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गये और जनपदों ने महाजनपदों का रूप ले लिया। बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। इन महाजनपदों में दस राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी शेष में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी।
बौद्ध कालीन गणराज्यों के विधान और शासन पद्धति में गणराज्य का राजा या प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता था। उपराजा भण्डारिक एवं सेनापति राजा की सहायता करते थे। गणतन्त्रों की न्यायिक व्यवस्था भी विशेष प्रकार की होती थी। इसमें अपराधी की जाँच-पड़ताल सात न्यायिक अधिकरियों द्वारा की जाती थी तथा उसके बाद ही उसे दण्ड दिया जाता था।
हमारी वर्तमान संसदीय एवं संवैधानिक व्यवस्था में महाजनपदकालीन गणतंत्रीय व्यवस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन यह व्यवस्था लम्बे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकी। कालान्तर में मौर्य शासक चन्द्रगुप्त ने केन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कर सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक राजनैतिक इकाई के रूप में संगठित किया।
प्रश्न 5. प्राचीन काल में भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के विश्व में प्रसार का वर्णन कीजिए।
उत्तर: भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारम्भिक काल से गौरवमयी रही है। उत्खनन एवं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी हमें भारतीय संस्कृति का विश्व स्वरूप दिखायी देता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं
- चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है ‘यक्षों’ के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करें।
- पश्चिमी इतिहासकारों म्यूर, सरवाल्टर रैले, कर्नल अल्काट, फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर, मैक्समूलर आदि ने भी भारतीय संस्कृति एवं इतिहास की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में अपने उद्गार प्रकट किये हैं।
- चम्पा, अनाम पाण्डरेग, इन्द्रपुर बाली, कलिंग जैसे; नगरों के नाम या राम, बर्मा जैसे व्यक्तियों के नाम भारतीय परम्परा से अटूट सम्बन्ध दर्शाते हैं।
- कम्बोडिया के अंगकोरवाट के स्मारक, जावा के बोरोबुदूर के मन्दिर अन्य देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रमाण देते हैं।
प्राचीन काल में भारत भूमि और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएँ अफगानिस्तान से लेकर सम्पूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्म देश, श्याम, इण्डोनेशिया, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, बोर्निओ, फिलीपीन्स, जापान एवं कोरिया तक पहुँचे और वहीं अपना राजनैतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्रशान्त महासागर के द्वीपों से ऐसे ही अन्य नाविक मध्य अमेरिका के मैक्सिको, हांडुरास, दक्षिण अमेरिका के पेरु, बोलीविया तथा चिली के विभिन्न स्थानों पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपने निवास बनाये।
पश्चिमी भारत के बन्दरगाहों से द्रविड़ पर्यटक तथा नाविक सोमालीलैण्ड से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी समुद्र तट पर जगह – जगह अपने वास स्थल बनाने में सफल हुए। इसी प्रकार भारतीय शूरवीरों की एक शाखा ने तिब्बत, मंगोलिया, सिंक्यान, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया और चीन पहुँचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव जमाया। पश्चिम की ओर गंधार, पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की तथा दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलीस्तीन पहुँचकर भी भारतीयों ने अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया।
इस प्रकार सुसंस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल तथा थल मार्ग से पहुँचे तथा वहाँ उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता का प्रचार कर वहाँ के निवासियों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जिसके परिणामस्वरूप निम्न साम्राज्यों व संस्कृतियों का उदय हुआ
- कौण्डिन्य नाम के वीर ने फूनान संस्कृति का निर्माण किया।
- कम्बु ने कम्बोडिया पहुँचकर साम्राज्य स्थापित किया।
- चम्पा और अनाम के बलाढ्य हिन्दू राज्य उदित हुए।
- सुमात्रा में श्रीविजय के वैभवपूर्ण साम्राज्य का उदय हुआ।
- अश्ववर्मन नामक साहसी वीर बोनिओ पहुँचा तथा उसने अपनी संस्कृति का विस्तार किया।
इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत वैदिक ग्रंथों आदि का विश्व में प्रसार किया। इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, इण्डोचाइना, बोर्निओ से संस्कृत भाषा के सैकड़ों लेख मिले हैं। यहाँ के शिव, विष्णु व बौद्ध मन्दिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। इन देशों को रहन – सहन परम्परा, पूजा पद्धति, शास्त्र विधि, नीति कल्पना, आचारे व्यवहार आदि में भारतीय परम्परा की झलक मिलती है।
प्रश्न 6. प्राचीनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस कथन के सम्बन्ध में प्राचीन भारत के आर्थिक वैभव को रेखांकित करिए।
उत्तर: भारत की आर्थिक समृद्धता हमारे वैभवशाली अतीत को दर्शाती है। आर्थिक समृद्धता के कारण प्राचीनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राचीन भारत कृषि, खनिज, प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण था जो इसकी आर्थिक समृद्धि का आधार थे। लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे।
1. कृषि:
भारत सदैव एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि एवं पशुपालन भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। ऋग्वेद में जुताई, बुवाई, फसल की कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खाद्यान्नों के उत्पादन का उल्लेख है। इनसे तत्कालीन समय की उन्नत कृषि के संकेत मिलते हैं। कुल्याओं (नहरों) का भी उल्लेख मिलता है जो उत्तम सिंचाई व्यवस्था को इंगित करते हैं।
2. पशुपालन:
वैदिक काल में लोग कृषि के साथ पशुपालन भी किया करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि इनके प्रमुख पाल्य पशु थे। महाकाव्य काल तक आते आते पशुपालन तकनीकी में विकास के संकेत मिलते हैं।
3. उद्योग:
प्राचीन काल में आभूषण निर्माण, कपड़ा, बर्तन तथा चमड़ा उद्योग विकसित अवस्था में थे। इस समय मुद्रा का भी प्रचलन हो गया था। वैदिक काल में हस्तशिल्प उद्योगों का सर्वाधिक महत्व था। भौतिक समृद्धि और मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार नये – नये हस्तशिल्प उद्योगों का विकास हुआ था। स्त्रियाँ भी इन व्यवसायों में रुचि लेती थीं जैसे- कपड़ा बुनना, रंगना, बर्तन निर्माण आदि। इस समय के नये प्रमुख उद्योग मछली पकड़ना, रस्सी बटना, स्वर्णकारी, वैद्यगिरी और रंगसाजी आदि थे। इस काल में लोगों को धातुओं का व्यापक रूप से ज्ञान था जिनका प्रयोग वे औजार, हथियार तथा आभूषण बनाने में करते थे।
4. व्यापार:
प्राचीन भारत में व्यापार भी काफी उन्नत था। एक प्रसंग में इन्द्र की प्रतिमा का मूल्य 10 गायें बताया गया है। ऋग्वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख है। तेतरीय उपनिषद् में अधिक अन्न उपजाने का संदेश दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कृषि की नई तकनीकी का विकास हुआ। इस काल में अनेक व्यावसायिक संघों का चलन भी अस्तित्व में आ गया। श्रेष्ठी, गज, गणपति शब्द का प्रयोग इसी सन्दर्भ में हुआ है।
5. कर:
महाकाव्य काल में यह प्रमाण मिलता है कि उपज का 1/6 से 1/10 भाग कर के रूप में देना होता था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ एवं समृद्धशाली थी जिसके संसाधनों ने चिरकाल तक सम्पूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया।
प्रश्न 7. भारत के प्राचीन धार्मिक वैभव पर एक निबन्ध लिखिए।
उत्तर: धार्मिक विशेषताओं एवं समृद्धि के कारण ही भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त था। वैदिक कालीन सभी देवी देवता तीन वर्गों में विभाजित थे
- स्वर्गवासी देवता (आकाशवासी) – द्यौस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, ऊषा, मित्र, विष्णु, अश्विन।
- पार्थिव देवता (पृथ्वीवासी) – पृथ्वी, अग्नि, सोम, वृहस्पति सरस्वती आदि।
- वायुमण्डलीय देवता (अन्तक्षवासी) – वरुण, वात, इन्द्र, रुद्र, पर्जन्य, मारुत।
इन देवताओं की उपासना प्रार्थना, स्तुति तथा यज्ञ के माध्यम से की जाती थी।
प्रकृति पूजा:
ऋग्वेद में अनेक ऐसी ऋचाएँ हैं जिनसे पता चलता है कि इन प्राकृतिक शक्तियों की देव रूप में उपासना अन्त में सम्पूर्ण प्रकृति के देवता की उपासना में परिवर्तित हो गयी। प्रकृति की बहुदैवीय शक्तियों की उपासना होते हुए भी ईश्वर की परम एकता पर बल दिया जाता था।
यज्ञ:
प्रार्थना तथा स्तुति के द्वारा देवताओं की पूजा करने के अतिरिक्त आर्य लोग यज्ञ भी करते थे। यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करके वे मंत्रोच्चारण के साथ हवन करते थे। आर्यों का धर्म मानव कल्याण के लिए था। ये लोग प्रकृति के रूप में अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हुए बहुदेववादी होते हुए भी सभी देवताओं को परम परमात्मा का अंश मानते थे। इस दृष्टि से वे एकेश्वरवादी थे। उपनिषदों के दर्शन के अनुसार ब्रह्म से सम्पूर्ण जगत की उत्पति हुई है और यह जगत पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाता है। आत्म का ब्रह्म में विलय होना ही मोक्ष कहलाता है।
उपनिषद् हमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह – त्याग, मन व बुद्धि को निर्मल बनाने और सादगी व सदाचारी जीवन जीने का संदेश देते हैं। हमारे अनेक महापुरुषों रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उपनिषद् दर्शन की विवेचना की है। श्रीमद्भागवत जैसे; धर्म, दर्शन व नीति के उत्कृष्ट ग्रंथ ने नैतिकतापूर्ण आचरण पर विशेष बल दिया तथा फल की कामना के बिना कर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। नि:संदेह भारतीय धार्मिक दर्शन का मानव कल्याण व राष्ट्र कल्याण में अमूल्य योगदान है।
प्रश्न 8. भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियों का महत्व बताइये।
उत्तर: वंशावली लेखन परम्परा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। यह एक ऐसी परम्परा है जिसमें वंशावली लेखक हर जाति, वर्ग के घर-घर जाकर प्रमुख लोगों की उपस्थिति में संक्षेप में सृष्टि रचना से लेकर उसके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश क्रम हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। वंशावली लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी एवं भाट, तीर्थ पुरोहित पण्डे, बारोट आदि प्रमुख हैं। ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से वंशावलियाँ निम्नलिखित रूप से विशेष महत्वपूर्ण हैं
- पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावलियाँ प्रामाणिक दस्तावेज एवं न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियों इत्यादि को सुसंगत न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है।
- पुरातन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में वंशावलियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। कई ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण वंशावलियों से मिलते हैं।
- समाज जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानता है, उनकी जानकारी भी हमें वंशावलियों से प्राप्त होती है।
- समाज के आर्थिक जीवन के विकास, लोगों के व्यवसाय आदि का उल्लेख भी वंशावली लेखकों द्वारा किया गया है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परम्परा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुलधर्म, कुलाचार, गोत्र वे पूर्वजों के नाम प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत वंशावलियाँ ही हैं।
- वंशावलियों द्वारा धर्मान्तरित हिन्दुओं को अपनी जड़ों का परिचय देकर आपसी विद्वेष को कम किया जा सकता है।
इससे धार्मिक उन्माद और अलगाववाद को कम करके देश में साम्प्रदायिक सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वंशावलियों के माध्यम से हमें इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। वंशावली लेखन परम्परा की शुरूआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी जो हजार वर्षों से आज भी अनवरत जारी है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
वस्तुनिष्ठ प्रश्न[/su_heading]
प्रश्न 1. वेदों की संख्या कितनी है?
(क) तीन
(ख) चार
(ग) दो
(घ) पाँच।
उत्तर: (ख) चार
प्रश्न 2. यज्ञ और कर्मकाण्डों पर आधारित साहित्य …………. कहलाते हैं।
(क) ब्राह्मण ग्रन्थ
(ख) आरण्यक
(ग) उपनिषद्
(घ) पुराण।
उत्तर: (क) ब्राह्मण ग्रन्थ
प्रश्न 3. पुराणो की संख्या कितनी है?
(क) सत्रह
(ख) उन्नीस
(ग) नौ
(घ) अट्ठारह।
उत्तर: (घ) अट्ठारह।
प्रश्न 4. सिंहलद्वीप के इतिहास को वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है-
(क) दीपवंश
(ख) महावंश
(ग) दीपवंश व महावंश दोनों में
(घ) सुत्तपिटक।
उत्तर: (ग) दीपवंश व महावंश दोनों में
प्रश्न 5. जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है?
(क) पाली भाषा
(ख) प्राकृत भाषा
(ग) हिन्दी भाषा
(घ) संस्कृत भाषा।
उत्तर: (ख) प्राकृत भाषा
प्रश्न 6. कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन-सा है?
(क) हर्षचरित
(ख) राजतरंगिणी
(ग) अर्थशास्त्र
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर: (ग) अर्थशास्त्र
प्रश्न 7. यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है?
(क) बाणभट्ट
(ख) ह्वेनसांग
(ग)फाह्यान
(घ) इत्सिंग।
उत्तर: (ख) ह्वेनसांग
प्रश्न 8. किस पुराण में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा गया है?
(क) अग्निपुराण
(ख) भागवत पुराण
(ग) मत्स्य पुराण
(घ) गरुड़ पुराण।
उत्तर: (क) अग्निपुराण
प्रश्न 9. सबसे प्राचीन वेद कौन – सा है?
(क) ऋग्वेद
(ख) अथर्ववेद
(ग) सामवेद
(घ) यजुर्वेद।
उत्तर: (क) ऋग्वेद
प्रश्न 10. मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन-सी है?
(क) स्नानागार
(ख) राजप्रसाद
(ग) अन्नागार
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर: (ख) राजप्रसाद
प्रश्न 11. हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में किस विद्वान का सहयोग प्राप्त था?
(क) राखालदास बनर्जी
(ख) मैकडॉनल्ड
(ग) दयाराम साहनी
(घ) एन. जी. सजूमदार।
उत्तर: (ग) दयाराम साहनी
प्रश्न 12. हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन-सा है?
(क) हड़प्पा
(ख) मोहनजोदड़ो
(ग) धौलावीरा
(द) लोथल।
उत्तर: (क) हड़प्पा
प्रश्न 13. सिंधु सरस्वती सभ्यता में खोजे गए स्थलों में कितने स्थल भारत में है?
(क) 388
(ख) 917
(ग) 517
(घ) 920.
उत्तर: (ख) 917
प्रश्न 14. हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से बना डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है?
(क) कालीबंगा
(ख) धौलावीरा
(ग) लोथल
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर: (ग) लोथल
प्रश्न 15. रथ की आकृति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है?
(क) लोथल
(ख) दैमाबाद
(ग) धौलावीरा
(घ) मोहनजोदड़ो।
उत्तर: (ख) दैमाबाद
प्रश्न 16. मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु वासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?
(क) आर्य
(ख) द्रविड
(ग) मेलूहा
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर: (क) आर्य
प्रश्न 17. सिन्धु सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी?
(क) कुल
(ख) वेश
(ग) परिवार
(घ) ग्राम।
उत्तर: (ग) परिवार
प्रश्न 18. ‘History of Sanskrit literature’ पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) मैकडॉनल्ड
(ख) अल्काट
(ग) वी. एस बाकणकर
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर: (क) मैकडॉनल्ड
प्रश्न 19. उपपुराणों की संख्या कितनी है?
(क) 20
(ख) 21
(ग) 29
(घ) 30.
उत्तर: (ग) 29
प्रश्न 20. वैदिक काल में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएँ कौन-सी थीं?
(क) सभा
(ख) समिति
(ग) सभा व समिति दोनों
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर: (ग) सभा व समिति दोनों
प्रश्न 21. वर्ण व्यवस्था में वर्गों का मुख्य आधार क्या था?
(क) व्यवस्था
(ख) ज़न्म
(ग) जाति
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर: (क) व्यवस्था
प्रश्न 22. धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है?
(क) 5
(ख) 8
(ग) 10
(घ) 7.
उत्तर: (ख) 8
उत्तरमाला:
1. (ख), 2. (क), 3. (घ), 4. (ग), 5. (ख), 6. (ग), 7. (ख), 8. (क), 9. (क), 10. (अ), 11. (ग), 12, (क), 13. (ख), 14. (ग), 15. (ख), 16. (क), 17. (ग), 18. (क), 19. (ग), 20. (ग), 21. (क), 22. (ख)।
CLASS 12 HISTIRY LESSON 1 BHARAT KA VAIBHAVPURN ATIT
सुमेलित प्रकार के प्रश्न उत्तर
सुमेलित कीजिए-
(I)
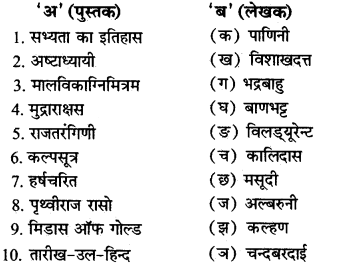
उत्तरमाला:
1. (ङ), 2. (क), 3. (च), 4. (ख), 5. (झ), 6. (ग), 7. (घ), 8. (अ), 9. (छ) 10. (ज)।
(II)
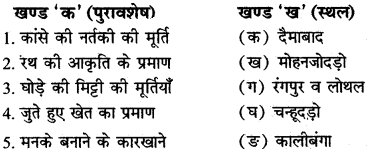
उत्तरमाला:
1, (ख), 2. (क), 3. (ग), 4. (ङ), 5. (घ)।
प्रश्न 1. भारत के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए।
उत्तर: भारत के पश्चिम में हिन्दूकुश सफेदकोह, तुर्कमान तथा किर्थर पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं।
प्रश्न 2. इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
उत्तर: इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य मानव संस्कृति का अध्ययन करना होता है।
प्रश्न 3. साक्ष्य किसे कहते हैं?
उत्तर: अतीत की जानकारी के लिए इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है, उन्हें साक्ष्य कहते हैं।
प्रश्न 4. भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
उत्तर: भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है-
- साहित्यिक स्रोत।
- पुरातात्विक स्रोत।
प्रश्न 5. प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण कीजिए।
उत्तर: प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यक स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।
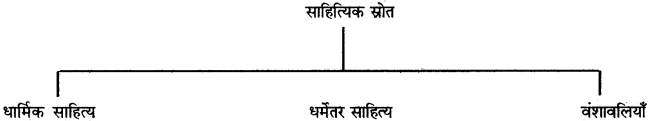
- धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य आते हैं।
- धर्मेतर साहित्य के अन्तर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध हैं साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य व विदेशी विवरण आते हैं।
- वंशावलियाँ इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं।
प्रश्न 6. सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइये।
उत्तर: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।
प्रश्न 7. वेदों की संख्या कितनी है नामोल्लेख कीजिए।
उत्तर: वेदों की संख्या चार हैं-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद।
प्रश्न 8. आर्यों द्वारा गाये जाने वाले छन्दों का विवरण किस वेद में मिलता है?
उत्तर: आर्यों द्वारा गाये जाने वाले छन्दों का विवरण सामवेद में मिलता है।
प्रश्न 9. वेदांग साहित्य के कितने भाग हैं?
उत्तर: वेदांग साहित्य के छः भाग हैं-शिक्षा, कल्पे, व्याकरण, निरुक्त, छन्दं एवं ज्योतिष।
प्रश्न 10 पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताइये।
उत्तर: पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है।
प्रश्न 11. सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताइये।
उत्तर: मत्स्य पुराण।
प्रश्न 12.पुराणों के पाँच विषय कौन-कौन से हैं?
उत्तर: पुराणों के पाँच विषय हैं-सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवन्तर, वंश व वंशानुचरित।
प्रश्न 13. पुराणों का रचयिता किन्हें माना जाता है।
उत्तर: पुराणों का रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र अग्रश्रवा को माना जाता है।
प्रश्न 14. बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए।
उत्तर: बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटिक है-ये तीन हैं-सुत्तपिटक, विनयपिटक व अभिधम्म पिटक।
प्रश्न 15. प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थों मिलिन्दपन्ह, दीपवंश व महावंश की रचना किस भाषा में की गई?
उत्तर: प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों मिलिन्दपन्हों, दीपवंश व महावंश की रचना पाली भाषा में की गयी।
प्रश्न 16. गौतम बुद्ध के जीवन – चरित्र पर आधारित ग्रन्थों का नाम बताइये।
उत्तर: महावस्तु ग्रन्थ, बुद्ध चरित्र, मंजुश्री मूलकल्प, सौन्दरानन्द।
प्रश्न 17. ‘हिस्ट्री ऑफ दी वार’ पुस्तक के लेखक कौन हैं?
उत्तर: ‘हिस्ट्री ऑफ दी वार’ पुस्तक के लेखक एरिस्टोब्युलस हैं।
प्रश्न 18. प्राचीन काल में भारत आने वाले प्रमुख चीनी यात्रियों के नाम बताइये।
उत्तर: प्राचीन काल में भारत आने वाले प्रमुख चीनी यात्री-फाह्ययान, सुंगयुन, हवेनसांग एवं इत्सिग हैं।
प्रश्न 19. प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत कौन-कौन से हैं?
उत्तर: प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत-अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मुहरें, स्मारक, मूर्तियाँ व मंदिर तथा शैल चित्रकला हैं।
प्रश्न 20. अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गये हैं?
उत्तर: अशोक के अभिलेख खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गये हैं।
प्रश्न 21. अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम बताइए।
उत्तर: अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर तथा बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधि था।
प्रश्न 22.किस पुस्तक में नौका निर्माण का उल्लेख मिलता है?
उत्तर: राजा भोज द्वारा रचित युक्ति कल्पतरु पुस्तक में नौका निर्माण एवं नौकाओं के प्रकार का उल्लेख मिलता है।
प्रश्न 23. इतिहास एवं प्राक् इतिहास किसे कहा जाता है?
उत्तर: जब से मानव ने पढ़ना – लिखना सीखा तब से वर्तमान तक के क्रियाकलापों को ‘इतिहास’ तथा इससे पूर्व के मानव के क्रियाकलाप को ‘प्राक् इतिहास’ कहा जाता है।
प्रश्न 24. पाषाण काल किसे कहते हैं?
उत्तर: जिस काल में मनुष्य पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उस काल को पाषाणकाल कहते हैं।
प्रश्न 25.पाषाण युग को कितने भागों में बाँटा गया है?
उत्तर: पाषाण युग को तीन भागों में बाँटा गया है-
- पुरापाषाण काल।
- मध्यपाषाण काल।
- नवपाषाण काल।
प्रश्न 26. आदि मानव ने कृषि तथा पशुपालन करना किस काल में सीखा?
उत्तर: आदि मानव ने कृषि तथा पशुपालन करना नव पाषाण काल में सीखा।
प्रश्न 27. शैलचित्र क्या हैं?
उत्तर: शैलश्रयों की दीवारों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित चित्रांकन किया गया, जिन्हें शैलचित्र कहते हैं।
प्रश्न 28. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसके निर्देशन में हुई?
उत्तर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ई. में कनिंघम के निर्देशन में हुई।
प्रश्न 29. मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय किसे जाता है?
उत्तर: मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है। इन्होंने 1922 ई. में मोहनजोदड़ो का पता लगाया था।
प्रश्न 30.वैदिक काल में कौन-सी नदी लोगों के जीवन का आधार थी?
उत्तर: वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी।
प्रश्न 31. सिन्धु सरस्वती सभ्यता को यह नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ?
उत्तर: इस सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार सिन्धु नदी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। इसलिए इसे सिन्धु सरस्वती सभ्यता कहा गया।
प्रश्न 32. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के उन चार स्थलों के नाम लिखिए जो आधुनिक भारत में नहीं हैं?
उत्तर: आधुनिक भारत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो तथा सुत्कागेण्डोर नामक स्थल स्थित नहीं हैं। ये पाकिस्तान में स्थित हैं।
प्रश्न 33. सिन्धु सरस्वती सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन-सी है?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी उचित जल निकास व्यवस्था थी।
प्रश्न 34. सिन्धु सरस्वती सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह कौन-सा था?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बन्दरगाह लोथल था।
प्रश्न 35.किन्हीं चार भौतिक साक्ष्यों के नाम बताइये जो पुरातत्वविदों को सिन्धु सभ्यता के लोगों के जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निमित करने में सहायक होते हैं।
उत्तर:
- मृदभाण्ड
- आभूषण
- औजार
- घरेलू सामान।
प्रश्न 36. सिन्धु सरस्वती सभ्यता में खोपड़ी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता में खोपड़ी के अवशेष कालीबंगा तथा लोथल से मिले हैं।
प्रश्न 37. नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है?
उत्तर: नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
प्रश्न 38.सिन्धु सरस्वती सभ्यता में किन फसलों का उत्पादन होता था?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता में गेहूँ, जौ, ज्वार, दाल, मटर, रागी, साम्बा, कपास, खजूर, तिल, चावल आदि का उत्पादन होता था।
प्रश्न 39 . मनके बनाने के कारखानों का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है?
उत्तर: मनके बनाने के कारखाने लोथल व चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए है।
प्रश्न 40. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के व्यापारिक सम्बन्ध किस अन्य देश के साथ थे?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता के व्यापारिक सम्बन्ध मेसोपोटामिया के साथ थे।
प्रश्न 41.‘हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिट्रेचर’ के लेखक कौन हैं?
उत्तर: ‘हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिट्रेचर’ के लेखक मैकडॉनल्ड हैं।
प्रश्न 42. यज्ञीं, कर्मकाण्डों व अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह किस वेद में है?
उत्तर: यज्ञों, कर्मकाण्डों व अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह यजुर्वेद में है।
प्रश्न 43.अन्तिम वेद कौन – सा है? इसकी रचना किसने की?
उत्तर: अन्तिम वेद अथर्ववेद है। इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गयी।
प्रश्न 44. नौकाओं के प्रकार का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है?
उत्तर: राजा भोज द्वारा रचित ‘युक्ति कल्पतरु’ पुस्तक में।
प्रश्न 45.वैदिक काल में राजनैतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या थी?
उत्तर: वैदिक काल में राजनैतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई कुल थी।
प्रश्न 46 . महाजनपद काल के चार शक्तिशाली जनपद कौन-से थे?
उत्तर: महाजनपद काल के चार शक्तिशाली जनपद-कोसल, मगध, वत्स और अवन्ति थे।
प्रश्न 47. सोलह महाजनपदों में कितने राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी?
उत्तर: सोलह महाजनपदों में 10 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन,प्रणाली थी।
प्रश्न 48. चार वर्षों का उल्लेख किस वेद में किया गया है?
उत्तर: चार वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र) का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के दसवें मण्डल में किया गया है।
प्रश्न 49. वर्ण भेद व्यवस्था को आधार क्या था?
उत्तर: वर्ण भेद व्यवस्था का आधार कर्म था।
प्रश्न 50.आश्रम व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर: आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों का समान रूप से समन्वयीकरण करना था।
प्रश्न 51. संस्कार किसे कहते हैं?
उत्तर: भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है, उन्हें संस्कार कहा जाता है।
प्रश्न 52.वेदों के प्रमुख विषय क्या हैं?
उत्तर: वेदों के तीन प्रमुख विषय हैं- ईश्वर, आत्मा एवं प्रकृति।
प्रश्न 53.पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धान्त किसने प्रतिपादित किया?
उत्तर: पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धान्त आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया।
प्रश्न 54. कणाद ऋषि कौन थे?
उत्तर: कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन के रचयिता एवं अणु सिद्धान्त के प्रवर्तक थे।
प्रश्न 55. आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है?
उत्तर: आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है।
प्रश्न 56.दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ?
उत्तर: दशमलव प्रणाली एवं शून्य को आविष्कार भारत में हुआ।
प्रश्न 1. भारतवर्ष के उत्तर में कौन-कौन से पर्वतीय स्थल हैं?
उत्तर: भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें बल्ख, बदरखाँ, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूँ, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊँची पर्वत श्रेणियाँ हैं।
प्रश्न 2. इतिहास क्या है तथा इसके अन्तर्गत किन विषयों को रखा जाता है?
उत्तर: इतिहास अतीत की घटनाओं का कोलक्रम है। इतिहास के अन्तर्गत मानव के क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित किया जाता है। अतीत का प्रत्यक्षीकरण करना सम्भव नहीं है। अतः साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। इतिहास में मानव का सम्पूर्ण अतीत समाहित रहता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित हो, इसके अन्तर्गत विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, धर्म व दर्शन आदि विषयों को रखा जाता है।
प्रश्न 3. साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते समय इतिहासकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर: साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते समय इतिहासकारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए
- ग्रन्थ की भाषा क्या है, जैसे-पाली, प्राकृत, तमिल अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों एवं विशेष वर्ग की भाषा थी।
- ग्रन्थ किस प्रकार का है-मंत्रों के रूप में अथवा कथा के रूप में।
- ग्रन्थ के लेखक की जानकारी प्राप्त करना जिसके दृष्टिकोण एवं विचारों से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है।
- इन ग्रन्थों के श्रोताओं को भी इतिहासकार को परीक्षण करना चाहिए क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा।
- ग्रंथों के सम्भावित संकलन एवं रचनाकाल की जानकारी प्राप्त करना और उसकी रचना-भूमि की जानकारी करना।
प्रश्न 4. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य की विवेचना कीजिए।
उत्तर: प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका है। बौद्ध साहित्य के अन्तर्गत अनेक ग्रंथों की रचना हुई जिनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री निहित है इनमें से कुछ ग्रंथ निम्नलिखित हैं
- बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है- ये तीन हैं- सुत्तपिटक, विनयपिटक व अभिधम्म पिटक। इनमें बौद्ध धर्म के नियम व आचरण संगृहीत है।
- बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है।
- एक अन्य बौद्ध ग्रंथ मिलिन्दपन्ह में यूनानी आक्रमणकारी मिनेण्डर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता को विवरण है।
- पाली भाषा में रचित अन्य ग्रंथों दीपवंश व महावंश में सिहंलद्वीप के इतिहास का वर्णन है।
- महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन – चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, जबकि ललितविस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है और उनके अद्भुत कार्यों से सम्बन्धित जीवन वृत्त अंकित किया है।
इनके अतिरिक्त मंजुश्री मूलकल्प, अश्वघोष का बुद्धचरित्र, सौदरानन्द काव्य तथा दिव्यावदान से भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है।
प्रश्न 5. अभिलेख क्या है? इतिहास के अध्ययन में अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं?
उत्तरं: अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों का वर्णन होता है जो इसका निर्माण करवाते हैं। अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं। इतिहास के अध्ययन में इनका बहुत योगदान होता है। सम्राट अशोक के अभिलेखों से हमें सम्राट के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त होता है।
प्रयाग प्रशस्ति स्तम्भ अभिलेख से समुद्रगुप्त के काल की घटनाओं का ज्ञान होता है। जूनागढ़ शिलालेख से राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। अधिकतर अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। कई अभिलेखों पर इनके निर्माण की तिथि भी अंकित है। सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक लगभग एक लाख अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं।
प्रश्न 6. इतिहास के अध्ययन हेतु सिक्के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। टिप्पणी कीजिए।
उत्तर: प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए सिक्के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देश के विभिन्न भागों से प्राचीन काल के सिक्के बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चाँदी व ताँबे के हैं। मौर्यों के पश्चात् हिन्द यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारम्भ की। कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किये तथा गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा प्रचलन में थी। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती थी। सिक्कों से प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती हैं
- सिक्कों से शासकों के सम्बन्ध में क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। तिथिक्रम निर्धारण के लिए सिक्के उपयुक्त प्रमाण हैं।
- सिक्कों के ऊपर खुदे हुए धर्म चिन्ह राजाओं के धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
- सिक्कों से तत्कालीन समय की मुहर निर्माण कला के बारे में पता चलता है।
- सिक्के सम्बन्धित शासक के शासनकाल में व्यापार एवं आर्थिक दशा को इंगित करते हैं।
- सिक्कों से शासकों की अभिरुचियों का भी पता चलता है। इनके अतिरिक्त सिक्के साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान भी कराते हैं तथा नवीन तथ्यों के उद्घाटन में भी सहायक होते हैं।
प्रश्न 7. किन पश्चिमी इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में अपने उद्गार प्रकट किये हैं?
उत्तर: भारतीय संस्कृति का अतीत अत्यधिक वैभवशाली रहा है। इस संस्कृति ने सम्पूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। पश्चिमी इतिहासकारों एवं विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति के विश्व स्वरूप तथा इसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया है
- इतिहासकार म्यूर ने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौन्दर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है।
- सरवाल्टर रैले ने लिखा है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खण्ड में हुआ।
- कर्नल अल्काट ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही माना है।
- फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर ने ऋग्वेद की प्रति की भेंट प्राप्त कर कहा था कि यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे।
- मैक्समूलर ने मानवीय अन्त:करण एवं बुद्धि की परिपूर्णता, गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण तथा अध्ययन योग्य विषय सुलझाने का श्रेय भारतीय संस्कृति को दिया है।
इस प्रकार भारत की वैभवशाली संस्कृति का गुणगान केवल भारतीय ग्रंथों में ही नहीं वरन् पाश्चात्य विवरणों में भी मिलता है।
प्रश्न 8. भारतीयों ने किन स्थानों पर अपना राजनीतिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया?
उत्तर:
प्राचीन काल में भारत का विस्तार भूमि और समुद्र दोनों पर था। उसकी सीमा सुमात्रा, जावा द्वीप तक फैली थी। इसका विस्तार अफगानिस्तान से लेकर सम्पूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में था। शक्तिशाली जलयानों में बैठकर भारतीय ब्रह्म देश, श्याम, इण्डोनेशिया, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, बोर्निओ, फिलीपीन्स, जापान व कोरिया तक पहुँचे तथा वहाँ अपना राजनैतिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया।
पश्चिम भारत के बन्दरगाहों से द्रविड़ पर्यटक तथा नाविक सोमालीलैण्ड से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक के समस्त पूर्वी समुद्र तट पर जगह-जगह अपने वासस्थल स्थापित करने में सफल हुए।
भारतीय शूरवीरों की एक शाखा हिमालय पर्वत के उत्तर में पूर्व की ओर बढ़ी तथा इन्होंने दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों तिब्बत, मंगोलिया, सिंक्यांन, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया आदि स्थानों तक पहुँचकर भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्थापित किया। भारतवासियों की एक शाखा ने पश्चिमी द्वार से प्रस्थान किया और गांधार, पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की तथा दक्षिणी रूस के विभिन्न राज्यों एवं फिलीस्तीन पहुँचकर अपनी संस्कृति का ध्वज फहराया।
प्रश्न 9. प्राचीन भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार किन बन्दरगाहों से होता था?
उत्तर:
प्राचीन भारत के व्यापारिक सम्बन्ध मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों के साथ थे। व्यापार के लिए अधिकांशतः जलमार्गों का प्रयोग किया जाता था। पाँच-छः हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बन्दरगाह थे। उत्खनन में प्राप्त सौराष्ट्र को लोथल बन्दरगाह व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक प्रसिद्ध था।
इस बन्दरगाह पर 756 फीट लम्बे व 126 फीट चौड़े, 60 से 75 टन माल वाहक जहाज प्रयोग किये जाते थे। पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगुकच्छ भी प्रसिद्ध बन्दगाह थे। प्रथम शताब्दी में पेरीप्लस में चोल, दंभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोटायम्, कोणार्क, मच्छलीपट्टनम एवं कावेरीपट्टनम के बन्दरगाहों का उल्लेख है जिनका प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था।
प्रश्न 10. सिन्धु सरस्वती सभ्यता की जानकारी हमें किन साधनों से मिलती है?
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता की जानकारी हमें भौतिक साक्ष्यों से मिलती है जो निम्नलिखित हैं-
- नगरों तथा भवनों के अवशेष
- मृद्भाण्ड, आभूषण, औजार पकी हुई ईंटें एवं घरेलू सामान
- पत्थर के फलक, मुहरें एवं बाट
- जानवरों की अस्थियाँ।
प्रश्न 11. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के विस्तार तथा महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में संक्षेप में समझाइये।
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता का सर्वाधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। इस सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में लगभग 917 स्थान भारत में, 481 पाकिस्तान व 2 स्थान अफगानिस्तान में हैं। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किमी. व उत्तर से दक्षिण तक 1400 किमी. था।
इसका विस्तार अफगानिस्तान (शोर्तगोई व मुण्डीगाक), बलूचिस्तान (सुत्कारेण्डोर, सुत्काखोह, बालाकोट), सिन्ध (मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, जुदीरजोदड़ा), पंजाब (पाकिस्तान-हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर), पंजाब (रोपड़, सघोल), हरियाणा (बनावाली, मीताथल, राखीगढ़ी), राजस्थान (कालीबंगा, पीलीबंगा), उत्तर प्रदेश (आलमगीरपुर, हुलास) गुजरात (रंगपुर, धौलावीरा, प्रभास पट्टन, खम्भात की खाड़ी) वे महाराष्ट्र (दैमाबाद) तक था।
प्रश्न 12. वर्तमान में लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल तथा विस्तार के बारे में बताइये।
उत्तर: सरस्वती नदी का उद्भव हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में माना पर्वत से था। यह आदि बद्री से समतल में उतरती थी। इसके बाद थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, झाँसी, अग्राहेहा; अनुमानगढ़, कालीबंगा से होती हुई अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तक बहती थी। यह अनेक भागों से होते हुए समुद्र में जाकर मिलती थी।
एक शाखा प्रभास पट्ट्टन में जाकर सिन्धु सागर में मिलती थी। दूसरी शाखा सिन्धु में प्रविष्ट होकर कच्छ के रण में समा जाती थी। इसकी लम्बाई 1600 किमी और चौड़ाई 32 से 12 किमी. तक थी। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण व मूल जल स्रोतों से पानी न मिलने से धीरे-धीरे यह नदी लुप्त हो गई।
प्रश्न 13. मोहनजोदड़ों तथा हड़प्पा के नगर नियोजन की वर्तमान सन्दर्भ में उपयोगिता बताइये।
उत्तर: मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में हमें जो नगर नियोजन दृष्टिगत होता है उसकी वर्तमान सन्दर्भ में भी उपादेयता है। क्योंकि वर्तमान समय के नगरों में भी उसी प्रकार की संरचना का विकास किया जाता है जो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में दिधमान थी। इन दोनों नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, दुर्ग क्षेत्र, जहाँ शासक तथा उच्च अधिकारी रहते थे और निचला शहर जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे।
आधुनिक नगर नियोजन भी कुछ इसी तरह का होता है, एक तरफ उच्च लोगों के निवास होते हैं तथा दूसरी तरफ मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों के निवास होते हैं। दोनों नगरों में सड़कों की व्यवस्था रखी जाती थी जो आज के नगरों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोनों नगरों में सड़कों का निर्माण भी वर्तमान नगरों की भाँति ही किया गया था। प्रत्येक घर में कुआँ होता था तथा जल निकास की व्यवस्था भी उत्तम थीं।
नालियाँ गन्दे पानी को नगर से बाहर पहुँचाती थीं। बड़ी नालियाँ ढकी हुई थीं। सड़कों की नालियों में मेन होल (तरमोखे) भी मिले हैं। सड़कों की नालियों के बीच – बीच में चेम्बर (शोषगर्त) भी थे जिनकी सफाई करके कूड़ा-करकट निकाल दिया जाता था। यह व्यवस्था आधुनिक समय में भी प्रचलन में है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में भी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के नगर नियोजन की प्रासंगिकता है।
प्रश्न 14. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारें में संक्षेप में समझाइए।
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोगों को आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन एवं अनेक व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित था। इन्हीं गतिविधियों से उनको जीवन-यापन होता था। इस सभ्यता की प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ निम्नलिखित र्थी-
1. कृषि:
मूलतः यह सभ्यता कृषि पर आधारित थी। गेहूँ, जौ, धान, बाजरा, कपास, दाल, चना, तिल आदि की खेती इस सभ्यता के लोगों द्वारा की जाती थी। हल तथा बैलों का प्रयोग जुताई हेतु किया जाता था। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी।
2. पशुपालन:
पशुपालन कृषि आधारित दूसरा प्रमुख उप व्यवसाय था।
3. व्यापार:
सिन्धु घाटी सभ्यता के निवासी ने केवल अपने देश वरन् विदेशों से भी व्यापार करते थे। सोने, चाँदी, ताँबे और कीमती पत्थरों, मूर्तियों तथा बर्तनों से पता चलता है कि इनका विदेशों से आयात किया जाता था। अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ इनके व्यापारिक सम्बन्ध थे। विदेशी व्यापार के लिए लोथल बन्दरगाह का प्रयोग किया जाता था।
4. उद्योग:
सिन्धु सरस्वती सभ्यता से उत्खनन में प्राप्त ताँबे व कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ यहाँ धातु उद्योग के विकसित होने का प्रमाण देती हैं। इसके अतिरिक्त, मेनके बनाने का उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि भी उन्नत अवस्था में थे।
प्रश्न 15. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के नाप-तौल के साधन (बाट प्रणाली) की क्या विशेषताएँ थी? वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
उत्तर: सिन्धु सभ्यता के लोग विनिमय (लेन – देन) हेतु नाप -तौल के लिए बाटों का प्रयोग करते थे। बाट सामान्यतया चर्ट, जैसार वे अगेट के बने होते थे। बाट प्रायः घनाकार व गोलाकार होते थे और इन पर निशान नहीं होते थे। इन बाटों के निचले मानदण्ड द्विआधारी (1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12800 तक) थे, जबकि ऊपरी मानदण्ड दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। छोटे बाटों का प्रयोग सम्भवतः आभूषणों और मनकों को तौलने हेतु किया जाता था।
सिन्धु सभ्यता में बाट जिसे अनुपात में प्रयुक्त होते थे उसी अनुपात में वर्तमान में भी होते हैं। सिन्धु सभ्यता के सभी नगरों में माप, तौल, प्रणाली एक समान थी। वर्तमान में भी माप तौल प्रणाली पूरे देश में एक समान है। निश्चित ही माप तौल प्रणाली की प्रेरणा हमें सिन्धु सभ्यता से मिली होगी। सिन्धु सभ्यता की माप तौल प्रणाली आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जितनी उस समय थी।
प्रश्न 16. सिन्धु सभ्यता की धातु कला के विषय में संक्षेप में आलेख लिखिए।
उत्तर: सिन्धु सभ्यता आर्थिक दृष्टि से उन्नत अवस्था में थी, इस बात का प्रमाण यहाँ की विकसित धातु कला से मिलता है। हमें सोना, चाँदी, ताँबा, काँसे तथा टिन इत्यादि सामग्री अवशेष पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में एक कूबड़दार बैल का खिलौना तथा कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
इन सबके साथ ही ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के काँटे, आरियाँ, तलवारें, दर्पण, छेणी, चाकू, भाला, बर्तन आदि भी मिले हैं। चन्हुदड़ों धातु गलाने का मुख्य स्थान था। यहाँ मनके बनाने के लिए विभिन्न धातुओं को गलाया जाता था। ये सभी तथ्य स्पष्ट करते हैं कि सिन्धु सरस्वती सभ्यता की धातु कला अत्यन्त विकसित अवस्था में थी।
प्रश्न 17. सिन्धु सरस्वती सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं?
उत्तर: पुरातत्वविदों की उत्खनन में पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई है जिसके आधार पर इतिहासकार सुगमता से इतिहास का निर्धारण कर सकते हैं। सिन्धु सभ्यता से हमें पर्याप्त मात्रा में मातृदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकल रहा है जिससे पता चलता है सम्भवतः यह पृथ्वी माता का रूप है। इस सभ्यता की धार्मिक परम्पराओं में मातृदेवी की उपासना, पशुपतिनाथ की पूजा, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता, तप, योग तथा पशु-पक्षियों की पूजा का प्रचलन था।
प्रश्न 18. आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म आज भी भारतीय धार्मिक जीवन में परिलक्षित होता है?
उत्तर: हुम इस कथन से पूरी तरह से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म आज भी भारतीय धार्मिक जीवन में परिलक्षित होता है। ऐसा इसलिए है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग मातृदेवी, आद्य शिव,वृक्षों, पशुओं आदि की पूजा करते थे जिनके स्पष्ट प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। आज भी हिन्दू धर्म में लोग आद्य शिव, वृक्षों (जैसे- पीपल, तुलसी) तथा कुछ पशुओं (जैसे गाय) को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। कई जगहों पर लोग नागों की भी पूजा करते हैं, जिसका साक्ष्य भी सिन्धु घाटी के नगरों में प्राप्त होता है।
प्रश्न 19. भारतीय सभ्यता पर सिन्धु सरस्वती सभ्यता का क्या प्रभाव है?
उत्तर: भारतीय सभ्यता पर सिन्धु घाटी की सभ्यता का व्यापक प्रभाव है। सिन्धु घाटी सभ्यता के कुछ प्रभाव हमारे आज के जीवन में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं-
- धार्मिक समानता – सिन्धु सभ्यता के पूज्नीव पशुपति शिव, मातृदेवी की पूजा, बैल तथा अन्य पशुओं की उपासना, जल की पवित्रता, धार्मिक अवसरों पर स्नान, ये सभी परम्पराएँ आज भी भारतीय जीवन में परिलक्षित होती हैं।
- आभूषण एवं श्रृंगार – सिन्धु सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। प्राप्त अवशेषों में जो आभूषण मिले हैं उनमें गले के आभूषण, पैरों की पायल, करधनी आदि प्रमुख हैं जो आज भी स्त्रियाँ अपनी सज्जा के लिए प्रयोग करती हैं।
- नगर नियोजन – आधुनिक नगरों के अनुसार सिन्धु घाटी के नगर भी योजना के अनुसार बनाए जाते थे। चौड़ी सड़कें और गलियाँ, जल निस्तारण की व्यवस्था, सार्वजनिक मालगोदाम, स्नानागार आदि इस बात के साक्ष्य हैं।
- निवास स्थान – सिन्धु सभ्यता के भवनों में आज की भाँति प्रवेश द्वार, आँगन, स्नानगृह, सीढ़ियाँ आदि होती थीं।
प्रश्न 20. नगर नियोजन तथा धर्म को छोड़कर सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन-सा पहलू है जिससे न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी देश प्रेरणा ले सकते हैं? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: सिन्धु सभ्यता के नगर नियोजन तथा धर्म से भारत लोग प्रेरणा तो ले ही सकते हैं। एक अन्य पहलू भी है। जिससे न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी देश भी प्रेरणा ले सकते हैं। पहलू हैं शांति सिन्धु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। सिन्धु सभ्यता निवासियों ने अपने समय का अधिकांश उपयोग सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए किया। सिन्धु सभ्यता के निवासियों ने अपने समय का उपयोग युद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में न करके अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए किया।
आज विश्व में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। हिंसक तथा आतंकवादी गतिविधियों ने अनेक देशों को ऐसी स्थिति में ला दिया है जहाँ शांति की परम आवश्यकता है। इस सम्दर्भ में भारत एवं विश्व के देश सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं तथा अपने देशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं।
प्रश्न 21. वेद क्या हैं और कितने हैं? प्रत्येक का वर्णन कीजिए।
उत्तर: वेद संसार के प्राचीनतम संस्कृत भाषा में रचे गये ग्रंथ हैं। वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भण्डार हैं। वेदों के द्वारा हमें सम्पूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। हमारे ऋषियों ने लम्बे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया है। इसलिए वेदों को संहिता भी कहा गया है। वेदों की संख्या चार है-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
- ऋग्वेद – आर्यों का सबसे प्राचीनतम् ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 अध्याय और 1028 सूक्त हैं। इसमें छन्दों में रचित देवताओं की स्तुतियाँ हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता व ऋषि का उल्लेख है। कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार-विचारों का वर्णन है।
- सामवेद – सामवेद में काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। इसके 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नये हैं शेष ऋग्वेद के हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाये जाते हैं।
- यजुर्वेद – यजुर्वेद में यज्ञों, कर्मकाण्डों व अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह है। इसमें 40 अध्याय हैं एवं शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद के दो भाग हैं।
- अथर्ववेद – अन्तिम वेद अथर्ववेद में 20 मण्डल 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसकी रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गयी थी। इसको अन्तिम अध्याय ईशोपनिषद है जिसका विषय आध्यात्मिक चिन्तन है।
प्रश्न 22. वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
उत्तर: वैदिक काल में व्यवस्थित राजनैतिक जीवन की शुरूआत हो चुकी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी राजनैतिक इकाई कुल तथा सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। राष्ट्र – जन – विश – ग्राम – कुल राजनैतिक संगठन का अवरोही क्रम था। एक राष्ट्र,में कई जन थे। कुल का मुखिया कुलुप, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश का अधिकारी विशपति, जन का मुखिया गोप तथा राष्ट्र का मुखिया राजा था।
राजा को पद वंशानुगत होता था। लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप उस समय भी दिखाई देता है। राजा को राज्याभिषेक के समय प्रजा हित की शपथ लेनी होती थी। जनता राजा को कर देती थी जिसे बलिहृत कहा जाता था। राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए पुरोहित व सेनानी होते थे। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली सभा तथा समिति दो संस्थाएँ थीं।
प्रश्न 23. सभा व समिति में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर: समिति-समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा होती थी जिसमें महत्वपूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक विषयों पर विचार होता था। समिति सभा की तुलना में बड़ी संस्था थी जिसकी बैठकों में राजा भी भाग लेता था।
सभा: समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था थी जिसमें विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। ऋग्वेद में सुजात (कुलीन या श्रेष्ठ) व्यक्तियों की सभा का उल्लेख है। सभा अनुभवी, वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी जो राजा को परामर्श देने के साथ न्याय कार्य में सहयोग करती थी।
प्रश्न 24. सोलह महाजनपद तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए।
उत्तर: बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानियाँ निम्न प्रकार थीं-
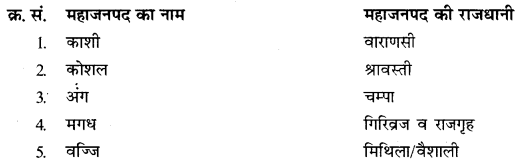
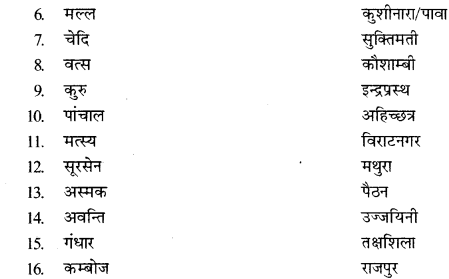
प्रश्न 25. बौद्ध साहित्य में वर्णित दस गणराज्यों के नाम लिखिए।
उत्तर: महाजनपद काल में दस राज्यों में गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये राज्य इस प्रकार थे-
- कपिलवस्तु के शाक्य
- रामग्राम के कोलिय
- पिप्पलिवन के मोरिय
- मिथिला के विदेह
- पावा के मल्ल
- कुशीनगर के मल्ल
- अलकप्प के बुलि
- वैशाली के लिच्छवि
- सुसुमारगिरि के भग्ग
- केसपुत्त के कालाम।
प्रश्न 26. ऋग्वेद के अनुसार वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत चार वर्षों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई?
उत्तर: प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था में लोग चार वर्षों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के दसवें मण्डल के अनुसार वर्ण व्यवस्था के चार वर्षों की उत्पत्ति आदिमानव परम पुरुष से हुई है। उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इन वर्गों का मुख्य आधार व्यवसाये था।
प्रश्न 27. बौद्धों ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था की किस प्रकार आलोचना की?
उत्तर: जिस समय समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में संहिताबद्ध किया जा रहा था, उस समय कुछ अन्य धार्मिक परम्पराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। लगभग छठी शताब्दी ई. पू. में आरम्भिक बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की गई।
यद्यपि बौद्धों ने इस बात को तो स्वीकार किया कि समाज में विषमताएँ मौजूद होती हैं परन्तु उनके अनुसार ये भेद प्राकृतिक नहीं थे और न ही स्थायी। उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अस्वीकार कर दिया।
प्रश्न 28. क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज भी भारतीय समाज में जाति प्रथा के कुछ तत्व विद्यमान हैं?
उत्तर: यह बात पूरी तरह सत्य है कि आज भी भारतीय समाज में जाति प्रथा के कुछ तत्व विद्यमान हैं। वर्तमान युग आधुनिकता का युग है। आधुनिकता की इस दौड़ में हम बहुत – सी चीजों को पीछे छोड़ आये हैं। परन्तु बहुत-सी चीजें ऐसी भी हैं जो आज भी भारतीय समाज में विद्यमान हैं। जाति प्रथा उनमें से एक है।
शहरों में तो जाति प्रथा के अधिक उदाहरण नहीं देखने को मिलते परन्तु आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथा के तत्व देखे जा सकते हैं। बेशक आज का समाज कितना ही विकसित क्यों न हो गया हो परन्तु हम दकियानूसी एवं रूढ़िवादी प्रथाओं से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाये हैं।
प्रश्न 29. प्राचीन समाज में प्रचलित आश्रम व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
उत्तर:व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसके जीवन की गति को चार आश्रमों में विभाजित किया गया। मनुष्य से यह अपेक्षा की गई कि वह जीवन के इन चार सोपानों – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम को पार करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेगा।
मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म से परिचित होता था, शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता था, गृहस्थाश्रम में धर्मरत होकर अर्थ और काम को प्राप्त करता था, वानप्रस्थ में वह पूरा समय समाज कार्य के लिए लगाता था तथा संन्यास में वह मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता था। आश्रम व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक लक्ष्यों को समान रूप से समन्वयीकरण था।
प्रश्न 30. पुरुषार्थ की परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए कि इनका सम्बन्ध किससे है?
उत्तर: पुरुषार्थ से तात्पर्य उन आदर्शों से है जिनका अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। भारत में मानव के अनुसरण करने योग्य मूल्यों का वर्गीकरण चार पुरुषार्थ के रूप में किया गया है
- धर्म – धर्म का सम्बन्ध सदाचार, कर्तव्य पालन तथा सद्गुण से है।
- अर्थ – अर्थ का सम्बन्ध मनुष्य की भौतिक समृद्धि व उपभोग से है।
- काम – काम का सम्बन्ध सुख के उपभोग से है।
- मोक्ष – मोक्ष का सम्बन्ध सांसारिक जीवन से मुक्त होने अर्थात् अध्यात्म से है।
भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का दर्शन सम्पूर्ण जीवन दृष्टि से है जिसमें लौकिक जीवन के विभिन्न पक्षों के साथ-साथ व्यक्ति के पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक सम्बन्ध भी सम्मिलित हैं।
प्रश्न 31. भारतीय संस्कृति में कितने ऋणों का उल्लेख किया गया है?
उत्तर: ऋण की अवधारणा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऋग्वेद में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों सन्दर्भ में मनुष्य के ऋणों की चर्चा की गयी है। भारतीय ऋषियों ने तीन ऋणों की व्यवस्था की है। ये ऋण हैं-देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण। इन ऋणों से मुक्त होने पर ही मुक्ति सम्भव है। ये ऋण मनुष्य के सामाजिक दायित्वों से सम्बन्धित हैं
- पितृ ऋण – सन्तानोत्पत्ति के द्वारा मानव जाति की निरन्तरता बनाकर हम पितृ ऋण की पूर्ति कर सकते हैं।
- ऋषि ऋण – जो ज्ञान हमें ऋषियों से मिलता है और जिस ज्ञान की परम्परा के हम उत्तराधिकारी हैं, उस ज्ञान और परम्परा का संवर्द्धन करके ऋषि ऋण की पूर्ति कर सकते हैं।
- देव ऋण – देवताओं से सम्बद्ध दायित्व जिसे यज्ञादि से पूरा किया जाता है। यह ऋण मनुष्य को सृष्टि से जोड़ता है।
अतः मनुष्य को समस्त प्राणियों कीट-पतंगों, पशु-पक्षियों को भोजन व सूर्य चन्द्र की स्तुति कर सृष्टि की निरन्तरता में योगदान करना चाहिए।
प्रश्न 32. भारतीय संस्कृति में आवश्यक पंच महायज्ञ कौन-कौन से हैं?
उत्तर: भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञों का प्रावधान है-
- ब्रह्म या ऋषि यज्ञ – स्वाध्याय व ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना।
- देव यज्ञ – देवताओं की यज्ञ करके स्तुति करना, पूजा करना, प्रार्थना करना एवं वन्दना करना।
- पितृ यज्ञ – माता-पिता की सेवा करना तथा गुरु, आचार्य एवं वृद्धजन का सम्मान व सेवा करना।
- भूत यज्ञ – विभिन्न प्राणियों पशु पक्षियों, गाय, कौआ, चींटी, कुत्ता को भोजन कराकर संतुष्ट करना एवं अतिथियों की सेवा करना।
- नृप यज्ञ – सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना।
प्रश्न 33. उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: उपनिषदों के दार्शनिक विचारों द्वारा आत्मा, परमात्मा, कर्म, जीवन के अर्थ, जीवन की सम्भावना पुनर्जन्म तथा मोक्ष आदि की विवेचना हुई है। इस विचार के अनुसार आत्मा, अगाध, अपार, अवर्णनीय एवं सर्वव्यापक है। सभी तत्व इस आत्मा में ही समाहित हैं। यह आत्मा ही ब्रह्म है तथा यही सर्वव्यापक है। अतः मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा में विलीन कर स्वयं परमब्रह्म को जानना है।
निबन्धात्मक प्रश्न[/su_heading]
प्रश्न 1. प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में साहित्यिक स्रोतों की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर: इतिहासकार समाज में हुए परिवर्तनों को समझने और इतिहास की पुनः रचना करने के लिए साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करते हैं। इन स्रोतों के आधार पर वे विश्वसनीय विवरण तैयार करते हैं। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो प्रमाणों से सिद्ध हों। साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को अग्रांकित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।
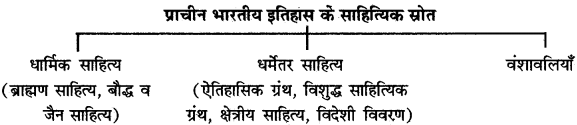
धार्मिक साहित्य: प्राचीन भारतीय धर्मों से सम्बन्धित जो साहित्य रचा गया उसे धार्मिक साहित्य कहा जाता है। इनमें प्रमुख ब्राह्मण साहित्य बौद्ध व जैन साहित्य है।
(क) ब्राह्मण साहित्य – इनमें सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। इनकी संख्या चार है-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के चार भाग हैं-संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। इसके छ: भाग हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष। वेदों के चार उपवेद हैं-आयर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद व शिल्प, वेद इनसे चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त होती है।
(ख) बौद्ध साहित्य – बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रन्थ त्रिपिटिक है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम व आचरण संगृहीत हैं। अन्य बौद्ध ग्रंथों जैसे-मिलिन्दपन्हों, दीपवंश, महावंश, महावस्तु ग्रंथ, ललित विस्तार, मंजुश्री, मूलकल्प, अश्वघोष का बुद्धचरित्र, सौंदर्यानन्द काव्य, दिव्यावदान एवं जातक ग्रंथों से बौद्ध धर्म व गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है।
(ग) जैन साहित्य – जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में रचित हैं अन्य जैन ग्रंथों में। कथाकोष, परिशिष्टपर्वन, भद्रबाहुचरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांगसूत्र आदि प्रमुख हैं जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है।
मैतर साहित्य: इस साहित्य के अन्तर्गत धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखे गये ग्रंथ आते हैं, जैसे
(i) ऐतिहासिक ग्रंथ:
प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों में 1150 ई० में लिखी गई कल्हण की राजतरंगिणी एवं कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख है। ये ग्रंथ तत्कालीन शासकों एवं उनकी शासन पद्धतियों का उचित ब्यौरा देते हैं। अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं-बाणभट्ट का हर्षचरित, वाक्पति का गौढवहो, विल्हण का विक्रमांकदेव चरित, जयसिंह का कुमारपाल चरित, जयचन्द का हम्मीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित्र, बल्लाल का भोज चरित एवं जयानक की पृथ्वीराज विजय आदि।
(ii) विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ:
इनके तहत अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा-साहित्य एवं कोष की , रचना की गई जो उस समय के शासकों, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को जानने का प्रमुख स्रोत हैं। इनमें प्रमुख हैं-पाणिनी .. का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाकाव्य, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, विशाखदत्त का मुद्राराक्षस, शूद्रक को मृच्छकटिकम्, मेघातिथि की मिताक्षरा के कामन्दक का नीतिसार। कथा साहित्य कोष की दृष्टि से विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, क्षेमेन्द्र की वृहतकथामंजरी, गुणाढ्य की कथा-मंजरी, सोमदेव की कथासरित्सागर, अमरसिंह का अमरकोष प्रमुख हैं।
(iii) क्षेत्रीय साहित्य:
क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथों में धूर्जटि द्वारा रचित तेलगू ग्रंथ कृष्णदेवराय विजयुम, विजय नगर के शासक कृष्णदेवराय के सम्बन्ध में जानकारी देता है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चन्दबरदाई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कान्हड़दे प्रबन्ध, बीठू सूजा का राव जैतसी रो छन्द, सूर्यमल मिसण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसी की ख्यात बांकीदास की ख्यात आदि प्रमुख हैं।
(iv) विदेशी विवरण:
विदेशी लेखक भी भारत की सांस्कृतिक व आर्थिक उपलब्धियों से प्रभावित हुए तथा उन्होंने अपने लेखों में भारत के सम्बन्ध में पर्याप्त विवरण दिया है। यूनानी साहित्य में मेगस्थनीज की इंडिका, टॉलमी का भूगोल, प्लिनी दि एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोब्यूलस की हिस्ट्री ऑफ दी वार’, स्ट्रेबो का भूगोल आदि रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। चीनी विवरणों में फाह्यान, ह्वेनसांग, सुंगयुन तथा इत्सिग चीनी यात्रियों के विवरणों से तत्कालीन शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिलती है।
तिब्बती वृत्तान्त में तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना गया है। अरबी यात्रियों के विवरण में मसूदी की पुस्तक ‘मिडास ऑफ गोल्ड’ सुलेमान नवी की पुस्तक सिलसिलात-उल-तवारीख तथा अलबरुनी की पुस्तक तारीख-ए-हिन्द में भारतीय समाज व संस्कृति सम्बन्धी जानकारी मिलती है।
वंशावलियाँ:
वंशावली लेखन परम्परा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। वंशावलियाँ एक न्यायिक दस्तावेज हैं, जो व्यक्ति की परम्परा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुलधर्म, कुलाचार, गोत्र व पूर्वजों के नाम आदि प्राप्त करने का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत हैं। वंशावली लेखन परम्परा की शुरूआत वैदिक ऋषियों द्वारा समाज को सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से की गई थी जो हजारों वर्षों से आज भी अनवरत जारी है।
प्रश्न 2. इतिहास के विश्वसनीय स्रोत के रूप में यूनानी साहित्य, चीनी विवरण व तिब्बती वृत्तान्त का वर्णन कीजिए।
उत्तर: इतिहास के विश्वसनीय स्रोत के रूप में यूनानी साहित्य, चीनी विवरण व तिब्बती वृत्तान्त का क्रमशः वर्णन निम्नलिखित है
1. यूनानी साहित्य:
यूनानी लेखकों में टेसियस, हेरोडोटस, निर्याकस, एरिस्टोब्युलस, आनेक्रिट्स, स्ट्रेबो, एरियन एवं स्काई लेक्स प्रमुख हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखित ‘इंडिका’ है। यूनानी विवरणों से चन्द्र गुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज एवं आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यूनानी साहित्य में टॉलमी का भूगोल, प्लिनी दी एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोब्यूलस की हिस्ट्री ऑफ दी वार’ स्ट्रेबो का भूगोल आदि विशेष उल्लेखनीय है। ‘पेरीप्लस ऑफ दी एरिथ्रीयन सी’ पुस्तक में बन्दरगाहों व व्यापार का विस्तृत विवरण है।
2. चीनी विवरण:
चीनी यात्रियों में फाह्यान, सुंगयुन, ह्वेनसांग एवं इत्सिग का वृत्तान्त महत्वपूर्ण है। फाह्यान गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त II के समय (399 – 414 ई.) भारत आया था। ह्वेनसांग को ‘यात्रियों का राजकुमार’ कहा जाता है। उसने नालन्दा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। वह हर्षवर्धन के राज्य काल में 629 ई. से 644 ई. में भारत आया था और उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। इत्सिग ने सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 672 से 688 ई. तक भारत भ्रमण किया। इससे नालन्दा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ ही भारतीय संस्कृति व समाज की भी जानकारी मिलती है।
3. तिब्बती वृत्तान्त:
तिब्बती वृत्तान्त में तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर वे तंग्यूर ग्रन्थों को उपयोगी माना गया है। अरबी यात्री और भूगोलवेत्ताओं ने भी भारत के सम्बन्ध में जानकारी दी है। मसूदी ने अपनी पुस्तक ‘मिडास ऑफ गोल्ड’ में भारत का विवरण,दिया है और लिखा है कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। सिन्ध के इतिहास ‘चचनामा’ में तथा सुलेमान नवी की पुस्तक ‘सिलसिलात-उल-तवारीख’ में पाल – प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है।
अरबी लेखकों में अल्बेरूनी (तारिख ए हिन्द) सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने संस्कृत भाषा सीखी व मूल स्रोतों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक तारीख-उल-हिन्द में भारतीय समाज व संस्कृति के बारे में लिखा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इतिहास के विश्वसनीय स्रोत के रूप में यूनानी साहित्य चीनी विवरण, तिब्बती वृत्तान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
प्रश्न 3. पाषाण काल किसे कहते हैं तथा इसे कितने भागों में बाँटा गया है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर: मानव के उद्भव एवं उसके विकास के प्रत्येक काल को उस समय प्रचलित औजारों तथा उपकरणों के आधार पर विभाजित किया गया है क्योंकि ये ही उस काल के इतिहास को जानने के प्रमुख साधन हैं। पाषाण काल में मानव ने पत्थर के टुकड़े को तोड़-फोड़कर तथा काँट-छाँटकर उनसे उपकरण बनाये। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण ही प्रथम काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को सामान्यतः अग्र तीन प्रमुख उपविभागों में विभाजित किया गया है।
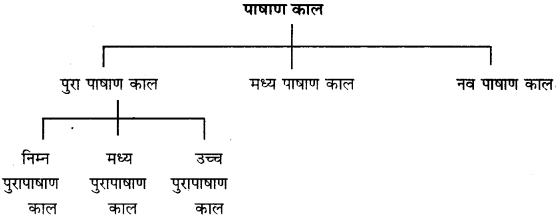
1. पुरा पाषाण काल:
पुरा पाषाण काल के उपकरण 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने प्रथम बार बनाये थे जो आकार में बड़े व मोटे हैं, पर सुगढ़ नहीं हैं। भारतीय पुरापाषाण युग के मानव द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पत्थर के औजारों को स्वरूप तथा जलवायु परिवर्तन के आधार पर तीन अवस्थाओं में बाँटा जाता है। पहली अवस्था को निम्न पुरा पाषाण युग, दूसरी को मध्य पुरा पाषाण युग और तीसरी को उच्च पुरा पाषाण युग कहते हैं।
2. मध्य पाषाण काल:
प्रस्तर युगीन संस्कृति में एक मध्यवर्ती अवस्था आयी जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। इस युग में पत्थरों का आकार छोटा होता गया। लघु आकार के कारण इन्हें सूक्ष्म पाषाण,उपकरण कहते हैं। इस समय का मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने लगा और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ तथा नदी के तटों व झीलों के किनारे लकड़ी व घासफूस से बनी गोल झोंपड़ियों में रहने लगा। इस युग में मिट्टी के पात्रों का भी उपयोग होने लगा तथा खाद्य सामग्री को भी पकाया जाने लगा।
3. नव पाषाण काल:
नव पाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाना शुरू किया जो कृषि कार्य व पशुपालन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, वसूला, छिद्रित वृत्त, हथौड़ा, सिललोढ़, ओखली आदि सम्मिलित थे। ये उपकरण बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर के थे जिन्हें घिसकर चिकना किया जाता था। कृषि कार्य ने धीरे – धीरे मानव को एक जगह बसने को विवश कर दिया। इसी के साथ आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के नये युग का आरंभ हुआ।
प्रश्न 4. सिन्धु सभ्यता की खोज में पुरातत्वविदों का योगदान एवं सिंधु सभ्यता के विस्तार – क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
उत्तर: भारत की सिन्धु नदी की घाटी में विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता फल – फूल रही थी। इस सभ्यता के नष्ट हो जाने के हजारों वर्षों के बाद जब लोगों ने इस क्षेत्र में रहना शुरू किया तो उन्हें अनेक पुरावस्तुएँ प्राप्त हुईं। यही पुरावस्तुएँ हड़प्पा सभ्यता की खोज को आधार बनीं। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में पुरातत्वविद् दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। 1922 ई. में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया।
हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों की समानता के आधार पर पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि यह दोनों पुरास्थल एक ही संस्कृति के भाग थे। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यतो कहा गया। इस सभ्यता के प्रारम्भिक स्थल सिन्धु नदी के आस-पास थे अतः इसे प्रारम्भ में सिन्धु घाटी सभ्यता कहा गया था परन्तु इस सभ्यता का सर्वाधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है।
अतः इसे सिन्धु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया जाना सर्वथा उचित है। पुरातत्वविदों की निरन्तर खोजों के परिणामस्वरूप केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही इसे सभ्यता से सम्बन्धित लगभग 1400 पुरास्थल प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से लगभग 917 स्थल भारत में तथा 481 स्थल पाकिस्तान में व 2 अफगानिस्तान में हैं। इस सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल निम्नलिखित जगहों से प्राप्त हुए हैं-
- राजस्थान – कालीबंगा
- हरियाणा – बनावली राखीगढ़ी व मीताथल
- गुजरात – रंगपुर, धौलावीरा, प्रभास पाटन, खम्भात की खाड़ी
- महाराष्ट्र – दैमाबाद।
प्रश्न 5. सिन्धु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। यह सभ्यता एवं संस्कृति विशुद्ध भारतीय है। इस सभ्यता का उद्देश्य, रूप और प्रयोजन मौलिक एवं स्वदेशी है। उत्खनन द्वारा जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर सिन्धु सरस्वती सभ्यता का जो जीवन्त रूप व विशेषताएँ उभरकर सामने आयी हैं वे निम्न प्रकार हैं
1. नगर योजना:
सिन्धु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ के निवासी अपने निवास एक निश्चित योजना के अनुसार बनाते थे। शासक वर्ग के लोग दुर्ग में रहते थे तथा साधारण वर्ग के लोग निश्चित निचली जगह पर रहते थे। मकान निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक मकान में एक आँगन, रसोईघर, स्नानघर, द्वार आदि होते थे। नगरों में चौड़ी-चौड़ी सड़कें वे गलियाँ बनायी जाती र्थी जो एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगरों में गन्दे पानी के निकास की उचित व्यवस्था थी। इस सभ्यता में कई विशिष्ट भवन मिले हैं जो इस सभ्यता के उत्कृष्ट नगर नियोजन को दर्शाते हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो का मालगोदाम, विशाल स्नानागार तथा हड़प्पा का विशाल अन्नागार प्रमुख हैं।
2. सामाजिक जीवन:
सिन्धु सभ्यता के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। मातृदेवी की मिट्टी की प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व व परिवार के मातृसत्तात्मक होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र बना है जो सिंधु-सरस्वती सभ्यतावासियों की वाद्य कला में रुचि को दर्शाता है।
3. धार्मिक जीवन:
सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोग धार्मिक विचारों के थे। ये मातृदेवी की पूजा करते थे तथा शिव की भी उपासना करते थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों में वृक्षों तथा पशुपक्षियों की पूजा भी प्रचलित थी। इनके धार्मिक जीवन में पवित्र स्नान तथा जल पूजा का भी विशेष महत्व था।
4. आर्थिक जीवन:
सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि थी। ये लोग गेहूँ, जौ, चावल, चना, बाजरा, दाल एवं तिल आदि की खेती करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया के अनेक देशों के साथ व्यापार होता था। विदेशों से व्यापार के लिए जलमार्गों का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के लोग उद्योग-धन्धों में भी संलग्न थे। मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, औजार बनाना आदि उद्योग विकसित अवस्था में थे। तोल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था।
5. राजनीतिक जीवन:
सिन्धु सरस्वती सभ्यता के राजनैतिक जीवन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के चार बड़े केन्द्र रहे होंगे-हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। सुव्यवस्थित नगर नियोजन स्वच्छता, जल संरक्षण आदि प्रतीकों से पूर्ण एवं कुशल राजसत्ता नियंत्रण तथा व्यवस्थित नगर पालिका प्रशासन के संकेत मिलते हैं। अस्त्र – शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना यहाँ के निवासियों के शान्तिप्रिय होने की सूचना देते हैं।
6. लिपि:
सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोगों ने लिपि का भी आविष्कार किया। इस सभ्यता की लिपि भाषा चित्रात्मक थी। इस लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था।
7. कला:
सिन्धु सरस्वती सभ्यता के लोगों ने कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी। उत्खनन से प्राप्त मुहरों एवं बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी देखने को मिलती है। मिट्टी से बने मृदभाण्ड, मृणमूर्तियाँ, मुहर निर्माण, आभूषण बनाना आदि इनकी उत्कृष्ट कला प्रेम के उदाहरण हैं।
प्रश्न 6. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं? वर्णन कीजिए।
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता इसका नगर नियोजन था। पुरातत्वविद् इस काल की नगर नियोजन की व्यवस्था को देखकर हतप्रभ हैं जो आज के वास्तुविदों की नियोजन शैली से किसी भी प्रकार कमतर नहीं है। उत्खनन में प्राप्त हुए इन नगरों के निर्माण की आधार योजना, निर्माण शैली तथा आवास व्यवस्था में विलक्षण एकरूपता प्राप्त होती है। इस नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार थीं-
1. व्यवस्थित सड़कें तथा गलियाँ:
सिन्धु सभ्यता के नगरों की सड़कें, सम्पर्क मार्ग और गलियाँ एक सुनिश्चित योजना के अनुसार निर्मित र्थी। नगर में एक-दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थीं जिसकी चौड़ाई 9 से 34 फीट थी। गलियाँ एक से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थीं। कालीबंगा की सड़कें 1.8, 3.6, 5.4 व 7.2 मी. चौड़ी होती थीं।
2. नियोजित जल निस्तारण व्यवस्था:
सिन्धु घाटी सभ्यता में जल निस्तारण की व्यवस्था अति उत्तम थी। घरों के पानी का निकास नालियों से होता था। नालियाँ गन्दे पानी को नगर से बाहर पहुँचाती थीं। बड़ी नालियाँ ढंकी हुई थीं। नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग होता था। सड़कों की नालियों में मेन होल (तरमोखें) भी मिले हैं। नालियों के बीच-बीच में चेम्बर (शोषगर्त) भी थे, जिनकी सफाई करके कूड़ा-करकट निकाल दिया जाता था।
3. व्यवस्थित आवासीय भवन:
आधुनिक गृह स्थापत्य कला के अनुसार सिन्धु सरस्वती सभ्यता के वास्तुशिल्पी आवासीय नियोजन में सुव्यवस्थित गृह स्थापत्य कला का पूरा ध्यान रखते थे। आवास एक निश्चित योजना के अनुसार ही बनाये जाते थे। प्रत्येक मकान में एक स्नानागार, आँगन और आगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे। शौचालय व दरवाजों, खिड़कियों आदि की भी समुचित व्यवस्था थी। मकानों के निर्माण में प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग होता था।
4. विशाल स्नानागार:
मोहनजोदड़ो का यह महत्वपूर्ण भवन है जिसका आकार 39 × 23 × 8 फीट है। इसमें ईंटों की सीढ़ियाँ हैं। तीन तरफ बरामदे हैं। फर्श व दीवारों पर ईंटों का प्रयोग है। पास में एक कुएँ के भी अवशेष मिले हैं जो जल का स्रोत था। उत्तर की ओर छोटे – छोटे आठ स्नानागार भी बने हुए हैं।
5. विशाल अन्नागार:
हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 × 15.23 मीटर का है। दो खंण्डों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल 55 × 43 मीटर है जो पानी के बचाव हेतु ऊँचे चबूतरे पर बना हुआ है। प्रत्येक खण्ड में 6 – 6 की दो पंक्तियों में भण्डारण कक्ष हैं, दोनों के मध्य 23 फुट की दूरी है।
6. विशाल जलाशय व स्टेडियम:
धौलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे – बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर बनाया गया 95 × 11.42 × 4 मीटर का जलाशय प्रमुख उदाहरण है। इसके अतिरिक्त धौलावीरा से ही 283 × 45 मीटर के आकार के स्टेडियम के भी प्रमाण मिले हैं।
इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं। समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ है और इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। उक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि उस काल में सिन्धु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन कला उच्चकोटि की थी। लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त थीं।
प्रश्न 7. सिन्धु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख नगरों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: सिन्धु सरस्वती सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किमी. व उत्तर से दक्षिण तक 1400 किमी. था। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर निम्न प्रकार थे-
- मोहनजोदड़ो – मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन योजनाबद्ध नगर है। यह पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त के लरकाना जिले में सिन्धु नदी के किनारे स्थित है। सन् 1922 ई० में भारतीय पुरातत्वविद् श्री राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की। इस नगर से एक विशाल स्नानागार मिला है जो सिन्धु सभ्यता के नगर नियोजन का महत्वपूर्ण भाग है।
- हड़प्पा – हड़प्पा पाकिस्तान के साहीवाल जिले में स्थित है। पुरातत्वविद् श्री दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज 1921 ई० में की थी। हड़प्पा के नगरों की सड़कें चौड़ी होती थीं। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। नगर नियोजन को पूरा ध्यान रखा जाता था। इस नगर के नाम पर सिन्धु सरस्वती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति भी कहा जाता है।
- लोथल – लोथल भी सिन्धु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केन्द्र है। पुरातत्वविदों के अनुसार लोथल भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बन्दरगाह था। यहाँ से शल्य चिकित्सा, धातु उद्योग, मनका उद्योग तथा मुहरं निर्माण आदि के प्रमाण मिले हैं।
- चन्हूदड़ो – वर्तमान पाकिस्तान में स्थित यह नगर शिल्पकारी के कार्यों के लिए प्रमुख केन्द्र था। यहाँ से तैयार मनके, शंख, बाट तथा मुहरें आदि बड़े नगरों में भेजी जाती थीं।
- कालीबंगा – राजस्थान में स्थित यह स्थल भी सिन्धु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से भी नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ सड़कें 1.8, 3.6, 5.4 व 7.2 मी. चौड़ी होती थीं जो समानुपातिक ईंटों से बनी हैं। इस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अग्निकुण्ड व अग्निवेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं जो धार्मिक जीवन में तप, योग व यज्ञ का प्रमाण देती हैं।
अन्य केन्द्र: इनके अतिरिक्त धौलावीरा, हरियाणा में स्थित बनावली, सुरकोटड़ा आदि सिन्धु सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं।
प्रश्न 8. सिन्धु सरस्वती सभ्यता की धार्मिक स्थिति तथा लोगों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालो।
उत्तर: सिन्धु संरस्वती सभ्यता के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इस सभ्यता के लोगों का धर्म क्या था? कारण यह है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन में कोई मन्दिर या सुस्पष्ट धार्मिक सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। खण्डहरों के उत्खननों से प्राप्त अवशेषों (मुहरों, मूर्तियों, अग्निवेदिकाएँ) की सहायता से पुरातत्वविदों ने धार्मिक स्थिति। तथा धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाए हैं-
1. मातृशक्ति की पूजा:
सिन्धु घाटी के लोग मातृ देवी या मातृ शक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों से मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली हैं। इस देवी का उनके धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव था। यह दैवीय शक्ति या ईश्वरी शक्ति का प्रतीक थी। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाई देता है, संभवत: यह पृथ्वी माता का स्वरूप है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मान्यता के अनुसार मातृशक्ति सभी की उत्पत्ति का स्रोत थी।
2. शिव की पूजा:
सिन्धु घाटी के लोग एक देवता की पूजा करते थे। इस सभ्यता से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है। इसके एक तरफ हाथी व बाघ है दूसरी तरफ भैंसा व गेंदा है, नीचे हिरण है। एक अन्य.मुहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति की आकृति त्रिमुखी एवं त्रिशृंगी है तथा नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया है। इससे पशुपतिनाथ या आद्य शिव की पूजा के संकेत मिलते हैं।
3. पशुओं की पूजा:
सिन्धु घाटी के लोग बैल, शेर, बाघ व हाथी आदि पशुओं की भी पूजा करते थे। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर एक सींग वाले वृषभ का चित्रण मिलता है। इसके अलावा कूबड़दार बैल, बिना कूबड़दार बैल, बाघ व हाथी का चित्रण मिलता है। विभिन्न पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए।
4. वृक्षों की उपासना:
सिन्धु घाटी के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष पूजा को इस समय प्रचलन था। एक मुहर में देवता को दो पीपल के वृक्ष के मध्य दिखाया गया है। सात मानवाकृतियाँ उसकी पूजा कर रही हैं।
5. प्रकृति पूजा:
प्रकृति की पूजा की जाती थी। कालीबंगा, वनावली, राखीगढ़ी तथा लोथल के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं, अग्निवेदियों में राख के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इससे यज्ञ सम्बन्धी अनुष्ठान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शुभ अवसरों और विशेष पर्वो और जल पूजा के साक्ष्य मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से प्राप्त होते हैं।
प्रश्न 9. प्राचीन समाज़ में परिवार व्यवस्था तथा स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर: परिवार व्यवस्था की संकल्पना भारतीय सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। परिवार व्यवस्था ने व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर समाज व राष्ट्र तक पहुँचाया है। इसी भाव से हम भारतीय वसुधैव कुटुम्बकम् का विश्व – संदेश देते हैं। पुरा ऐतिहासिक युग (सिन्धु सरस्वती सभ्यता) में भी हमें परिवार की संकल्पना के अवशेष दिखाई देते हैं। अनेक संख्या में मातृ-मृणमूर्तियों के अवशेष मिले हैं जो कि उस समय के मातृसत्तात्मक परिवार का संकेत देते हैं। सिन्धु सभ्यता में स्त्रियों का आदर होता था एवं परिवार में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।
स्त्रियाँ पुरुषों के साथ विभिन्न सामाजिक व धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं। खुदाई में जितनी मानव आकृतियों के चित्र मिले हैं उनमें अधिकांश स्त्रियों के हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है। कि स्त्रियाँ समाज में समादृत थीं। इनका मुख्य कार्य सन्तान का लालन – पालन एवं गृह संचालन था। वैदिक काल में परिवार को कुटुम्ब कहा जाता था। उसमें दो या तीन पीढ़ियों के लोग रहते थे। वैदिक युग में पितृ सत्तात्मक परिवारों का उल्लेख है, लेकिन पुत्र व पुत्री के सामाजिक व धार्मिक अधिकारों में अन्तर नहीं था। पुत्र के समान ही पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा व यज्ञ करने का अधिकार था। प्राचीन काल में पत्नी और माँ के रूप में स्त्री की अत्यधिक प्रतिष्ठा थी।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता (जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं) का भाव भारतीय समाज में था। ऋग्वेद की कुछ रचनाओं की स्रष्टा ऋषियों की तरह ऋषिकाएँ भी थीं। घोषा, अपाला, लोपमुद्रा आदि जैसी विदुषी महिलाएँ याज्ञिक अनुष्ठानों का सम्पादन करती थीं। प्राचीन भारतीय कुटुम्ब का स्वरूप पति – पत्नी, माता – पिता व बच्चों के सम्बन्ध पर आधारित था। पुरुष व स्त्री के सम्बन्धों का मूल आधार विवाह संस्था थी। यही संस्था परिवार की आधारशिला थी। इस प्रकार प्राचीन भारतीय समाज में परिवार व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति अन्य कालों की अपेक्षा अच्छी थी।
प्रश्न 10. प्राचीन भारत में खगोल, ज्योतिष, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर: प्राचीन भारत खगोल विद्या, ज्योतिष विधा, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अत्यन्त समृद्ध था। इस बात को हम निम्नलिखित विवरण द्वारा समझ सकते हैं।
1. खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान:
अपनी निरीक्षण शक्ति के बल पर प्राचीन भारतीय अन्वेषकों ने अन्तरिक्ष, तारे, ब्रह्माण्ड आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। सम्बन्धित ग्रन्थों की रचना की। भारतीय पंचांग प्रणाली से प्रकट होता है कि पृथ्वी का आकार और भ्रमण, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, ग्रह – उपग्रह, तारों की गति, सताईस नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी व गणना वर्तमान प्रगति विज्ञान के युग में भी सटीक हैं। जब विश्व को पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी नहीं थी तब आर्यभट्ट ने पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।
तारों व ग्रहों की गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में है। प्राचीन ज्योतिषविदों द्वारा प्रतिपादित चन्द्र का पृथ्वी के चारों ओर घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर बारह राशियाँ, सताईस नक्षत्र, तीस दिन का चन्द्र मास, बारह मास का वर्ष, चन्द्र व सौर वर्ष में समन्वय हेतु तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) द्वारा समायोजन आदि सिद्धान्त आज भी यथावत् चल रहे हैं।
2. भौतिक तथा रसायन विज्ञान:
कणाद ऋषि वैशेषिक दर्शन के रचयिता एवं अणु सिद्धान्त के प्रवर्तक थे। इनमें हमें प्राचीन भारत में भौतिक विज्ञान की प्रगति की जानकारी मिलती है। कणाद ने पदार्थ (matter) उसके संघटक तत्व व गुण (atoms) का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। अणुओं के संयोजन की विशद् धारणा भी कणाद ने दी। पदार्थ (matter) कार्यशक्ति (power) गति (motion) व वेग (velocity) आदि विषयक भौतिक सिद्धान्त प्राचीन ऋषियों व विद्वानों ने दिये।
यूरोप में 14वीं शताब्दी में भौतिकी के जो. सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये, वे पांचवीं शताब्दी के प्रशस्तपाद के ‘पदार्थ धर्म संग्रह’ व व्योम शिवाचार्य के ‘व्योमवती’ ग्रन्थों में उपलब्ध है। प्राचीन काल में भारतीयों को रासायनिक मिश्रण का भी ज्ञान था, इसका उदाहरण मेहरौली (दिल्ली) को लोह स्तम्भ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा।
मानचित्र कार्य
प्रश्न 1. भारत के मानचित्र में हड़प्पा – सभ्यता के किन्हीं 4 स्थानों को चिह्नित कर उनके नाम लिखिए।
उत्तर:
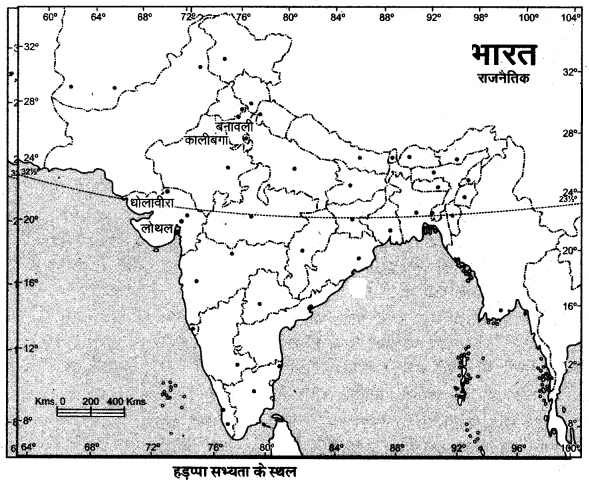
प्रश्न 2. भारत के मानचित्र में सोलह महाजनपद राज्यों को दर्शाइये।
उत्तर:
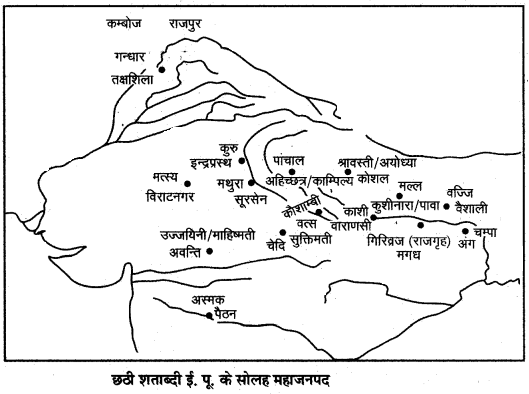
CLCIK HERE FOR FREE MOCK TEST
CLICK HERE FOR ALL CLASS STUDY MATERIAL 2021
JOIN TELEGRAM
SUBSCRIBE US SHALA SUGAM
SUBSCRIBE US SHIKSHA SUGAM
(Jan Aadhaar) राजस्थान जन आधार कार्ड पंजीकरण 2021 HOW TO APPLY FOR JAN AADHAAR AT HOME ऑनलाइन आवेदन दस्तावेजRAJASTHAN SINGLE DAUGHTER DAUBLE DAUGHTER SCHEMEपन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना )
SOME USEFUL POST FOR YOU
⇓ ⇓ ⇓
![SMILE 3 CLASS 8]()
by Sheetal Panwar | Apr 13, 2021 | CLASS 10, E CONTENT, REET, STUDENT CORNER |
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 5 CHEMEISRY IN EVERYDAY LIFE
K. L. SEN MERTA (M.Sc. M.A. B.Ed.)
SCIENCE EDUCATOR,
These Solutions for Class 10 Science Chapter 5 दैनिक जीवन में रसायन are part of Solutions for Class 10 Science. Here we have given Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 5 दैनिक जीवन में रसायन
| Board |
RBSE |
| Textbook |
SCERT, Rajasthan |
| Class |
Class 10 |
| Subject |
Science |
| Chapter |
Chapter 5 |
| Chapter Name |
दैनिक जीवन में रसायन . |
| Number of Questions Solved |
102 |
| Category |
RBSE CLASS X |
आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न
1. क्षार का जलीय विलयन
(क) नीले लिटमस को लाल कर देता है।
(ख) लाल लिटमस को नीला कर देता है।
(ग) लिटमस विलयन को रंगहीन कर देता है।
(घ) लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।
2. अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के–
(क) कुचालक
(ख) सुचालक
(ग) अर्द्धचालक
(घ) अप्रभावित
3. pH किन आयनों की सान्द्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है?
(क) [H2O]
(ख) [OH-]
(ग) [H+]
(घ) [Na+]
4. किसी अम्लीय विलयन की pH होगी
(क) 7
(ख) 14
(ग) 11
(घ) 4
5. हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है
(क) अम्लीय
(ख) क्षारीय
(ग) उदासीन
(घ) परिवर्तनशील
6. अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है
(क) सोडियम कार्बोनेट
(ख) सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
(ग) प्लास्टर ऑफ पेरिस
(घ) सोडियम क्लोराइड
7. धावन सोडा होता है..
(क) NaHCO3
(ख) NaCl
(ग) CaSO4.½H2O
(घ) Na2CO3.10 H2O
8. विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है?
(क) H2
(ख) O2
(ग) Cl2
(घ) CO2
9. साबुन कार्य करता है
(क) मृदु जल में
(ख) कठोर जल में
(ग) कठोर व मृद दोनों में
(घ) इनमें से कोई नहीं
10. मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है
(क) अंदर की तरफ
(ख) बाहर की तरफ
(ग) परिवर्तनशील
(घ) किसी भी तरफ
11. प्रोटॉन [H+] ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं
(क) अम्ल
(ख) लवण
(ग) इनमें से कोई नहीं
(घ) क्षार
1. (ख) 2. (ख)
3. (ग) 4. (घ)
5. (क) 6. (ख)
7. (घ) 8. (ग)
9. (क) 10. (क)
11. (घ)
प्रश्न 12. लाल चींटी के डंक में कौनसा अम्ल पाया जाता है?
उत्तर- लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल (HCOOH) पाया जाता है।
प्रश्न 13. प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं ?
उत्तर- प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक अम्ल कहलाते हैं।
प्रश्न 14. उदासीनीकरण से क्या समझते हैं ?
उत्तर- अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें लवण तथा जल बनते हैं।
उदाहरण- NaOH + HCl → NaCl + H2O
प्रश्न 15. पेयजल को जीवाणुमुक्त कैसे किया जा सकता है?
उत्तर- पेयजल को विरंजक चूर्ण (CaOCl2) द्वारा जीवाणुमुक्त किया जा सकता है।
प्रश्न 16. अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? समीकरण दें।
उत्तर- अम्ल, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं।
उदाहरण- 2HCl अम्ल + MgO धात्विक ऑक्साइड → MgCl2 लवण + H2O
प्रश्न 17. pH में p एवं H किसको सूचित करते हैं?
उत्तर- pH में p एक जर्मन शब्द पुसांस अर्थात् शक्ति तथा H, हाइड्रोजन आयनों का सूचक है।
प्रश्न 18. हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे?
उत्तर- हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए दुर्बल। क्षार जैसे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड [Mg(OH)2] जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है जो कि एन्टएसिड होता है।
प्रश्न 19. सोडियम के दो लवणों का नाम लिखें।
उत्तर-
- धावन सोडा (सोडियम कार्बोनेट)-Na2CO2.10H2O
- साधारण नमक (सोडियम क्लोराइड)-NaCl
प्रश्न 20. लुइस के अनुसार क्षार की परिभाषा दें।
उत्तर- इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इन्हें लुइस क्षार कहते हैं। जैसे NH3
प्रश्न 21. साबुनीकरण किसे कहते हैं ?
उत्तर- उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
प्रश्न 22. अपमार्जक की क्या विशेषता है?
उत्तर- अपमार्जक कठोर जल तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में सफाई का कार्य करते हैं।
प्रश्न 23. हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर- प्लास्टर ऑफ पेरिस (CaSO4.½H2O)
प्रश्न 24. एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता 1 x 10-4 gm mole L-1 है। विलयन का pH मान ज्ञात करें। बताइए कि यह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय?
उत्तर-
pH = – log [H+]
pH = – log [1 x 10-4]
pH = – (log 1 + log 10-4)
pH = – (0 – 4 log 10)
pH = 4
यह विलयन अम्लीय होगा क्योंकि अम्लीय विलयन की pH, 7 से कम होती है।
प्रश्न 25. दो प्रबल अम्ल एवं दो प्रबल क्षारों के नाम तथा उपयोग लिखें।
उत्तर-
(a) प्रबल अम्ल-
- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)-यह अम्लराज बनाने में प्रयुक्त होता है जो कि सोने जैसी धातु को भी विलेय कर देता है। अम्लराज बनाने के लिए इसे HNO3 के साथ मिलाया जाता है।
- सल्फ्यूरिक अम्ल (H2SO4)-यह सेल, कार बैटरी तथा उद्योगों में काम आता है।
(b) प्रबल क्षार-
- सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)-इसे बॉक्साइट के धातुकर्म तथा पेट्रोलियम के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है।
- पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH)-इसे साबुन तथा अन्य उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है।
प्रश्न 26. साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए।
उत्तर-
साबुन और अपमार्जक में अन्तर
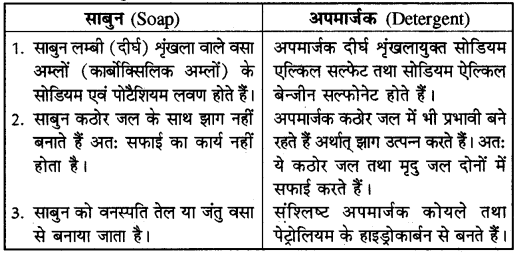
प्रश्न 27. आरेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषाएं लिखिए।
उत्तर- आरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+
या H3O+ देते हैं। जलीय विलयन में H+ स्वतंत्र नहीं रहता। यह H2O से क्रिया करके H3O+ बना लेता है। जैसे-HCl, HNO3 इत्यादि।
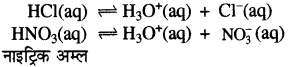
क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- (हाइड्रॉक्साइड). आयन देते हैं। जैसे-NaOH, KOH इत्यादि
प्रश्न 28. pH किसे कहते हैं? अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की pH परास को स्पष्ट करें।
उत्तर- pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता को मापता है।
अर्थात् हाइड्रोजन आयनों की सान्द्रता के ऋणात्मक लागेरिथ्म (लघुगणक) को pH कहते हैं।
pH = – log10 [H+]
H+ जल से क्रिया करके [H3O+] हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अतः pH को निम्न प्रकार भी दिया जाता है
pH = – log10 [H3O+]
[H+] आयनों की सान्द्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होगा। जल उदासीन होता है जिसके उदासीन लिए [H+] तथा [-OH] आयनों की सान्द्रता 1 x 10-7 मोल/लिटर होती हैं। अतः इसकी pH 7 होगी।
इस प्रकार
pH = 0 से < 7 तक विलयन अम्लीय,
pH = 7 विलयन उदासीन,
pH > 7 से 14 तक विलयन क्षारीय होता है।
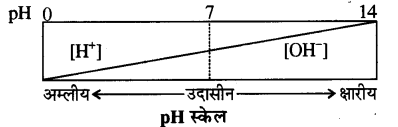
प्रश्न 29. क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? उदाहरण दें।
उत्तर- किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे-Na2CO3.10H2O
यहाँ सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 अणु जल के क्रिस्टलन जल के रूप में हैं। अन्य उदाहरण –
CaSO4.2H2O, (जिप्सम) K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.(फिटकरी)
प्रश्न 30. क्या होता है जब
- दही या खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में रखा जाता है?
- रात्रि में भोजन के पश्चात् दाँतों को साफ नहीं किया जाता है?
उत्तर-
- दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। अतः जब इन्हें पीतल एवं ताँबे जैसी धातुओं के बर्तनों में रखा जाता है, तो ये अम्लों की उपस्थिति के कारण पीतल एवं ताँबा की सतह से क्रिया कर विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं।
- रात्रि में भोजन के पश्चात् दाँतों को साफ नहीं करने पर मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दाँतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ‘जिससे मुख की pH कम हो जाती है तथा pH का मान 5.5 से कम होने पर दाँतों के इनैमल का क्षय होने लगता है।
प्रश्न 31. एक यौगिक A अम्ल H2SO4, से क्रिया करता है तथा बुदबुदाहट के साथ गैस B निकालता है। गैस B जलाने पर फट-फट ध्वनि के साथ जलती है। A व B का नाम बताइए तथा अभिक्रिया का समीकरण दें।
उत्तर-
तत्व A, जिंक (Zn) है तथा गैस B, हाइड्रोजन है, जिसे जलाने पर यह फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है।
समीकरण- Zn(s) जिंक + H2SO4(aq) सल्फ्यूरिक अम्ल, → ZnSO4(aq) जिंक सल्फेट + H2(g) हाइड्रोजन
प्रश्न 32. ब्रांस्टेड-लोरी तथा लुइस के अनुसार अम्ल एवं क्षार को स्पष्ट करें।
उत्तर-
ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना–ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार ‘अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं।” उन्होंने संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षारक की अवधारणा भी दी।
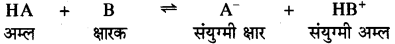
(HA – A–) को अम्ल-संयुग्मी क्षार युग्म तथा (B – HB+) को क्षारसंयुग्मी अम्ल युग्म कहते हैं।
उदाहरण-
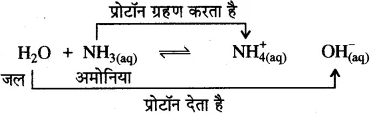
यहाँ जल प्रोटॉन दाता है अतः यह अम्ल है, यह प्रोटॉन देकर संगत संयुग्मी क्षार (OH–) में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया (NH3) प्रोटॉन ग्राही है, अतः यह क्षार है और यह प्रोटॉन ग्रहण करके संगत संयुग्मी अम्ल (NH4+) अमोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। NH4+ – NH3 तथा H2O – OH– युग्मों को संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म कहते हैं। अतः संयुग्मी अम्ल-क्षार युग्म में केवल एक प्रोटॉन (H+) का अन्तर होता है।
अन्य उदाहरण
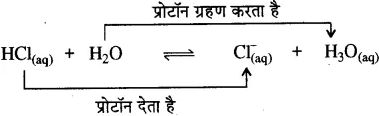
लुइस संकल्पना-लुइस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अतः अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही तथा क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं।
जैसे- BE3, अम्ल + :NH3, क्षार → F3B ← NH3
लुइस अम्ल तथा लुइस क्षार आपस में मिलकर उपसहसंयोजक बन्ध द्वारा योगात्मक यौगिक बनाते हैं। उपरोक्त उदाहरण में BF3, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अमोनिया से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है।
इस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं। साधारणतया धनायन, या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, लुइस अम्ल होते हैं। जैसे-BF3, AlCl3, Mg+2, Na+ आदि।
इलेक्ट्रॉन धनी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक लुइस क्षार का कार्य करते हैं। उदाहरण-H2O::, :NH3, OH–, Cl– आदि।।
अतः केवल H+ या OH- युक्त पदार्थ ही अम्ल एवं क्षार नहीं होते हैं। इन संकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन रहित यौगिको के अम्लीय तथा क्षारीय गुणों की व्याख्या भी की जा सकती है।
प्रश्न 33. pH के सामान्य जीवन में उपयोग बताइए।
उत्तर-
हमारे सामान्य जीवन (दैनिक जीवन) में pH के उपयोग निम्नलिखित हैं
- उदर में अम्लता- हमारे पाचन तंत्र में pH का बहुत महत्त्व होता है। हमारे उदर के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) होता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। उदर में अम्लता की स्थिति में, उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसके लिए ऐन्टैसिड का उपयोग किया जाता है। यह ऐन्टैसिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड (मिल्क ऑफ मैगनीशिया) [Mg(OH)2] जैसे दुर्बल क्षारकों को उपयोग किया जाता है।
- दंत क्षय- मुख की pH साधारणतया 6.5 के करीब होती है। खाना खाने के पश्चात् मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दाँतों में लगे अवशिष्ट भोजन (शर्करा एवं खाद्य पदार्थ) से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख की pH कम कर देते हैं। pH का मान 5.5 से कम होने पर दाँतों का इनैमल, जो कि कैल्सियम फास्फेट का बना होता है, का क्षय होने लग जाता है। अतः भोजन के पश्चात् दंतमंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, जिससे अम्ल की आधिक्य मात्रा उदासीन हो जाती है, इससे दंतक्षय पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
- कीटों का डंक- मधुमक्खी, चींटी तथा मकोड़े जैसे कीटों के डंक अम्ल स्रावित करते हैं, जो हमारी त्वचा के सम्पर्क में आता है। जिसके कारण ही त्वचा पर जलन तथा दर्द होता है। दुर्बल क्षारकीय लवणों जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट (NaHCO3) का प्रयोग उस स्थान पर करने पर अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाता है।
- अम्ल वर्षा- वर्षा के जल को सामान्यतः शुद्ध माना जाता है लेकिन जब वर्षा के जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस वर्षा जल से नदी तथा खेतों की मिट्टी प्रभावित होती है, जिससे फसलों, जीवों तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है। अतः प्रदूषकों को नियंत्रित करके अम्ल वर्षा को कम किया जा सकता है।
- मृदा की pH- अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। अतः विभिन्न स्थानों की मिट्टी की pH ज्ञात करके उसमें बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार उसका उपचार किया जाता है। जब मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उसमें चूना (CaO) मिलाया जाता है तथा मिट्टी के क्षारीय होने पर उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिलाकर उचित pH पर लाया जाता है। pH के अनुसार ही उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जिससे अच्छी फसल प्राप्त होती है।
प्रश्न 34. निम्नलिखित के नाम, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए
(i) NaOH
(ii) NaHCO3
(iii) Na2CO3.10H2O
(iv) CaOCl2,
(v) CaSO4.½H2O
उत्तर-
(i) NaOH-इसका नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड है तथा इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं।
बनाने की विधि-औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके साथ ही कैथोड पर विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी प्राप्त होता है।
2NaCl(aq) + 2H2O → 2NaOH(aq) + Cl2(g) + H(g)
उपयोग- NaOH के उपयोग निम्न हैं
- साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में
- बॉक्साइट के धातुकर्म में
- पेट्रोलियम के शोधन में
- वसा तथा तेलों के निर्माण में
- प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में
(ii) NaHCO3-इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
बनाने की विधि-
(a) NaCl की NH3 तथा CO2 गैस से अभिक्रिया द्वारा NaHCO3 का निर्माण किया जाता है।
NaCl + H2O + CO2 + NH3 → NH4Cl अमोनियम क्लोराइड + NaHCO3
(b) सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाईऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से भी NaHCO3 का निर्माण होता है।
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट + CO2 + H2O → 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन ,कार्बोनेट
उपयोग-NaHCO3 के उपयोग निम्न प्रकार हैं
- खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, जो कि बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है।
- सोडा वाटर तथा सोडायुक्त शीतल पेय बनाने में,
- पेट की अम्लता को दूर करने में एन्टा एसिड के रूप में,
- मंद पूतिरोधी के रूप में,
- अग्निशामक यंत्र में,
- प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में।
(iii) Na2CO3.10H2O-इसे कपड़े धोने का सोडा ( धावन सोडा) कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है।
बनाने की विधि-
(a) सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि से किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त किया जाता है।
(b) बेकिंग सोडा को गर्म करने पर भी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है।
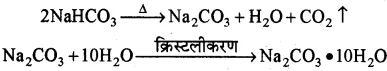
उपयोग- धावन सोडा के उपयोग निम्न हैं
- धुलाई एवं सफाई में,
- कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, काँच, साबुन तथा बोरेक्स के निर्माण में,
- अपमार्जक के रूप में,
- कागज, पेन्ट तथा वस्त्र उद्योग में,
- प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
(iv) CaOCl2– इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं तथा इसका रासायनिक नाम कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड है।
बनाने की विधि-शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है।
Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड
उपयोग-विरंजक चूर्ण के उपयोग निम्न हैं
- वस्त्र उद्योग तथा कागज उद्योग में विरंजक के रूप में,
- पेयजल को शुद्ध करने में,
- रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में,
- प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
(v) CaSO4.½H2O-इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस (P.O.P) कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्सियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट (हेमी हाइड्रेट) है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सर्वप्रथम जिप्सम को गर्म करके इसे बनाया गया था अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया।
बनाने की विधि
जिप्सम (CaSO4.2H2O) को 393K ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है।
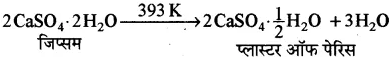
P.O.P. को और अधिक गर्म करने पर सम्पूर्ण क्रिस्टलन जल बाहर निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर [CaSO4] प्राप्त होता है।
उपयोग- प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्न हैं
- टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर करने तथा जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में,
- अग्निसह पदार्थ के रूप में,
- भवन निर्माण में,
- दंत चिकित्सा में,
- मूर्तियाँ तथा सजावटी सामान बनाने में।
प्रश्न 35. मिसेल कैसे बनते हैं? क्रियाविधि भी दें।
उत्तर-
साबुन तथा अपमार्जक, मिसेल बनाकर ही शोधन की क्रिया करते हैं। सर्वप्रथम साबुन (जैसे सोडियम स्टिएरेट) के अणुओं का जल में आयनन होता है।
C17H35COONa → C17H35COO– + Na+
सोडियम स्टिएरेट
इसे सामान्य सूत्र के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं|
R COONa → R COO– + Na+
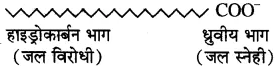
इसमें हाइड्रोकार्बन पूंछ (R) जल विरोधी तथा ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होता है। ये दोनों भाग इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई के अंदर की तरफ तथा ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ होता है। इसे मिसेल कहते हैं ।
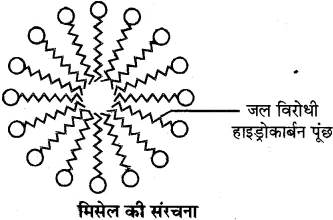
क्रियाविधि-अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद तथा चिकनाई जल में अघुलनशील परन्तु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। साबुन के द्वारा सफाई की प्रक्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जलस्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ रहता है। इस प्रकार यह चिकनाई को चारों ओर से घेर कर मिसेल बना लेता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं, इससे सम्पूर्ण चिकनाई जल की तरफ खिंचकर बाहर निकल जाती है।
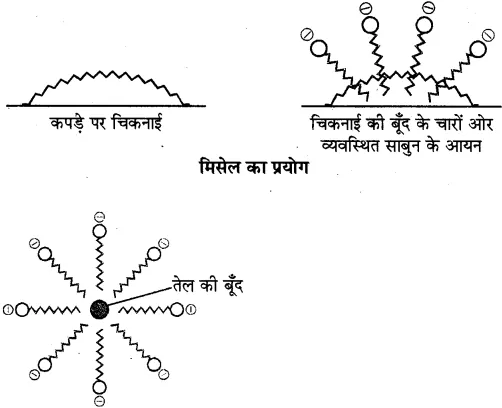
शोधन क्रिया-साबुन के द्वारा घिरी चिकनाई की बूंद (मिसेल)
सभी मिसेल ऋणावेशित (समान आवेशित) होते हैं अतः इनका अवक्षेपण नहीं होता है तथा ये मिसेल, विलयन में कोलॉइडी अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के पश्चात् पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से पृथक् होकर पानी में आ जाती है तथा कपड़ा साफ हो जाता है।
( आपकी पाठ्य पुस्तक के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर )
1. दाँत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है?
(अ) क्षारीय
(ब) अम्लीय
(स) उदासीन
(द) संक्षारकीय
2. पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
(अ) बेकिंग सोडा
(ब) विरंजक चूर्ण
(स) धोने का सोडा
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
3. आसुत जल की pH का मान होता है
(अ) 9
(ब) 7
(स) 5
(द) 3
4. हमारे रुधिर की प्रकृति होती है
(अ) अम्लीय
(ब) क्षारीय
(स) उदासीन
(द) कुछ अम्लीय व कुछ क्षारीय
5. अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति होती है
(अ) क्षारीय
(ब) अम्लीय
(स) उदासीन
(द) अक्रिय
6. बेकिंग सोडा को गर्म करने पर निम्न में से कौनसा यौगिक बनता है?
(अ) NaNO3
(ब) Na2CO3
(स) NH4Cl
(द) NaHCO3
7. कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है तो इस विलयन में निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक होगा?
(अ) NaCl
(ब) HCl
(स) LiCl
(द) KCl
8. तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है?
(अ) Zn
(ब) Mg
(स) Fe
(द) उपरोक्त सभी
9. साबुन बनाने की प्रक्रिया में सहउत्पाद है
(अ) NaOH
(ब) ग्लिसरॉल
(स) वसा व अम्ल
(द) ऐल्कोहॉल
10. अपमार्जक सामान्यतः होते हैं
(अ) RCOONa
(ब) RCOOK
(स) RSO4Na .
(द) RCOOR
1. (अ) 2. (ब)
3. (ब) 4. (ब)
5. (ब) 6. (ब)
7. (ब) 8. (द)
9. (ब) 10. (स)
प्रश्न 1. बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख घटक लिखिए।
उत्तर-
- NaCl (सोडियम क्लोराइड)
- CO2, NH3 इत्यादि।
प्रश्न 2. दो अम्लीय ऑक्साइडों के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्ल वर्षा होती
उत्तर-
प्रश्न 3. ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है, लेकिन वे अम्ल नहीं हैं तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता।
उत्तर- ऐल्कोहॉल (C2H5OH) तथा ग्लुकोज (C6H12O6
प्रश्न 4. हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी?
उत्तर- सोरेन्सन
प्रश्न 5. टमाटर के रस का pH कितना होता है?
उत्तर- टमाटर का रस अम्लीय होता है तथा इसके pH का मान 4.0-4.4 होता है।
प्रश्न 6. मनुष्य के मूत्र के pH का मान बताइए।
उत्तर- pH = 5.5-7.5
प्रश्न 7. Zn की NaOH विलयन से क्रिया करवाने पर H2 गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए।
उत्तर- Zn(s) + 2NaOH(aq) → Na2ZnO2(aq) सोडियम जिंकेट + H2
प्रश्न 8. धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर- धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे CaO, MgO.
प्रश्न 9. प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों के दो-दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर- प्रबल अम्ल-HCl (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल), H2SO4 (सल्फ्यूरिक अम्ल)।
प्रबल क्षार-NaOH (सोडियम हाइड्रॉक्साइड), KOH (पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड)।
प्रश्न 10 दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारों के दो-दो उदाहरण लिखिए।
उत्तर- दुर्बल अम्ल- CH3COOH, HCN
दुर्बल क्षार- NH4OH, Mg(OH)2
प्रश्न 11. निम्न में से किसका pH अधिक होता है
(i) रक्त अथवा आसुत जल
(ii) जठर रस अथवा नींबू का रस?
उत्तर- (i) रक्त
(ii) जठर रस।।
प्रश्न 12. जठर रस की pH कितनी होती है?
उत्तर- जठर रस की pH लगभग 1.2 होती है।
प्रश्न 13. टमाटर में कौनसा अम्ल पाया जाता है?
उत्तर- टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है।
प्रश्न 14. सोडियम वर्ग के चार लवण बताइए।
उत्तर- सोडियम सल्फेट (Na2SO4), सोडियम क्लोराइड (NaCl), सोडियम नाइट्रेट (NaNO3), सोडियम कार्बोनेट (Na2CO3)
प्रश्न 15.सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों?
उत्तर- सोडियम एसीटेट (CH3COONa), दुर्बल अम्ल (CH3COOH) तथा प्रबल क्षार (NaOH) से बना लवण है अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है।
प्रश्न 16.सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर कौनसी गैस प्राप्त होती है?
उत्तर- सोडियम क्लोराइड (NaCl) के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर H, तथा एनोड पर Cl) गैस बनती है।
प्रश्न 17 बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए।
उत्तर- NaCl + H2O + CO2 + NH3 → NH4Cl अमोनियम क्लोराइड + NaHCO3 बेकिंग सोडा
प्रश्न 18. CuSO4. 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है?
उत्तर- CuSO4. 5H2O को नीला थोथा कहते हैं।
प्रश्न 19. संतरे में कौनसा अम्ल उपस्थित होता है?
उत्तर- एस्कार्बिक अम्ल ।।
प्रश्न 20. जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है?
उत्तर- जिप्सम (CaSO4. 2H2O) का रासायनिक नाम कैल्सियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है।
प्रश्न 21. कैल्सियम कार्बोनेट (CaCO3) के विभिन्न रूप कौनसे होते हैं?
उत्तर- चूना पत्थरे (Lime Stone), खड़िया (Chalk) एवं संगमरमर (Marble) ।।
प्रश्न 22. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया [Mg(OH)2] की pH कितनी होती है?
उत्तर- pH = 10
प्रश्न 23.विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए।
उत्तर- CaOCl2
प्रश्न 24.धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय होता है अथवा क्षारीय?
उत्तर- क्षारीय।
प्रश्न 25 .ताजे दूध का pH मान 6 होता है। इससे दही बन जाने पर इसका pH मान घटेगा या बढ़ेगा तथा क्यों ?
उत्तर- दूध से दही बन जाने पर pH मान घटेगा क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है।
प्रश्न 26.यदि आप लिटमस पत्र (लाल एवं नीला) से साबुन की जाँच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा?
उत्तर- साबुन का विलयन क्षारीय होता है क्योंकि यह दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बना लवण है। अतः यह लाल लिटमस को नीला करता है, लेकिन नीले । लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता।
प्रश्न 27.सोडियम स्टिएरेट का सूत्र क्या होता है ?
उत्तर- C17H35COO–Na+ (सोडियम स्टिएरेट)।
प्रश्न 1. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए
(i) ब्लीचिंग पाउडर (A) CaSO4. 2H2O
(ii) जिप्सम (B) (NH4)2CO3
(iii) अमोनियम कार्बोनेट (C) CaOCl2
उत्तर-
(i) (C)
(ii) (A)
(iii) (B)
प्रश्न 2. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए
(i) लेक्टिक अम्ल (A) संतरा में
(ii) एसीटिक अम्ल (B) दही में
(iii) एस्कार्बिक अम्ल (C) सिरका में
उत्तर-
(i) (B)
(ii) (C)
(iii) (A)
प्रश्न 1. (अ) pH पैमाने को चित्र द्वारा समझाइये।
(ब) (i) कीटों के डंक मारने पर त्वचा पर जलन क्यों होती है?
(ii) उदर में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए दुर्बल क्षारकों का उपयोग क्यों किया जाता है? (माध्य. शिक्षा बोर्ड, मॉडल पेपर, 2017-18 )
उत्तर-
(अ) pH पैमाने का चित्र
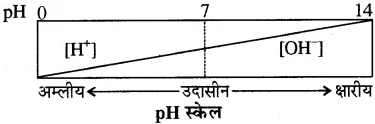
(ब) (i) कीट डंक से अम्ल स्रावित करते हैं, जैसे लाल चींटी फार्मिक अम्ल स्रावित करती है, जिसके सम्पर्क में आने पर त्वचा पर जलन होती है।
(ii) उदर में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए दुर्बल क्षारकों जैसे Mg(OH)2, का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं।
प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है?
(अ) ऐसीटिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
(ब) सोडियम हाइड्रॉक्साइड अथवा कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड।
उत्तर-
(अ) प्रबल अम्ल-हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
(ब) प्रबल क्षार-सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)
प्रश्न 3. pH स्केल किसे कहते हैं? स्पष्ट करो कि मुँह का pH परिवर्तन दन्त क्षय का कारण है।
उत्तर- pH स्केल-किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सान्द्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH स्केल कहते हैं।
pH स्केल से शून्य (अधिक अम्लता) से 14 (अधिक क्षारीय) तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय एवं pH को मान 7 से ज्यादा हो तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। ।
मुँह की pH का मान 5.5 से कम होने पर दन्त क्षय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुँह में उपस्थित बैक्टीरिया दाँतों में लगे अवशिष्ट भोजन के कणों से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे मुख की pH कम हो जाती है तथा यही दन्त क्षय का कारण है।
प्रश्न 4. (अ) सोडियम हाइड्राक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए। अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए।
(ब) निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है?
(i) पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए
(ii) रसोईघर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में।
(iii) जल की स्थाई कठोरता दूर करने में ।
(iv) खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में।
उत्तर-
(अ) सोडियम हाइड्रॉक्साइड की जिंक धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन (H2) गैस निकलती है।
2 NaOH + Zn → Na2ZnO2 (सोडियम जिंकेट) + H2
(ब) (i) विरंजक चूर्ण ।
(ii) बेकिंग सोडा ।
(iii) धोने का सोडा।
(iv) प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्रश्न 5. स्तम्भ A से B को सुमेलित कीजिए
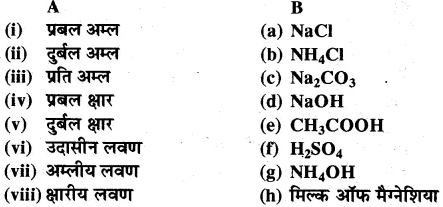
उत्तर-
(i) = f
(ii) = e.
(iii) = h
(iv) = d
(v) = g
(vi) = a
(vii) = b
(viii) = c
प्रश्न 6. विज्ञान की प्रयोगशाला में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक अम्ल (H2SO4), नाइट्रिक अम्ल (HNO3), ऐसीटिक अम्ल (CH3COOH), सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH), कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड [Ca(OH)2], पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH), मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड [Mg(OH)2] एवं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड (NH4OH) में से अम्ल तथा क्षार छाँटिए।
उत्तर- उपरोक्त यौगिकों में से अम्ल तथा क्षार निम्न प्रकार हैं
अम्ल-HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH
क्षार-NaOH, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2, NH4OH
प्रश्न 7. आपको तीन परखनलियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आसवित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे?
उत्तर- तीनों परखनलियों में स्थित विलयन की क्रिया लाल लिटमस पत्र से करवाते हैं। जिस विलयन द्वारा यह लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, वह विलयन क्षारीय होगा। अब इस नीले लिटमस पत्र की क्रिया शेष दोनों विलयनों से करवाते हैं। जिस विलयन द्वारा यह लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा, वह विलयन अम्लीय होगा तथा तीसरी परखनली में स्थित विलयन आसवित जल है क्योंकि आसवित जल उदासीन होता है अतः यह किसी भी लिटमस पत्र से कोई क्रिया नहीं करता।
प्रश्न 8. कोई धातु यौगिक ‘A’ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्सियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
उत्तर-
धातु यौगिक ‘A’ कैल्सियम कार्बोनेट होगा। अभिक्रिया में उत्पन्न एक यौगिक कैल्सियम क्लोराइड है अतः यौगिक कैल्सियम युक्त होगा तथा उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है जो कि CO2, होती है अतः यौगिक ‘A’ जो कि CaCO3 है, की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया इस प्रकार होगी|
CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(aq)(कैल्सियम क्लोराइड) + H2O(l) + CO2(g)↑
प्रश्न 9. HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि ऐल्कोहॉल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं?
उत्तर- HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं अतः ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। लेकिन ऐल्कोहॉल एवं ग्लुकोज के जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनते क्योंकि इनमें सहसंयोजी गुण होता है अतः ये अम्लीयता प्रदर्शित नहीं
प्रश्न 10. शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है?
उत्तर- शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनन नहीं होता अतः यह H+ नहीं देगी अर्थात् अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। अतः H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात् अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं होगा।
प्रश्न 11 अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में?
उत्तर- अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए जल में किसी सान्द्र अम्ल को सावधानीपूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे-धीरे तथा विलयन को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए।
इसके विपरीत सान्द्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है। इससे समीप खड़े व्यक्ति को हानि भी पहुँच सकती है। इससे स्थानीय ताप भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उपयोग किया जाने वाला कॉच का पात्र भी टूट सकता है।
प्रश्न 12. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए।
उत्तर- सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर Na2CO3 H2O तथा CO2 गैस प्राप्त होते हैं।
अभिक्रिया का समीकरण
2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट → Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट + H2O + CO2↑
प्रश्न 13.क्या क्षारकीय विलयन में H+(aq) आयन होते हैं? अगर हाँ, तो यह क्षारकीय क्यों होता है?
उत्तर- हाँ, क्षारकीय विलयन में H+(aq) आयन होते हैं लेकिन क्षारकीय विलयन में H+(aq) स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। क्षारकीय विलयन में H+ तथा OH- के मध्य साम्य होता है तथा H+(aq) की तुलना में OH- (aq) आयन अधिक मात्रा में होते हैं। अतः विलयन क्षारीय होता है।
प्रश्न 14.कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में उसके उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना (कैल्सियम ऑक्साइड), बुझा हुआ चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) या चॉक (कैल्सिय म कार्बोनेट) का उपयोग करेगा?
उत्तर- किसान अपने खेत की मिट्टी को बिना बुझा हुआ चूना (कैल्सियम ऑक्साइड), बुझा हुआ चूना (कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड) या चॉक (कैल्सियम कार्बोनेट) से उस समय उपचारित करेगा, जब मिट्टी में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, क्योंकि ये सभी पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के हैं, जो मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं।
प्रश्न 15. निम्न अक्रियाओं के लिए पहले शब्द-समीकरण तथा संतुलित समीकरण लिखिए
(a) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है।
(b) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के फीते के साथ अभिक्रिया करता है।
(c) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ऐलुमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है।
(d) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है।
उत्तर-
(a) जिंक + तनु सल्फ्यूरिक अम्ल – जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन गैस
Zn(s) + H2SO4(aq) → ZnSO4(aq) + H2(g) ↑
(b) मैग्नीशियम + तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल → मैग्नीशियम क्लोराइड + हाइड्रोजन गैस
Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) ↑
(c) ऐलुमिनियम + तनु सल्फ्यूरिक अम्ल → ऐलुमिनियम सल्फेट + हाइड्रोजन गैस
2Al(s) + 3 H2SO4(aq) + Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g) ↑
(d) लोहा + तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल → फेरस क्लोराइड + हाइड्रोजन गैस
Fe(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g) ↑
प्रश्न 16. आसवित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है, क्यों?
उत्तर- आसवित जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है तथा इसमें H+ आयन नहीं होते। अतः यह उदासीन होता है, इस कारण इसमें विद्युत को चालन नहीं होता जबकि वर्षा जल अम्लीय होता है अतः इसमें हाइड्रोजन आयन (H+) होते हैं। इसी कारण वर्षा जल विद्युत का चालन करता है।
प्रश्न 17 जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, क्यों?
उत्तर- जलं की अनुपस्थिति में कोई भी अम्ल आयनित नहीं होता, अतः अम्ल से हाइड्रोजन आयन (H+) पृथक् नहीं हो पाते। चूँकि हाइड्रोजन आयन ही अम्ल के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता।
प्रश्न 18.पाँच विलयनों A, B, C, D तथा E की जब सार्वत्रिक सूचक से जाँच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4,1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं, तो कौन-सा विलयन-
(a) उदासीन है?
(b) प्रबल क्षारीय है?
(c) प्रबल अम्लीय है?
(d) दुर्बल अम्लीय है?
(e) दुर्बल क्षारीय है?
pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
उत्तर-
(a) उदासीन– pH 7 वाला विलयन D उदासीन है।
(b) प्रबल क्षारीय- pH 11 वाला विलयन C प्रबल क्षारीय है।
(c) प्रबल अम्लीय– pH 1 वाला विलयन B प्रबल अम्लीय है।
(d) दुर्बल अम्लीय- pH 4 वाला विलयन A दुर्बल अम्लीय है।
(e) दुर्बल क्षारीय– pH 9 वाला विलयन E दुर्बल क्षारीय है।।
इन विलयनों की हाइड्रोजन आयन सान्द्रता का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार होगाविलयन C< विलयन E< विलयन D < विलयन A< विलयन B
अर्थात् pH 11 < pH 9< pH 7 < pH 4 < pH 1
प्रश्न 19. परखनली ‘A’ एवं ‘B’ में समान लंबाई का मैग्नीशियम का फीता लेकर परखनली ‘A’ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl) तथा परखनली B’ में ऐसिटिक अम्ल (CH3COOH) डालने पर किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों?
उत्तर- परखनली ‘A’ में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि Mg से HCl तथा CH3COOH दोनों ही क्रिया करके H2 गैस देते हैं। लेकिन CH3COOH की तुलना में HCl अधिक तेजी से क्रिया करता है क्योंकि यह प्रबल अम्ल है, अर्थात् HCl में हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता अधिक होती है।
प्रश्न 20. ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा?
उत्तर- ताजे दूध के pH का मान 6 होता है अर्थात् यह हल्का-सा अम्लीय होता है। जब इसका किण्वन होकर यह दही बन जाता है तो pH का मान 6 से कम हो जाता है क्योंकि दही में अम्लीय गुण अधिक होता है तथा अम्लीय गुण बढ़ने पर pH के मान में कमी आती है।
प्रश्न 21.एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकरे
(a) ता जा दूध के pH मान को 6 ( अम्लीय) से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है, क्यों?
(b) इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है?
उत्तर-
(a) ताजा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध का pH मान 6 (अम्लीय) से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है अर्थात् pH का मान बढ़ जाता है। क्योंकि बेकिंग सोडा (NaHCO3) क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण है। क्षारीय प्रकृति के कारण दूध के परिरक्षण के दौरान बनने वाला अम्ले उदासीन हो जाता है, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता।
(b) बेकिंग सोडायुक्त दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि दूध से दही बनना किण्वन की प्रक्रिया है, जो कि एक निश्चित pH मान पर ही होती है, जो कि लगभग 7 (उदासीन माध्यम) होना चाहिए जबकि NaHCO3 (बेकिंग सोडा) मिलाने पर pH बढ़ जाती है। इससे दूध से दही बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है अर्थात् दूध को क्षारीय से अम्लीय होने में अधिक समय लगता है।
प्रश्न 22. प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी-रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए?
उत्तर- प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के सम्पर्क में आकर जल (H2O) के अणुओं से क्रिया करके शीघ्रता से कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। इस कारण इसे नमीरोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए।
2CaSO4.½H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस + 3H2O → 2CasO4 जिप्सम.2H2O
प्रश्न 23.धातुओं की अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कैसे होती है? क्या यह सभी धातुओं की सभी अम्लों से होती है? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर- धातुएँ अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं तथा अम्ल के शेष भाग के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रि या को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं| अम्ल + धातु → लवण + हाइड्रोजन गैस
Mg(s) + H2SO4(aq) → MgSO4(s) + H2↑
केवल सक्रिय धातुएँ ही हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके H2 देती हैं। कुछ धातुएँ क्षारों से भी क्रिया करके H2 गैस देती हैं तथा लवण भी बनाती हैं, जैसे Zn, Al इत्यादि।
Zn(s) + 2 NaOH(aq) → Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट (लवण) + H2↑
किन्तु ऐसी अभिक्रियाएँ सभी धातुओं के साथ नहीं होती हैं।
प्रश्न 24. धातु कार्बोनेट (Na2CO3) तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट (NaHCO3) की तनु HCl से क्रिया करवाने पर कौनसी गैस बनती है तथा इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? समीकरण सहित समझाइए।
उत्तर- धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की तनु HCl से क्रिया करवाने पर CO2 गैस निकलती है तथा लवण व जल बनता है।
Na2CO3(s) + 2HCl(aq) → 2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
NaHCO3(s) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
प्राप्त CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaCO3 का श्वेत अवक्षेप (दूधिया विलयन) बनता है लेकिन अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्सियम हाइड्रोजन कार्बोनेट [Ca(HCO3)2] बनने के कारण विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है।
Ca(OH)2(aq) चूने का पानी + CO2(g) → CaCO3(s) कैल्सियम कार्बोनेट + H2O(l)
CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) → Ca(HCO3)2(aq)(जले में विलेय)
प्रश्न 25. धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? इनकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर- धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे-धातु ऑक्साइड + अम्ल → लवण + जल
CuO(s) कॉपर ऑक्साइड + 2HCl(aq) →CuCl2(aq) (नील हरित रंग) कॉपर (II) क्लोराइड + H2O(l)
क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइडों को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं।
प्रश्न 26.CO2 जो कि कार्बन (अधातु ) को ऑक्साइड है, क्षार Ca(OH)2 से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। इससे क्या सिद्ध होता है?
उत्तर- CO2 (कार्बन डाइऑक्साइड) Ca(OH)2 (क्षार) से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि CO2 अम्लीय प्रकृति की होती है। यह क्षार एवं अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया के समान है। अतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
CO2(g) + Ca(OH)2(aq) →CaCO3(s) + H2O(l)
प्रश्न 27. अम्ल एवं क्षार की शक्ति किस पर निर्भर करती है? प्रबल एवं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल एवं दुर्बल क्षार से क्या अभिप्राय है?
उत्तर- अम्ल एवं क्षार की शक्ति जलीय विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है।
प्रबल एवं दुर्बल अम्ल-जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे-हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl); जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे-ऐसीटिक अम्ल [CH3COOH]
प्रबल एवं दुर्बल क्षार-जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH- आयन देने वाले क्षार, प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे-NaOH, KOH आदि; जबकि कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे-NH4OH, Mg(OH)2 आदि।।
प्रश्न 28.प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले कुछ अम्लों की सूची बनाइए।
उत्तर- प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्ल निम्न हैं
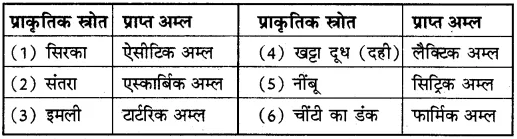
प्रश्न 29. (a) हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए।
(b) अम्ल वर्षा का कारण तथा इसके दो कुप्रभावों को लिखिए।
उत्तर-
(a) हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल को pH स्केल कहते हैं।
(b) अम्ल वर्षा-जब वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाता है, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं।
अम्ल वर्षा के कुप्रभाव-
- अम्ल वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH मान भी कम हो जाता है। ऐसे जल में जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है।
- अम्ल वर्षा के सम्पर्क में आने पर चर्म रोग हो सकता है।
प्रश्न 30. Zn धातु की तनु H2SO4, से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। (माध्य. शिक्षा बोर्ड, 2018)
उत्तर-
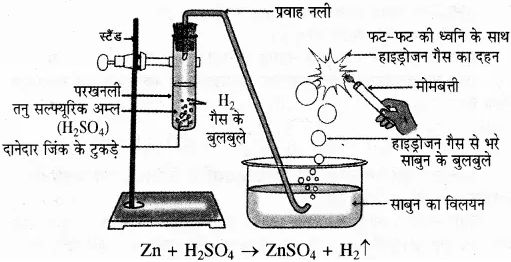
प्रश्न 31. अम्ल-क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना की कमी बताइए।
उत्तर- अम्ल-क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना अप्रोटिक अम्लों एवं क्षारों जैसे CO2SO2, BF3, Cl- इत्यादि के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करती है। अतः अम्ल-क्षार की नई इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना दी गई।
प्रश्न 32.बेकिंग सोडा (NaHCO3) के गुण बताइए।
उत्तर- बेकिंग सोडा के गुण निम्नलिखित हैं
(i) बेकिंग सोडा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है।
(ii) यह जल में अल्प विलेय है।।
(iii) इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है।
(iv) NaHCO3 को गर्म करने पर कार्बन डाईऑक्साइड गैस निकलती है। तथा Na2CO3 बनता है।
2NaHCO3 गर्म करने पर → Na2CO3 + H2O + CO2 ↑
प्रश्न 33.(a) विरंजक चूर्ण की तनु अम्लों से क्रिया के समीकरण लिखिए।
(b) विरं जक चूर्ण का सूत्र लिखिए। इसकी विरंजन क्रिया को समझाइए। (माध्य. शिक्षा बोर्ड, 2018)
उत्तर-
(a) विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है।
CaOCl2 +H2SO4 → CaSO4 + H2O + Cl2↑
CaOCl2 +2 HCl → CaCl2 + H2O + Cl2↑
(b) विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, (कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड) होता है। यह वायु में क्लोरीन गैस देता है जो कि जल से क्रिया कर नवजात ऑक्सीजन [O] देती है। यह ऑक्सीजन ही विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की भाँति व्यवहार करती है।
Cl2 + H2O → 2HCl + [O] परमाण्विक ऑक्सीजन
रंगीन पदार्थ + [O] → रंगहीन पदार्थ
प्रश्न 34. धावन सोडा के गुण बताइए।
उत्तर- (i) धावन सोडा सफेद क्रिस्टलीय ठोस है।
(ii) यह जल में विलेय होता है।
(iii) इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है।
(iv) धावन सोडा को गर्म करने पर यह क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एश। बनाता है।
Na2CO3.10H2O →373k→ Na2CO3 +10H2O
प्रश्न 35. बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर ये फूलकर हल्के हो जाते हैं, क्यों?
उत्तर- बेकिंग सोडा को खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बनडाइ ऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इससे केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र भी पड़ जाते हैं।
प्रश्न 36.क्या आप डिटरजेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं?
उत्तर- डिटरजेंट के उपयोग से यह ज्ञात नहीं कर सकते कि जल कठोर है। अथवा नहीं क्योंकि डिटरजेंट कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है तथा कोई अवक्षेप भी नहीं देता।
प्रश्न 37.लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वाशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है?
उत्तर-
साबुन से कपड़े साफ करने के लिए उन्हें रगड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि साबुन के अणु तेल के धब्बों, मैल के कण आदि को हटने के लिए मिसेल बना सके । मिसेल गन्दे मैल या तेल के धब्बों को हयने में सहायक होता है। अतः कपड़ों को विभिन्न प्रकार से रगड़ने से इनसे गंदगी के कणों को निकालने में सहायता मिलती है।
प्रश्न 38. कास्टिक सोडा के गुण बताइए।
उत्तर- (i) कास्टिक सोडा श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है।
(ii) इसका गलनांक 591 K होता है।
(iii) यह जल में शीघ्र विलेय हो जाता है।
(iv) यह प्रबल क्षार है तथा अपने जलीय विलयन में आयनित रूप में (Na– (aq) + OH– (aq)) रहता है। अतः यह एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है।
(v) इसके क्रिस्टल प्रस्वेद्य होते हैं।
प्रश्न 39.(i) क्या साबुन एथेनॉल में मिसेल का निर्माण करता है, यदि नहीं तो क्यों?
(ii) अप मार्जक का प्रयोग कठोर जल में भी किया जा सकता है, क्यों?
उत्तर- (i) साबुन, एथेनॉल (एथिल ऐल्कोहॉल) में मिसेल का निर्माण नहीं करता क्योंकि यह एथेनॉल में घुल जाता है।
(ii) अपमार्जक लम्बी कार्बन श्रृंखला युक्त सोडियम ऐल्किल सट तथा सोडियम ऐल्किल बेन्जीन सल्फोनेट होते हैं। इन अपमार्जकों के सोडियम आयन, कठोर जल में उपस्थित Ca2+ या Mg+2 आयनों से प्रतिस्थापित होकर कैल्सियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं जो कि जल में घुलनशील है। अतः ये साबुन के समान अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार ये कठोर जल में भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तथा सफाई क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है।
प्रश्न 40.साबुन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करते हैं, क्यों?
उत्तर- साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं क्योंकि कठोर जल में उपस्थित Ca2+ तथा Mg2+ आयन, साबुन के सोडियम आयनों (Na+) को प्रतिस्थापित कर उच्च वसीय अम्लों के कैल्सियम एवं मैग्नीशियम । लवण बनाते हैं जो कि जल में अविलेय होते हैं। अतः ये अवक्षेपित हो जाते हैं अतः सफाई की क्रिया आसानी से नहीं हो पाती तथा झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है।
प्रश्न 41.जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रसायनों के उपयोग का वर्णन कीजिए।
उत्तर- रसायनों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। हमारी सभी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों द्वारा ही होता है। साबुन, अपमार्जक, वस्त्र, घरेलू उपयोग के अने कों सामान भी रासायनिक पदार्थ ही हैं। भवन निर्माण में प्रयुक्त सीमेन्ट, विद्युत उपकरण, उपग्रह, मोटर वाहन से लेकर कृषि के क्षेत्र में रसायनों तथा रसायन विज्ञान के सिद्धान्तों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न बीमारियों में प्रयुक्त औषधियाँ भी रसायन ही हैं। अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक आदि भी रसायनों का मिश्रण ही है। अतः यह कहा जा सकता है। कि रसायनों के बिना दैनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
प्रश्न 42. (a) तनु तथा सान्द्र अम्ल या क्षार क्या होते हैं?
(b) विभिन्न प्रकार के लवणों की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति बताइए।
उत्तर- (a) अम्ल और क्षार जल में विलेय होते हैं। जब इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तनु कहलाते हैं और जब जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है तो ये सान्द्र कहलाते हैं।
(b) प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। लेकिन प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय तथा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं।
प्रश्न 43.(i) अम्ल-क्षार की आरेनियस संकल्पना की कमियाँ बताइए।
(ii) संयु ग्मी अम्ल-क्षार युग्म किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर- (i) आरेनियस की संकल्पना उन अम्लों एवं क्षारों के लिए उपयुक्त है। जिनमें क्रमशः H+ व OH– आयन होते हैं परन्तु इससे हाइड्रोजन आयन विहीन अम्लों तथा हाइड्रॉक्सिल आयन विहीन क्षारों की प्रकृति का स्पष्टीकरण नहीं होता।
(ii) जब किसी अम्ल तथा क्षार के युग्म में एक प्रोटॉन का अन्तर होता है, तो इसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं, जैसे
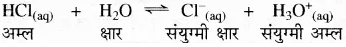
प्रश्न 44. कुछ प्रमुख विलयनों की pH परास बताइए।
उत्तर- प्रमुख विलयनों की pH परास निम्न प्रकार है
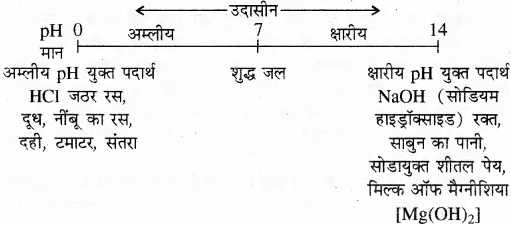
प्रश्न 45. प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण बताइए।
उत्तर- प्लास्टर ऑफ पेरिस श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। इसमें जल मिलाने पर यह 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस तथा कठोर हो जाता है। इस अभिक्रिया में जिप्सम बनता है।
2CaSO4.½H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस + 3H2O → 2CaSO4 जिप्सम .2H2O
प्रश्न 1. अम्ल व क्षार की आरेनियस संकल्पना को विस्तार से समझाइए।
उत्तर- आरेनियस (1887) के अनुसार जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ अम्ल तथा हाइड्रॉक्सिल आयन देने वाले पदार्थ क्षार कहलाते हैं।
अम्ले के उदाहरण–
HCl(aq) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल → H+(aq) +Cl–(aq)
CH3COOH(aq) एसीटिक अम्ल → CH3COO–(aq) + H+(aq)
HNO3(aq) नाइट्रिक अम्ल → H+(aq) + NO3–(aq)
यहाँ प्राप्त प्रोटॉन (H+) अत्यधिक क्रियाशील होता है अतः यह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। |
H+ +H2O →H3O+(aq)
वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं जैसे-HCl, H2SO4, HNO3, इत्यादि जबकि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते तथा कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में भी रहते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं जैसे-CH3COOH, H2CO3, इत्यादि।
क्षार के उदाहरण-
NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड → Na+(aq) + OH– (aq)
NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड → NH4+ (aq) + OH– (aq)
अम्लों के समान वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है. उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं, जैसे-NaOH, KOH इत्यादि तथा वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनने नहीं होता, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, जैसे– NH4OH, Mg(OH)2 इत्यादि।
वे अम्ल जिनमें H+ नहीं होता तथा वे क्षार जिनमें OH- नहीं होता, उनका स्पष्टीकरण आरेनियस की धारणा से नहीं होता है।
प्रश्न 2. सोडियम क्लोराइड के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए।
उत्तर- बनाने की विधि-सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। यह प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण है अतः इसके विलयन की pH 7
होती है, अर्थात् यह उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड व्यापारिक तौर पर समुद्र के जले या खारे पानी को सुखा कर बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त नमक में कई अशुद्धियाँ जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड (MgCl2), कैल्शियम क्लोराइड (CaCl2) होती हैं। अतः इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी-बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस (HCl) प्रवाहित की जाती है, जिससे शुद्ध नमक (NaCl) अवक्षेपित हो जाता है, जिसे एकत्रित कर लिया जाता है।
NaCl के गुण-
- यह श्वेत ठोस पदार्थ है।
- इसका गलनांक उच्च (1081 K) होता है।
- NaCl जल में अत्यधिक विलेय होता है।
- जलीय विलयन में यह आयनित होकर Na+ तथा Cl- देता है।
उपयोग-
- NaCl का उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है।
- इसका खाद्य परिरक्षण में भी प्रयोग किया जाता है।
- इससे हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है।
- NaOH, Na2CO3, NaHCO3 तथा विरंजक चूर्ण बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में भी NaCl को प्रयुक्त किया जाता है।
प्रश्न 3. दैनिक जीवन में विभिन्न अम्लों, क्षारों तथा लवणों के उपयोगों पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर- दैनिक जीवन में अम्लों, क्षारों तथा लवणों का उपयोग बहुत व्यापक है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है|
(a) अम्लों के उपयोग
- H2SO4, HCl तथा HNO3 को खनिज अम्ल कहा जाता है, जबकि पौधों तथा जन्तुओं में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे-सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। खनिज अम्ल विभिन्न उद्योग-धन्धों जैसे औषधि, पेन्ट तथा उर्वरक आदि में प्रयुक्त होते हैं।
- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक उद्योगों में, बॉयलर को साफ करने में, सिंक तथा सेनिटरी को साफ करने में विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है।
- नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने, चाँदी व सोने के गहनों को साफ करने में। काम आता है। एक भाग HNO3, तथा तीन भाग HCl को मिलाने पर अम्लराज (Aqua regia) बनता है जो कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मिश्रण है। अम्लराज सोने जैसे धातु को भी विलेय कर देता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल सेल, कार बैटरी तथा उद्योगों में काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा (King of acids) भी कहा जाता है।
- कार्बनिक अम्ल जैसे एसीटिक अम्ल सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों तथा अचार आदि को संरक्षित करने में एवं लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आता है।
(b) क्षारों के उपयोग
- विभिन्न क्षारों का भी उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से होता है। साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग तथा वस्त्र उद्योगों में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग होता है।
- कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। Ca(OH)2; सफेदी अर्थात् चूना तथा कीटनाशक का एक घटक भी है।
- मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड [Mg(OH)2] को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह एन्टएसिड के रूप में पेट की अम्लता और कब्ज दूर करने में उपयोग में लिया जाता है।
(c) लवणों के उपयोग
- दैनिक जीवन में लवणों के भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं-कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO3) को संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, धातुकर्म में लोहे के निष्कर्षण में तथा सीमेन्ट बनाने में उपयोग में लिया जाता है।
- सिल्वर नाइट्रेट (AgNO3) को फोटोग्राफी में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक व विस्फोटक बनाने में तथा फिटकरी (K2SO4. Al2 (SO4)3. 24H2O) को जल के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है।
प्रश्न 4. साबुन एवं अपमार्जक क्या होते हैं तथा इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है?
उत्तर- अपमार्जक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है स्वच्छ करने वाला। इसमें साबुन तथा अपमार्जकों को लिया जाता है।
साबुन (Soap)-साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। ये दीर्घ श्रृंखलायुक्त (12 से 18 कार्बन परमाणु) वसा अम्लों जैसे स्टियरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल तथा
ओलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटैशियम लवण होते हैं। इन्हें वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
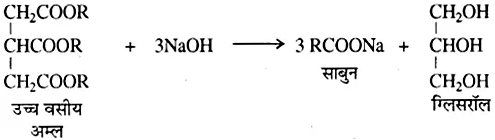
प्राप्त विलयन में NaCl मिलाने पर साबुन अवक्षेपित हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटैशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलेय होते हैं। पोटैशियम साबुन सोडियम साबुन से अधिक मृदु होते हैं, अतः इन्हें शेविंग साबुन तथा शैम्पू आदि बनाने में काम लेते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है।
अपमार्जक (Detergent)-अपमार्जक साबुन के समान ही होते हैं परन्तु ये कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कार्य करते हैं। अतः अपमार्जकों को सफाई के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है।
अपमार्जक दीर्घ श्रृंखलायुक्त सोडियम एल्किल सल्फेट R−O−SO3⊖Na⊕ तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट R−C6H4−SO3⊖Na⊕ होते हैं।
संश्लेषित अपमार्जकों के द्वारा जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा इनको आसानी से विघटन नहीं हो पाता है।
यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला (R समूह) कम शाखित हो तो इनका जीवाणुओं द्वारा विघटन या निम्नीकरण आसानी से हो जाता है। अतः लंबी तथा कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। आजकल अपमार्जकों की क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी मिलाये जाते हैं। साबुन एवं अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया मिसेल बनाकर की जाती है।
प्रश्न 5. अम्लों एवं क्षारों के सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर- अम्लों एवं क्षारों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं
(i) अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
(ii) अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं।
Zn धातु (जिंक) + H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल → ZnSO4 + H2 ↑
इसी कारण खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है।
Zn धातु की NaOH (क्षार) के साथ अभिक्रिया से भी लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है।
Zn + 2NaOH — Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट + H2 ↑
परन्तु सभी धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया में H2 गैस नहीं बनती है।
(iii) अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं।
धातु ऑक्साइड + अम्ल → लवण + जल ।
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
अतः ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं अतः ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं।
अधातु ऑक्साइड + क्षार → लवण + जल
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
(iv) सभी अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अतः इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में भी किया जाता है।
(v) सभी अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके अपने गुण को खोकर उदासीन हो जाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है।
अम्ल + क्षार → लवण + जल
HCl + NaOH → NaCl + H2O
We hope the given Solutions for Class 10 Science Chapter 5 दैनिक जीवन में रसायन will help you. If you have any query regarding Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 5 दैनिक जीवन में रसायन, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
कक्षा 10 का दोहरान करने के लिए नीचे विज्ञान पर क्लिक करें
विज्ञान SCIENCE REVISION
CLCIK HERE FOR FREE MOCK TEST
CLICK HERE FOR ALL CLASS STUDY MATERIAL 2021
JOIN TELEGRAM
SUBSCRIBE US SHALA SUGAM
SUBSCRIBE US SHIKSHA SUGAM
SOME USEFUL POST FOR YOU
⇓ ⇓ ⇓
![SMILE 3 CLASS 8]()
by Sheetal Panwar | Apr 12, 2021 | CLASS 10, E CONTENT, REET, STUDENT CORNER |
RBSE BSER CLASS X SCIENCE LESSON 4 IMMUNITY AND BLOOD GROUPS
K. L. SEN MERTA
(M.Sc. M.A. B.Ed.)
SCIENCE EDUCATOR,
These Solutions for Class 10 Science Chapter 4 प्रतिरक्षा एवं रक्तसमूह are part of Solutions for Class 10 Science. Here we have given Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 4 प्रतिरक्षा एवं रक्तसमूह .
| Board |
RBSE |
| Textbook |
SIERT, Rajasthan |
| Class |
Class 10 |
| Subject |
Science |
| Chapter |
Chapter 4 |
| Chapter Name |
प्रतिरक्षा एवं रक्तसमूह . |
| Number of Questions Solved |
74 |
| Category |
RBSE CLASS X |
आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न
1. प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं…………..में नहीं पाई जाती हैं।
(क) अस्थिमज्जा
(ख) यकृत
(ग) आमाशय
(घ) लसीका पर्व
2. प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है?
(क) बी लसीका कोशिका
(ख) टी लसीका कोशिका
(ग) न्यूट्रोफिल
(घ) क व ग दोनों
3. एण्टीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं ?
(क) प्रतिजन
(ख) IgG प्रतिरक्षी
(ग) IgM प्रतिरक्षी
(घ) प्लाविका कोशिका
4. प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है
(क) IgG
(ख) IgM
(ग) IgD
(घ) IgE
5. माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी कौनसी है?
(क) IgG
(ख) IgM
(ग) IgD
(घ) IgA
6. रक्त में निम्न में से कौनसी कोशिकाएं नहीं पाई जातीं ?
(क) लाल रक्त कोशिकाएं
(ख) श्वेत रक्त कोशिकाएं
(ग) बी लसीका कोशिकाएं
(घ) उपकला कोशिकाएं
7. रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया?
(क) लुइस पाश्चर
(ख) कार्ल लैण्डस्टीनर
(ग) रार्बट कोच
(घ) एडवर्ड जेनर
8. सर्वदाता रक्त समूह है
(क) A
(ख) AB
(ग) O
(घ) B
9. गर्भ रक्ताणुकोरकता (Erythroblastosis fetalis) का प्रमुख कारण है
(क) शिशु में रक्ताधान
(ख) आर एच बेजोड़ता।
(ग) ए बी ओ बेजोड़ता
(घ) क व ग दोनों
10. समजीवी आधान में किसका उपयोग होता है?
(क) व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का
(ख) अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का
(ग) भेड़ के संग्रहित रक्त का
(घ) क व ख दोनों
11. रक्ताधान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौनसा रोग नहीं होता है?
(क) हेपेटाइटिस बी
(ख) मलेरिया
(ग) रुधिर लवणता
(घ) क्रुएटज्फेल्डट जैकब रोग
12. निम्न में से कौनसा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है?
(क) A-रुधिर वर्ग
(ख) B-रुधिर वर्ग
(ग) O-रुधिर वर्ग
(घ) AB-रुधिर वर्ग
13. निम्न में से कौनसा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है?
(क) हीमोफीलिया का इलाज
(ख) मलेरिया का इलाज
(ग) डेंगू का इलाज
(घ) ख व ग दोनों
14. भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है?
(क) 13 सितम्बर
(ख) 13 अगस्त
(ग) 13 मई
(घ) 13 जून
15. भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या है (प्रति दस लाख में)
(क) 0.1
(ख) 2.0
(ग) 0.8
(घ) 1.8
1. (ग)
2. (क)
3. (क)
4. (ख)
5. (घ)
6. (घ)
7. (ख)
8. (ग)
9. (ख)
10. (क)
11. (ख)
12. (ग)
13. (घ)
14. (ख)
15. (ग)
प्रश्न 16. मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती हैं ?
उत्तर- मनुष्य में दो प्रकार की प्रतिरक्षी विधियाँ पाई जाती हैं
- स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि
- उपार्जित प्रतिरक्षा विधि।
प्रश्न 17. प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं ?
उत्तर- प्रतिरक्षी पाँच प्रकार के होते हैं।
प्रश्न 18. प्रतिजन का आण्विक भार कितना होना चाहिए?
उत्तर- प्रतिजन का आण्विक भार 6000 डाल्टन अथवा उससे ज्यादा होना चाहिए।
प्रश्न 19. प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं ?
उत्तर- प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन प्रकार की प्रोटीन है।
प्रश्न 20. कौनसा प्रतिरक्षी आवल को पार कर भ्रूण में पहुँच सकता है?
उत्तर- IgG प्रतिरक्षी आँवल को पार कर भ्रूण में पहुँच सकता है।
प्रश्न 21. मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखें।
उत्तर- मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम IgE है।
प्रश्न 22. रक्त में उपस्थित कौनसी कोशिका गैसों के विनिमय में संलग्न होती है?
उत्तर- रक्त में उपस्थित लाल रक्त कोशिका (RBC) गैसों के विनिमय में संलग्न होती है।
प्रश्न 23. रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया?
उत्तर- रक्त का वर्गीकरण वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया।
प्रश्न 24. सर्वदाता रक्त समूह कौनसी है?
उत्तर-‘O’ रक्त समूह वाले व्यक्ति सर्वदाता हैं।
प्रश्न 25. किस रक्त समूह में ‘A’ व ‘B’ दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं?
उत्तर- AB रक्त समूह में ‘A’ व ‘B’ दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं।
प्रश्न 26. विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त आरएच धनात्मक होता है?
उत्तर- विश्व के लगभग 85% व्यक्तियों का रक्त आरएच धनात्मक होता है।
प्रश्न 27. कौनसा आरएच कारक सबसे महत्त्वपूर्ण है?
उत्तर- Rh.D कारक सबसे महत्त्वपूर्ण है।
प्रश्न 28. प्रथम रक्ताधान किसके द्वारा संपादित किया गया?
उत्तर- प्रथम रक्ताधान डॉ. जीन बेप्टिस्ट डेनिस द्वारा सम्पादित किया गया।
प्रश्न 29. समजात आधान क्या है?
उत्तर- ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, उसे समजात आधान कहते हैं।
प्रश्न 30. रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम लिखें।
उत्तर- IA, IB तथा IO या i
प्रश्न 31. भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है?
उत्तर- भारत में हर वर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न 32. हाल ही में देहदान करने वाले दो व्यक्तियों के नाम लिखें।
उत्तर- (i) डॉ. विष्णु प्रभाकर
(ii) श्री ज्योति बसु
प्रश्न 33. प्रतिरक्षी को परिभाषित करें।
उत्तर- शरीर में एन्टीजन के प्रवेश होने पर इसे एन्टीजन के विरुद्ध शरीर की B लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ प्रतिरक्षी अथवा एन्टीबॉडी कहलाते हैं।प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन (संक्षिप्त में Ig) कहते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन (γ-globulin) प्रोटीन है जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं।
प्रश्न 34. एण्टीजनी निर्धारक क्या होते हैं?
उत्तर- प्रतिजन सम्पूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता वरन् इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। इन अंशों को एण्टीजनी निर्धारक (Antigenic determinant or epitope) कहा जाता है।प्रोटीन में करीब 6-8 ऐमीनो अम्लों की एक श्रृंखला एन्टीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एन्टीजनी निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को एन्टीजन की संयोजकता कहा जाता है। अधिकतर जीवाणुओं में एन्टीजनी संयोजकता सौ या अधिक होती है।
प्रश्न 35. प्रतिरक्षी में हिन्ज का क्या कार्य है?
उत्तर- अधिकांश प्रतिरक्षियों के Y स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं जिन्हें कब्जे अथवा हिन्ज कहते हैं। लचीले होने के कारण हिन्ज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे-बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में सहायता करता है।
प्रश्न 36. रक्त क्या है?
उत्तर- रक्त एक परिसंचारी (circulating) तरल ऊतक है जो रक्तवाहिनियों एवं हृदय में होकर पूर्ण शरीर में निरन्तर परिक्रमा करके पदार्थों का स्थानान्तरण करता रहता है। रक्त क्षारीय माध्यम का होता है तथा इसका pH 7.4 होता है। मनुष्य में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है।रक्त प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं जो निर्जीव होता है। प्लाज्मा आँतों से शोषित पोषक तत्त्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में तीन प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं(अ) लाल रक्त कणिकाएँ (Red Blood Corpuscles)- ये कणिकाएँ गैसों के परिवहन एवं गैस विनिमय का कार्य करती हैं।
(ब) श्वेत रक्त कणिकाएँ (White Blood Corpuscles)- श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती हैं।
(स) बिम्बाणु (Platelets)- ये कणिकाएँ रक्त वाहिनियों की सुरक्षा एवं रक्तस्राव रोकने में मदद करती हैं।
प्रश्न 37. A B O रक्त समूहीकरण को समझाइए।
उत्तर- RBC की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन (Antigen) पाये जाते हैं, जिन्हें प्रतिजन ‘A’ व प्रतिजन ‘B’ कहते हैं। इन प्रतिजनों (Antigens) की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः A, B, AB तथा O समूह कहते हैं। इस वर्गीकरण को A B O समूहीकरण कहते हैं।
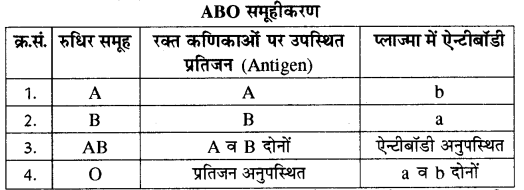 A रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर A प्रतिजन तथा B रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर B प्रतिजन पाया जाता है। AB प्रकार के रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर A व B दोनों प्रकार के प्रतिजन पाये जाते हैं। जबकि O रुधिर समूह की RBC पर कोई किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है अर्थात् A तथा B प्रतिजनों का अभाव होता है। देखिए ऊपर तालिका में।
A रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर A प्रतिजन तथा B रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर B प्रतिजन पाया जाता है। AB प्रकार के रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर A व B दोनों प्रकार के प्रतिजन पाये जाते हैं। जबकि O रुधिर समूह की RBC पर कोई किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है अर्थात् A तथा B प्रतिजनों का अभाव होता है। देखिए ऊपर तालिका में।
प्रश्न 38. आर एच कारक क्या है? इसके महत्त्व को समझाइए।
उत्तर- आर एच कारक-लैण्डस्टीनर तथा वीनर ने मकाका रीसस (Macaca rhesus) बंदर की RBC में एक अन्य प्रकार के कारक का पता लगाया था। इसे Rh कारक का नाम दिया गया। (Rh) संकेत का प्रयोग रेसिस शब्द को दर्शाने के लिए किया गया है। जिन व्यक्तियों में यह कारक पाया जाता है, उन्हें Rh धनात्मक (Rh+) और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें Rh ऋणात्मक (Rh-) कहते हैं। विश्व में 85 प्रतिशत जनसमुदाय Rh+ जबकि शेष 15 प्रतिशत Rh- हैं।आर एच कारक का महत्त्व- Rh- व्यक्ति में Rh एन्टीजन का अभाव होता है, लेकिन इसके रुधिर में Rh एन्टीजन प्रवेश करवा दिये जाने पर इससे कारक के प्रतिरोध में एण्टीबॉडी बनना प्रारम्भ हो जाती है जो रुधिर समूहन (agglutination) क्रिया का कारण बनते हैं। Rh कारक के कारण कई बार जन्म के समय बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। रुधिर समूहने के कारण भ्रूण की RBCs में हीमोलाइसिस द्वारा क्षति होती है। इसके फलस्वरूप एरिथ्रॉब्लास्टोसिस फीटेलिस नामक रोग हो जाता है। इसके कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है।
प्रश्न 39. रक्ताधान क्या है? समझाइए।
उत्तर- रक्ताधान वह विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानान्तरित किया जाता है। सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक डॉ. जीन बेप्टिस्ट डेनिस द्वारा 15 जून, 1667 में रक्ताधान सम्पादित किया। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्ताधान करवाया था।लेकिन इसके दस वर्ष बाद पशुओं से मानव में रक्ताधान पर रोक लगा दी गई। निम्न परिस्थितियों में रक्ताधान किया जा सकता है
- दुर्घटना के तहत लगी चोट तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने पर।
- शरीर में गम्भीर रक्तहीनता होने पर।
- रक्त में बिम्बाणु (Platelets) अल्पता की स्थिति में।
- हीमोफीलिया के रोगियों को।
- शल्यक्रिया के दौरान ।
- दात्र कोशिका अरक्तता (Sickle Cell anemia) के रोगियों को।
रक्तदान से व्यक्तियों/रोगियों को नया जीवनदान दिया जाता है। अतः रक्तदान हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है।
प्रश्न 40. रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ लिखें।
उत्तर- रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित हैं
- रोगी व रक्त देने वाले व्यक्ति अर्थात् दाता के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान करना चाहिए।
- दाता के रक्त में कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है, इसके लिए जाँच की जानी चाहिए।
- दोनों के रक्त में Rh कारक का मिलान करना चाहिए विशेष रूप से RhD का।।
- संग्रहित रक्त की वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रशीतित भण्डारण करना।
- किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाये रखना।
- संग्रहण व आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो।
प्रश्न 41. अंगदाने की आवश्यकता समझाइए।
उत्तर- अंगदान-किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंगदान करना अंगदान (Organ donation) कहलाता है। दाता द्वारा दिया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। अंगदान द्वारा दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि उसके जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। एक मृत देह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है।भारत में हर वर्ष करीब दो लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है जबकि मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 7000 से 8000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं परन्तु उपलब्धता केवल 10 से 15 की ही है। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में 50,000 यकृत की आवश्यकता है परन्तु केवल 700 व्यक्तियों को ही यह मौका प्राप्त हो पाता है। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब पाँच लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण ना हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।अतः अंगदान एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
प्रश्न 42. A B O रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूपों को समझाइए।
उत्तर- मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाये जाते हैं, जिन्हें A B O रुधिर तंत्र के नाम से सम्बोधित किया जाता है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण तीन विकल्पियों (alleles) के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं तथा IA, IB तथा IO या i के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। RBC की कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A (Antigen A) तथा प्रतिजन B (Antigen B) का निर्माण क्रमशः विकल्पी IA तथा IB द्वारा किया जाता है। विकल्पी I तथा i अप्रभावी होते हैं तथा किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं ।
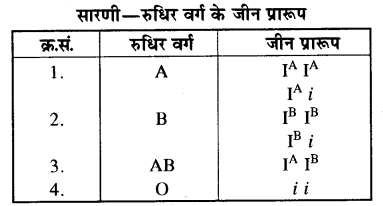 किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त वर्ग किन्हीं दो विकल्पियों के बीच की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। मनुष्यों में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल छः प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। देखिए ऊपर सारणी में।
किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त वर्ग किन्हीं दो विकल्पियों के बीच की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। मनुष्यों में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल छः प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। देखिए ऊपर सारणी में।
प्रश्न 43. प्रतिरक्षियों की संरचना को समझाइए।
उत्तर- प्रतिरक्षी की संरचना-यह जटिल ग्लाइको प्रोटीन से मिलकर बना अणु होता है, जिसमें चार पालीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ दो भारी व बड़ी (440 अमीनो अम्ल) तथा दो हल्की व छोटी श्रृंखला (220 अमीनो अम्ल) आपस में डीसल्फाइड बंध द्वारा मुड़कर Y आकृति बनाती है। देखिए आगे चित्र में प्रतिरक्षी को प्रदर्शित किया जाता है।भारी पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है। प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है|
(1) अस्थिर भाग
(2) स्थिर भाग।
- अस्थिर भाग (Variable portion)- यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला के NH2 भाग की तरफ पाया जाता है। इसे Fab भी कहते हैं।
- स्थिर भाग (Constant portion)- यह भाग श्रृंखला के COOH भाग की तरफ होता है तथा Fc भाग कहलाता है। प्रतिरक्षी के पुच्छीय भाग (Tail portion) को स्थिर भाग कहते हैं।
अधिकतर प्रतिरक्षियों के Y स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं जो कब्जे अथवा हिन्ज (Hinge) कहलाते हैं । लचीले होने के कारण हिन्जप्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे-बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में मदद करते हैं।
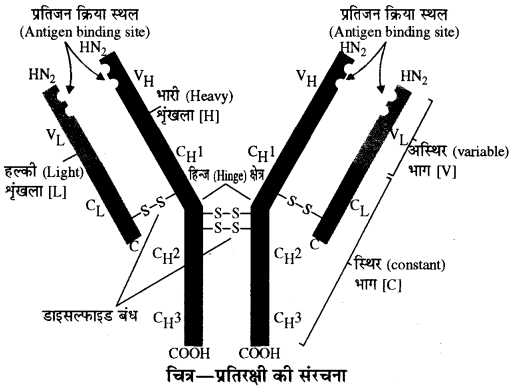
हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एन्टीबॉडी उत्पन्न किये जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं- IgA, IgM, IgE एवं IgG।
प्रश्न 44. गर्भ रक्ताणुकोरकता को समझाइए।
उत्तर-
यदि Rh- माता एक से अधिक बार Rh+ शिशु से युक्त गर्भधारण करती है तो Rh कारक के कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। Rh कारक वंशागत होता है। Rh+ प्रभावी तथा Rh- अप्रभावी होता है। Rh- माता से उत्पन्न Rh+ शिशु पिता से Rh कारक प्राप्त करता है। प्रसव के समय गर्भस्थ Rh+ शिशु से Rh प्रतिजन माता के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। माता के रक्त में इस प्रतिजन (Antigen) के कारण एन्टी Rh प्रतिरक्षी (Antibody) उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जो प्रथम बार उत्पन्न शिशु को हानि पहुँचा सके, लेकिन बाद में गर्भधारण की स्थिति में माता के रक्त से एन्टी Rh प्रतिरक्षी अपरा (Placenta) द्वारा गर्भस्थ शिशु के रक्त में पहुँचकर शिशु के रक्त कणिकाओं का लयन (Haemolysis) कर देती है।गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु के इस घातक रोग को रक्ताणुकोरकता (Erythroblastosis) कहते हैं। इस रोग से ग्रसित शिशु को रीसस शिशु (Rhesus baby) कहते हैं। सामान्यतः इसका जन्म समय पूर्व होता है तथा इसमें रक्ताल्पता पाई जाती है। शिशु के सम्पूर्ण रक्त को स्वस्थ रुधिर द्वारा प्रतिस्थापित करके शिशु को बचाया जा सकता है।
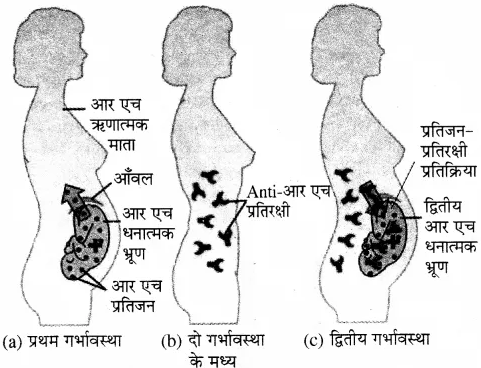 चित्र-गर्भ रक्ताणुकोरकता (Erythroblastosis fetalis)
प्रथम प्रसव के 24 घण्टों के भीतर माता को प्रति IgG प्रतिरक्षियों (anti RhD) का टीका लगाकर इसका उपचार किया जाता है। इन्हें रोहगम (Rhogam) प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकती है।
चित्र-गर्भ रक्ताणुकोरकता (Erythroblastosis fetalis)
प्रथम प्रसव के 24 घण्टों के भीतर माता को प्रति IgG प्रतिरक्षियों (anti RhD) का टीका लगाकर इसका उपचार किया जाता है। इन्हें रोहगम (Rhogam) प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकती है।
प्रश्न 45. रक्ताधान की प्रक्रिया कैसे संपादित की जाती है?
उत्तर-
रक्ताधान की प्रक्रिया (Process of Blood Transfusion)रक्ताधान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाती है
1. रक्त संग्रहण (Blood Collection)-
- रक्त के संग्रहण से पहले रक्त देने वाले अर्थात् दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है।
- तत्पश्चात् उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी (Cannula) के माध्यम से निर्जर्मीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियों में दाता का रक्त संग्रहित किया जाता है।
- अब संग्रहित रक्त का प्रशीतित भण्डारण किया जाता है, जिससे रक्त में जीवाणुओं की वृद्धि एवं कोशिकीय चपापचय को धीमा करते हैं।
- इस संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जाँचें की जाती हैं, जैसे
(अ) रक्त समूह
(ब) आर एच कारक
(स) हिपेटाइटिस बी
(द) हिपेटाइटिस सी
(य) एचआईवी
- दाता से रक्त लेने के पश्चात् दाता को कुछ समय के लिए चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। मानव में रक्तदान के पश्चात् प्लाज्मा की दोतीन दिन में पुनः पूर्ति हो जाती है एवं औसतन 36 दिनों के पश्चात् रक्त कोशिकाएँ परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती हैं।
2. आधान (Transfusion)-
- किसी व्यक्ति (मरीज) के रुधिर चढ़ाने (आधान) से पहले दाता व मरीज के रक्त का मिलान (ABO, Rh आदि) किया जाता है।
- आधान से पूर्व संग्रहित रक्त को 30 मिनट पूर्व ही भण्डारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है।
- रक्त प्रवेशनी (cannula) के माध्यम से मरीज को अंतःशिरात्मक रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग चार घण्टे लगते हैं।
- रक्त चढ़ाने (आधान) के दौरान मरीज को ज्वर, ठण्ड लगना, दर्द साइनोसिस (Cyanosis), हृदय गति में अनियमितता को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधियाँ दी जाती हैं।
रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान दो प्रकार का होता है
(1) समजाते आधान (Allogenic transfusion)- इस प्रकार के आधान में अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है।
(2) समजीवी आधान (Autogenic transfusion)- इस प्रकार के आधान में व्यक्ति के स्वयं का संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है।दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक्-पृथक् भी किया जा सकता है। प्रसंस्करण के बाद रक्त को RBC, प्लाज्मा तथा बिम्बाणु (platelets) में विभक्त कर प्रशीतित में भण्डारण किया जाता है।
प्रश्न 46. अंगदान क्या है? अंगदान का महत्त्व बताइए।
उत्तर-
अंगदान-जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग दान करना अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को ना केवल बचाया जा सकता है वरन् खुशहाल भी बनाया जाता है। अधिकांश अंगदान दाता की मृत्यु के पश्चात् ही होते हैं।एक मृत देह से करीब पचास जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। अतः अंगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बच्चों से लेकर नब्बे वर्ष तक के लोग भी। अंगदान व देहदान में सक्षम हैं।अंगदान का महत्त्व-‘पशु मरे मनुज के सौ काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम ना आवे।” अतः आवश्यकता है कि मानव मृत्यु (Death) के बाद प्राणिमात्र के काम आ सके। यह तभी सम्भव है जब मृत्यु उपरान्त भी हम दूसरे व्यक्तियों में जीवित रहें, हमारी आँखें, गुर्दे, यकृत, अग्न्याशय, हृदय, फेफड़े, अस्थिमज्जा, त्वचा आदि हमारी मृत्यु के पश्चात् भी किसी जरूरतमंद के जीवन में सुख ला पायें तो इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है।भारत में हर वर्ष करीब पाँच लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण ना हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अंगदान की भाँति देहदान भी समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसके दो कारण हैं–पहला, मृत देह से अंग निकालकर रोगी व्यक्तियों के शरीर में प्रत्यारोपित किये जा सकते हैं। दूसरा, चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र, मृत देह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बन सकें।हम अंगदान व देहदान के महत्त्व को समझें और उन लोगों की मदद करें जिनका जीवन किसी अंग के अभाव में बड़ा कष्टप्रद है। हमें इस नेक कार्य के लिए आगे आकर समाज को इस श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पवित्र कार्य हेतु शिक्षक, साधु-संत, बुद्धिजीवियों आदि की मदद से समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर कर अंगदान करने के लाभ लोगों तक पहुँचना अति आवश्यक है। इस प्रायोजन से भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है।समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस नेक काम के लिए आगे आये हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 90 वर्ष की उम्र में अपना कॉर्निया दान कर दो लोगों के जीवन में उजाला कर दिया। इसी प्रकार डॉ. विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु एवं श्री नाना देशमुख आदि की भी उनकी इच्छानुसार मृत्यु पश्चात् देह दाने कर दी गई।साध्वी ऋतम्भरा तथा क्रिकेटर गौतम गम्भीर ने भी मृत्यु के बाद देहदान करने की घोषणा की है। ऐसे मनुष्य सही मायनों में महात्मा हैं तथा ये ही विचार क्रान्ति के ध्वजक हैं। हम सभी को कर्तव्यबोध के साथ रक्तदान, अंगदान तथा देहदान के लिए संकल्पित होना चाहिए ताकि इस पुनीत कार्य से हमारे समाज में रह रहे हमारे साथी जिंदगी को जिंदगी की तरह जी सकें।
प्रश्न 47. रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्त्व की व्याख्या करें।
उत्तर-
रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्त्व-मानव में चार प्रकार के रुधिर वर्ग पाये जाते हैं, जिन्हें क्रमशः A, B, AB तथा O कहते हैं। मानव में रुधिर वर्ग वंशागते लक्षण है एवं जनकों से संततियों में मेण्डल के नियम के आधार पर वंशानुगत होते हैं। रुधिर वर्ग की वंशागति जनकों से प्राप्त होने वाले जीन्स/एलील पर निर्भर करती है। एलील्स जो मनुष्य में रुधिर वर्गों को नियंत्रित करती है, उनकी संख्या तीन होती है, जिन्हें क्रमशः IA, IB तथा IO या i कहते हैं । RBC की सतह पर पाई जाने वाली प्रतिजन का निर्माण एलील IA द्वारा, प्रतिजन B का निर्माण एलील IB द्वारा किया जाता है। एलील I तथा i अप्रभावी होते हैं जो किसी प्रतिजन के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं।इस प्रकार मानव में एलील की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के छः प्रकारे के जीन प्ररूप (Genotype) पाये जाते हैं।रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के कई उपयोग हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से पैतृकता सम्बन्धी विवादों को हल करने में, सफल रक्ताधान कराने में, नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता तथा आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि में किया जाता है। पैतृकता सम्बन्धी विवादों के हल में रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के ज्ञान को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता हैजैसे कि एक शिशु जिस पर दो दंपती अपना हक जता रहे हैं, का रुधिर वर्ग B है। एक दंपती में पुरुष का रुधिर वर्ग O(ii) है तथा स्त्री का रुधिर वर्ग AB(IAIB) है। दूसरे दंपती में पुरुष A(IAIA) तथा स्त्री B(IB i) रुधिर वर्ग की है। वंशागति के नियमानुसार शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न सम्भावनाएँ हैं
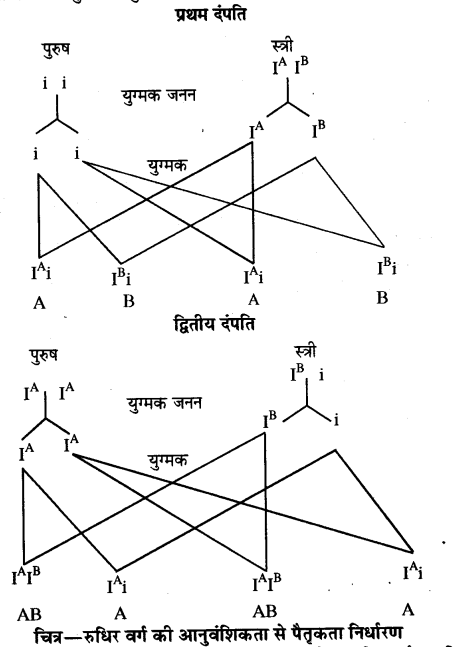 उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रथम दंपति ही B रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकता है।अतः हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्त्व है।
उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रथम दंपति ही B रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकता है।अतः हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्त्व है।
(अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर)
1. प्रतिरक्षी का आकार होता है
(अ) Z
(ब) H
(स) Y
(द) V
2. प्रतिरक्षी कितनी इकाइयों से मिलकर बनी होती है?
(अ) एक
(ब) दो
(स) तीन
(द) चार
3. निम्न में से प्रतिजन हो सकता है–
(अ) प्रोटीन
(ब) ग्लाइकोप्रोटीन
(स) कार्बोहाइड्रेट
(द) उपरोक्त सभी
4. मानव में कितने प्रकार के आर एच कारक पाये जाते हैं ?
(अ) दो
(ब) तीन
(स) चार
(द) पाँच
5. बिलीरुबिन की अधिकता निम्न में से किस अंग को हानि पहुँचाता है
(अ) जिगर (Liver)
(ब) तिल्ली
(स) गुर्दै
(द) उपरोक्त सभी
6. आर एच कारक कितने अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है ?
(अ) 417
(ब) 317
(स) 217
(द) 117
7. एक निष्प्राण देह से कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है?
(अ) करीब 30.
(ब) करीब 40
(स) करीब 50
(द) करीब 60
8. पुरातन काल में ऋषि दधीचि ने समाज की भलाई हेतु किसका दान किया?
(अ) अपनी हड्डियों का
(ब) अपने धन का
(स) अपने घर का
(द) अपने बच्चों का
9. प्रतिरक्षात्मक अंग है
(अ) अस्थिमज्जा
(ब) थाइमस
(स) यकृत
(द) उपरोक्त सभी
10. निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है
(अ) टिटेनस के टीके
(ब) त्वचा
(स) आमाशय
(द) आंत्र
11. कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपने शरीर का कौनसा अंग दान किया?
(अ) आमाशय
(ब) हड्डियों का
(स) कॉर्निया
(द) हृदय का
1. (स)
2. (द)
3. (द)
4. (द)
5. (द)
6. (अ)
7. (स)
8. (अ)
9. (द)
10. (अ)
11. (स)
प्रश्न 1. मां के दूध में पाये जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। (माध्य. शिक्षा बोर्ड, 2018)
उत्तर-
मां के दूध में पाये जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम IgA है।
प्रश्न 2. गर्भ रक्ताणुकोरकता रोग के उपचार में कौनसे टीके का उपयोग किया जाता है? (माध्य. शिक्षा बोर्ड, 2018)
उत्तर-
गर्भ रक्ताणुकोरकता रोग के उपचार में IgG प्रतिरक्षियों (anti RhD) के टीके का उपयोग किया जाता है। इन्हें रोहगम (Rhogam) प्रतिरक्षी कहा जाता है।
प्रश्न 3. Rh कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई? (माध्य. शिक्षा बोर्ड, मॉडल पेपर, 2017-18 )
उत्तर-
Rh कारक की खोज मकाका रीसस (Macaca rhesus) प्रजाति के बन्दर में हुई।
प्रश्न 4. डिप्थीरिया व टिटेनस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण (माध्य. शिक्षा बोर्ड, मॉडल पेपर, 2017-18)
उत्तर- ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं।
प्रश्न 5. किसी मनुष्य के रुधिर का जीन प्रारूप ii है तो उसका रुधिर वर्ग लिखिए। (माध्य. शिक्षा बोर्ड, मॉडल पेपर, 2017-18 )
उत्तर- ऐसे मनुष्य का रुधिर वर्ग O होगा।
प्रश्न 6. प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं ?
उत्तर- रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा सम्बन्धित तंत्र में अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं।
प्रश्न 7. मानव का शरीर आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। क्यों?
उत्तर- मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है।
प्रश्न 8. IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से किन कोशिकाओं पर क्रिया करती है?
उत्तर- IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है तथा एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है।
प्रश्न 9. किसी दो भौतिक अवरोधों के नाम लिखिए।
उत्तर-
- त्वचा
- नासिका छिद्रों में पाये जाने वाले पक्ष्माभ।
प्रश्न 10. अधिकांश जीवाणुओं में एण्टीजनी संयोजकतो की संख्या कितनी होती है?
उत्तर- अधिकांश जीवाणुओं में एण्टीजनी संयोजकता 100 या अधिक होती है।
प्रश्न 11. प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, वह क्या कहलाता है?
उत्तर-
प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, वह पैराटोप (Paratope) कहलाता है।
प्रश्न 12. कब्जे या हिन्ज (Hinge) किसे कहते हैं ?
उत्तर-
प्रतिरक्षियों के Y स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल कब्जे या हिन्ज कहलाते हैं।
प्रश्न 13. वह कौनसा अकेला प्रतिरक्षी है जो माँ के दूध में पाया जाता है?
उत्तर-
IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है।
प्रश्न 14. प्लाज्मा का कोई एक कार्य लिखिए।
उत्तर-
प्लाज्मा आँतों से शोषित पोषक तत्त्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है।
प्रश्न 15. कई बार रक्ताधान के पश्चात् होने वाले रुधिर लयणता का प्रमुख कारण क्या होता है?
उत्तर-
इसका प्रमुख कारण आर एच बेजोड़ता (Rh incompatibility) होता है।
प्रश्न 16. रक्त के स्रोत के आधार पर रक्ताधान कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए।
उत्तर-
रक्ताधान दो प्रकार का होता है
प्रश्न 17. जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना क्या कहलाता है?
उत्तर-
यह अंगदान कहलाता है।
प्रश्न 18. सर्वग्राही रक्त समूह कौनसा है ?
उत्तर-
सर्वग्राही रक्त समूह AB है।
प्रश्न 19. लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रतिजन पाये जाते हैं ?
उत्तर-
लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन (प्रतिजन ‘A’ व प्रतिजन ‘B’) पाये जाते हैं।
प्रश्न 20. प्लाज्मा का कार्य लिखिए।
उत्तर-
प्लाज्मार आँतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है।
प्रश्न 21. सफल रक्ताधान तथा आनुवांशिक रोगों से निदान हेतु किसकी आनुवांशिकता का ज्ञान परम आवश्यक है?
उत्तर-
सफल रक्ताधान तथा आनुवांशिक रोगों से निदान हेतु रुधिर वर्गों की आनुवांशिकता का ज्ञान परम आवश्यक है।
प्रश्न 22. मृत्यु के कितने घण्टों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है?
उत्तर-
मृत्यु के 6 से 8 घण्टों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है।
प्रश्न 1. प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के चरण लिखिए।
उत्तर-
प्रतिरक्षा विज्ञान-रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा सम्बन्धित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं।विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन के विनाश की कार्यविधि के चरण
- अन्तर्निहित प्रतिजन तथा बाह्य प्रतिजन में विभेद करना।
- बाह्य प्रतिजन के ऊपर व्याप्त एण्टीजनी निर्धारकों की संरचना के अनुसार बी-लसिका कोशिकाओं द्वारा प्लाविक कोशिकाओं का निर्माण।
- प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण।
- प्रतिजन-प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया तथा कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजन का विनाश।
प्रश्न 2. स्वाभाविक प्रतिरक्षा व उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए।
उत्तर-
स्वाभाविक प्रतिरक्षा व उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद
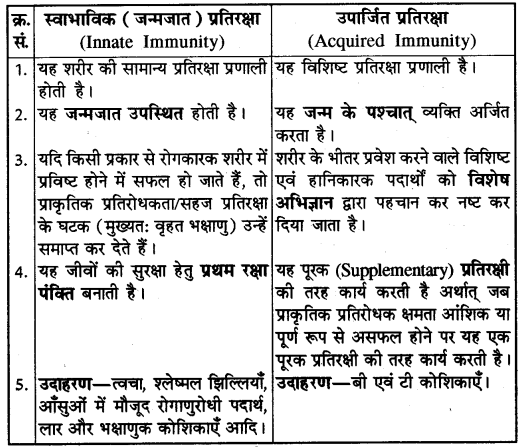
प्रश्न 3. निम्न को परिभाषित कीजिए
- प्रतिरक्षा
- एन्टीजन
- एन्टीबॉडी
- प्रतिरक्षा तंत्र।
उत्तर-
- प्रतिरक्षा (Immunity)-शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है।
- एन्टीजन (Antigen)-शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं, विषाणुओं एवं विषैले पदार्थों को प्रतिजन (Antigen) कहते हैं। इनको सीधे अथवा विशेष प्रतिरक्षी पदार्थों, एन्टीबॉडीज के द्वारा नष्ट किया जाता है। एन्टीबॉडीज के उत्पादन को उद्दीप्त प्रेरित करने वाले रसायन एन्टीजन कहलाते हैं।
- एन्टीबॉडी (Antibody)-शरीर में एन्टीजन के प्रवेश होने पर इस एन्टीजन के विरुद्ध शरीर की B-लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइको प्रोटीन पदार्थ एन्टीबॉडी (Antibody) कहलाते हैं ।
- प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System)-शरीर का वह तन्त्र जो शरीर को बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तन्त्र कहलाता है।
प्रश्न 4. पैराटोप (Paratope) किसे कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
पैराटोप (Paralope)-प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, पैराटोप कहलाता है।
सक्रिय प्रतिरक्षा व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अन्तर
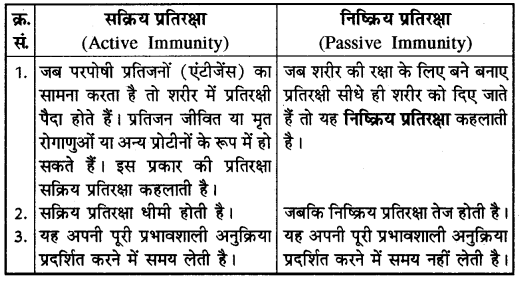
प्रश्न 5. सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा को समझाइए।
उत्तर-
जब परपोषी प्रतिजनों (एंटीजेंस) का सामना करता है तो शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन, जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा (एक्टिव इम्यूनिटी) कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है।प्रतिरक्षीकरण (इम्यूनाइजेशन) के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुँचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे हीशरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा (पैसव इम्यूनिटी) कहलाती है। दुग्धस्रवण (लैक्टेशन) के प्रारम्भिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष (कोलोस्ट्रम) में प्रतिरक्षियों (IgA) की प्रचुरता होती है तो शिशु की रक्षा करता है। सगर्भता (प्रेग्नेंसी) के दौरान भ्रूण को भी अपरा (प्लेसेंटा) द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कुछ उदाहरण हैं।
प्रश्न 6. प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? इनमें उपस्थित भारी श्रृंखला को यूनानी भाषा में किन अक्षरों से दर्शाया जाता है?
उत्तर-
प्रतिरक्षी पाँच प्रकार के होते हैं। इनमें उपस्थित भारी पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला को यूनानी भाषा के अक्षरों α (एल्फा), γ (गामा), δ (डेल्टा), ε (एपसीलन) तथा µ (म्यू) द्वारा दर्शाया जाता है, जो निम्न हैं
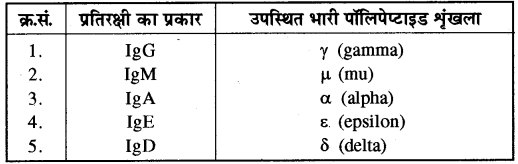
प्रश्न 7. रक्त क्या है? प्लाज्मा के कार्य लिखिए। इसमें पाई जाने वाली कणिकाओं का कार्य लिखें।
उत्तर-
रक्त (Blood)-रक्त एक तरल जीवित संयोजक ऊतक है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है। रक्त रक्त-वाहिनियों में बहता है। यह प्लाज्मा व रक्त-कणिकाओं से मिलकर बना होता है।
प्लाज्मा के कार्य
- प्लाज्मा आँतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है।
- विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है।
प्लाज्मा में तीन प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं
- लाल रक्त कणिकाएँ (RBC) -इनका कार्य गैसों का परिवहन तथा विनिमय है।
- श्वेत रक्त कणिकाएँ (WBC)- इनका कार्य शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना है।
- बिम्बाणु (Platelets)- इनका कार्य रक्त स्राव को रोकना अर्थात् रुधिर के थक्का बनने में सहायक एवं रक्त वाहिनियों की सुरक्षा करना।
प्रश्न 8. प्रतिरक्षी की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए।
उत्तर-
प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र
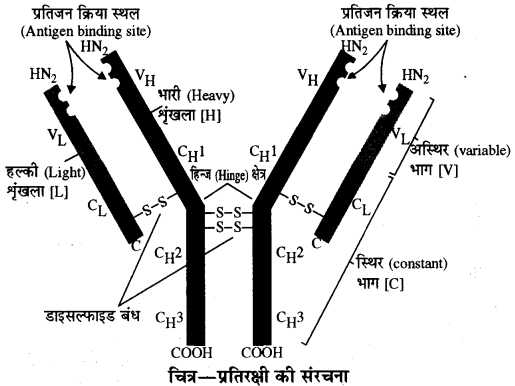
प्रश्न 9. एक दम्पती में पुरुष A तथा स्त्री B रुधिर वर्ग की है तो उनकी संतानों के रुधिर वर्ग की क्यो सम्भावना होगी?
उत्तर-
मेण्डल वंशागति के नियमानुसार पुरुष A तथा स्त्री B रुधिर वर्ग की है, तो संतान के रुधिर वर्ग की उपर्युक्त सम्भावनाएँ हैं।
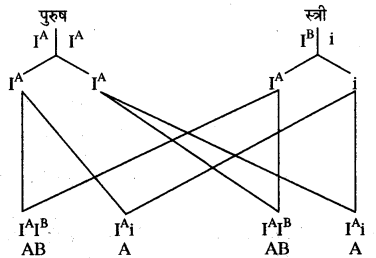
स्पष्ट है कि उनकी संतान AB रुधिर वर्ग या A रुधिर वर्ग की होगी ।प्रश्न 10.
आर एच कारक (Rh factor) क्या है? मानव में कितने प्रकार के आरं एच कारक पाये जाते हैं तथा इन कारकों की आवृत्ति बताइए।
उत्तर-
आर एच कारक-आर एच कारक करीब 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है जिसकी खोज मकाका रीसस नाम के बंदर में की गई थी। यह प्रोटीन मनुष्य की रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है।
मानव जाति में पाँच प्रकार के आर एच कारक पाये जाते हैं
- Rh.D.
- Rh.E
- Rh.e
- Rh.C
- Rh.c
मानव जाति में आर एच कारकों की आवृत्ति निम्नानुसार हैRh.D (85%), Rh.E (30%), Rh.e (78%), Rh.C (80%) तथा Rh.c (80%)। सभी Rh कारकों में Rh.D सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वाधिक (Immunogenic) है।
प्रश्न 11. अंगदान किसे कहते हैं? अंगदान व देहदान कौन कर सकता है? समझाइए।
उत्तर-
अंगदान (Organ Donation)-जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है।देहदान व अंगदान कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है तो कानूनी तौर पर उसके माता-पिता की या अभिभावक की सहमति लेना जरूरी है। अंगदान करने वाले व्यक्ति को दो गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति लेनी होगी। यदि मृत्यु पूर्व ऐसा नहीं किया गया है तो अंगदान व देहदान का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है, जिसके पास शव (Dead Body) का विधिवत आधिपत्य है।भारत में अंगदान व देहदान कानूनी रूप से मान्य है।
प्रश्न 12. प्रतिरक्षी संरचना के आधार पर अस्थिर भाग व स्थिर भाग में क्या अन्तर है?
उत्तर-
अस्थिर भाग व स्थिर भाग में अन्तरअस्थिर भाग
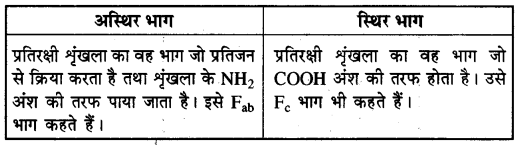
प्रश्न 13. रक्ताधान क्या है? रक्ताधान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण होने वाले रोगों के नाम लिखिए।
उत्तर-
रक्ताधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानान्तरित किया जाता है।
आधान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण निम्न रोग हो सकते हैं
- एच.आई.वी.-1 (HIV-1)
- एच.आई.वी.-2 (HIV-2)
- एच.टी.एल.वी.-1 (HTLV-1)
- एच.टी.एल.वी.-2 (HTLV-2)
- हैपेटाइटिस-बी (Hepatitis-B)
- हैपेटाइटिस-सी (Hepatitis-C)
- क्रुएटफेल्ड्ट्ट -जेकब रोग (Creutzfeldt-Jakob disease) आदि।
प्रश्न 14. प्रतिजन व प्रतिरक्षी में कोई चार अन्तर लिखिए।
उत्तर-
प्रतिजन व प्रतिरक्षी में अन्तर
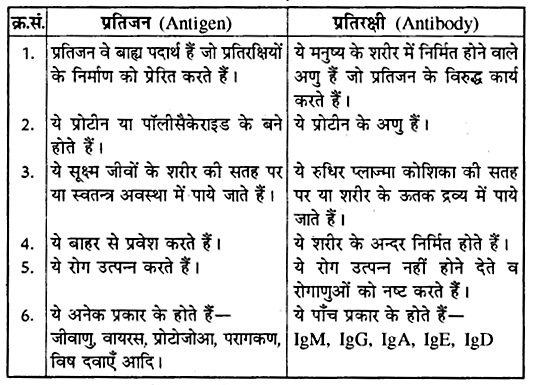
प्रश्न 15. किन परिस्थितियों में रक्ताधान की परम आवश्यकता होती है?
उत्तर-
निम्नांकित परिस्थितियों में रक्ताधान की परम आवश्यकता होती है
- चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर।
- शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर।
- शल्य चिकित्सा के दौरान।।
- रक्त में बिंबाणु (Platelets) अल्पता की स्थिति में।
- हीमोफीलिया (Hemophilia) के रोगियों को।
- दात्र कोशिका अरक्तता (Sickle cell anemia) के रोगियों को।
प्रश्न 16. भौतिक अवरोधक और रासायनिक अवरोधक में विभेद कीजिए।
उत्तर-
भौतिक अवरोधक व रासायनिक अवरोधक में विभेद
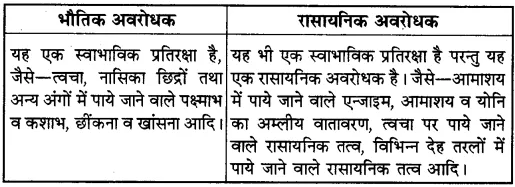
प्रश्न 1. व्युत्क्रम संकरण क्या है? जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी समयुग्मजी जनक से कराया जाता है, तो प्राप्त संतति में लक्षण-प्ररूप व जीनीप्ररूप अनुपात को समझाइए। (माध्य. शिक्षा बोर्ड, 2018)
उत्तर-
वह संकरण जिसमें ‘A’ पादप (TT) को नर व ‘B’ पादप (tt) को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरे संकरण में ‘A’ पादप (TT) को मादा व ‘B’ (tt) पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उसे व्युत्क्रम संकरण (Reciprocal Cross) कहते हैं।लक्षणप्ररूप (Phenotype) अनुपात-100% लम्बे
जीनीप्ररूप (Genotype) अनुपात–1 : 1, 50% TT : 50%Tt
प्रश्न 2. प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है एवं प्रत्येक का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
प्रतिरक्षा (Immunity)-शरीर में रोग या रोगाणुओं से लड़कर स्वयं को रोग से सुरक्षित बनाये रखने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो। प्रकार की होती है
- स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि
- उपार्जित प्रतिरक्षा विधि।
(1) स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि (Innate defense mechanism) –
यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही प्राप्त होती है अर्थात् यह माता-पिता से संतान में आती है। इसलिए इसे अविशिष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इस प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं और यदि प्रवेश कर भी जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाएँ इन्हें मृत कर देती हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा चार प्रकार के अवरोधकों से बनी होती है–
- भौतिक अवरोधक।
- रासायनिक अवरोधक
- कोशिका अवरोधक
- ज्वर, सूजन (Inflammation)
(i) भौतिक अवरोधक- हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। नासा मार्ग, नासिका छिद्रों तथा अन्य अंगों में पाये जाने वाले पक्ष्माभ (cilia) व कशाभ रोगाणुओं को रोकते हैं तथा इनमें उपस्थित श्लेष्मा ग्रन्थियाँ श्लेष्मा स्रावण करती हैं जो रोगाणुओं को अपने ऊपर चिपकाकर उन्हें अन्दर पहुँचने से रोकती हैं।(ii) रासायनिक अवरोधक-आमाशय में पाये जाने वाले एन्जाइम, आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण, जीवाणुओं व अन्य रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। त्वचा पर पाये जाने वाले रासायनिक तत्व (सीवम) व कर्ण मोम (सेरुमन) आदि रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं।(iii) कोशिकीय अवरोधक ( पेल्युलर बैरियर)-हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केन्द्रक श्वेताणु उदासीनरंजी (पीएमएनएल-न्यूट्रोफिल्स) जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एककेन्द्रकाणु (मोनासाइट्स) तथा प्राकृतिक, मारक लिंफोसाइट्स के प्रकार एवं ऊतकों में वृहत् भक्षकाणु (मैक्रोफेजेज) रोगाणुओं का भक्षण करते और नष्ट करते हैं।(iv) ज्वर, सूजन आदि।(2) उपार्जित प्रतिरक्षा विधि (Acquired defence mechanism)
इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा जन्म के पश्चात् व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर पहचान कर विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा अथवा उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है–
- सक्रिय प्रतिरक्षा
- निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(i) सक्रिय प्रतिरक्षा (Active Immunity)-इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशेष प्रतिजन (Antigen) के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी (Antibody) का निर्माण होता है।(ii) निष्क्रिय प्रतिरक्षा (Passive Immunity)-निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाये जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी (Antibody) का निर्माण नहीं किया जाता है। उदाहरण-टिटेनस, हिपेटाइटिस एवं डिप्थीरिया आदि।
प्रश्न 3. देहदान किसे कहते हैं? उन दो प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए जिनसे देहदान आवश्यक है?
उत्तर-
देहदान-अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण तथा चिकित्सकीय प्रशिक्षण के लिए दान करना देहदान कहलाती है।देहदान निम्न दो प्रमुख कारणों से आवश्यक है|
- मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किये जा सकते हैं। प्रायः अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है, जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो। ऐसे मामलों में मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बन्द कर देता है। परन्तु शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। ऐसी देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किये जा सकते हैं। हालांकि आँकड़े बताते हैं कि एक हजार में से केवल एक व्यक्ति की मौत ही इस प्रकार से होती है। मृत्यु के 6 से 8 घण्टों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है।
- चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृत देह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। मृत मानव की देह पर प्रायोगिक कार्य संपादन करने के बाद ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को भली प्रकार से समझ पाते हैं। इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता है। यह मानव देह की अन्तिम उपयोगिता है।
प्रश्न 4. विभिन्न रक्त समूह (एबीओ तथा आरएच समूहीकरण) को सारणी द्वारा समझाइए।
उत्तर-
विभिन्न समूह (एबीओ तथा आरएच समूहीकरण)
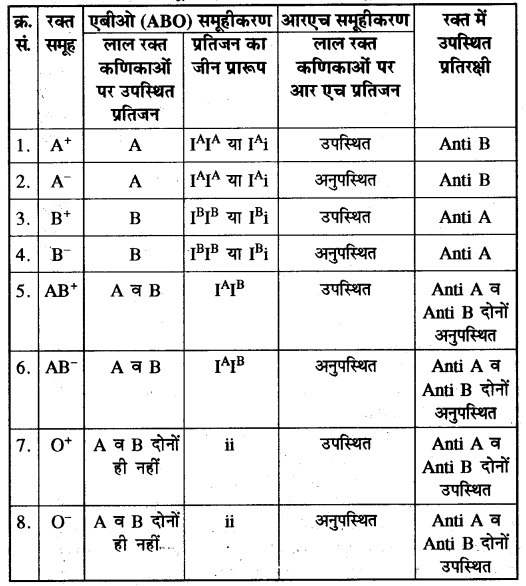
We hope the given Solutions for Class 10 Science Chapter 4 प्रतिरक्षा एवं रक्तसमूह will help you. If you have any query regarding Rajasthan Board RBSE Class 10 Science Chapter 4 प्रतिरक्षा एवं रक्तसमूह, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.
कक्षा 10 का दोहरान करने के लिए नीचे विज्ञान पर क्लिक करें
विज्ञान SCIENCE REVISION
CLCIK HERE FOR FREE MOCK TEST
CLICK HERE FOR ALL CLASS STUDY MATERIAL 2021
JOIN TELEGRAM
SUBSCRIBE US SHALA SUGAM
SUBSCRIBE US SHIKSHA SUGAM
SOME USEFUL POST FOR YOU
⇓ ⇓ ⇓
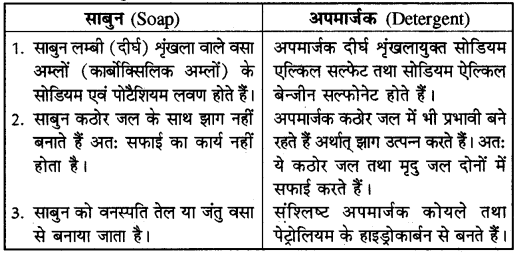
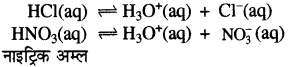
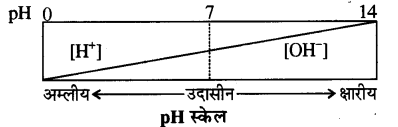
![]()
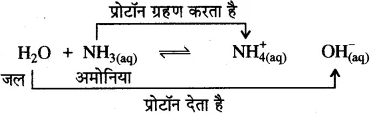
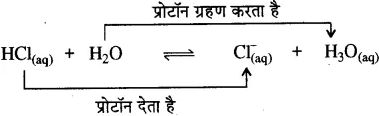
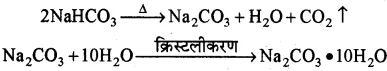
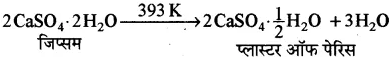
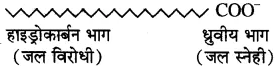
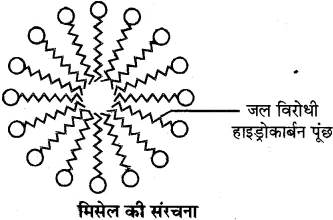
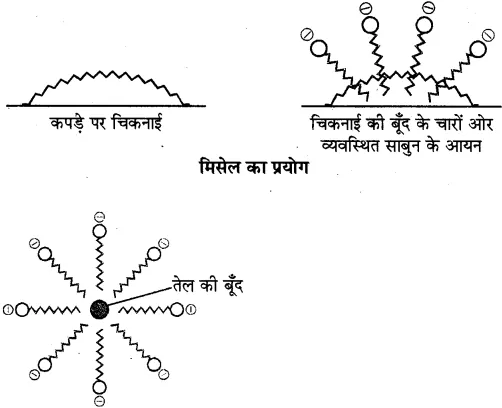
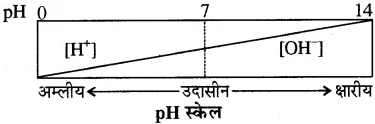
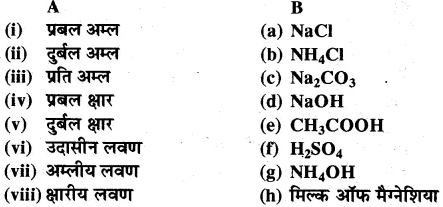
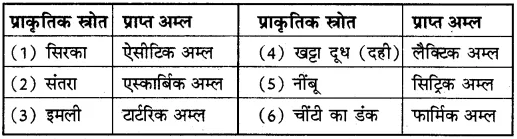
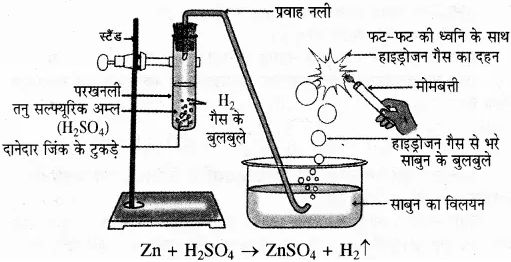
![]()